The post अनुवादक की बात appeared first on Translators of India.
]]>
तो आख़िरकार गालेआनो की किताब मुखेरेस (Mujeres) का हिंदी अनुवाद आपके सामने है। “आख़िरकार” शब्द यहाँ जोड़ना जरूरी है। ज़रूरी यह बताने के लिए है कि मैंने मूल किताब 2015 में ही स्पेन में रहने के दौरान ख़रीदी थी। उन्हीं दिनों गालेआनो 75 की उम्र में कैंसर से लड़ते हुए इस दुनिया से विदा हुए थे। यह मेरा दुर्भाग्य ही था कि जब मैं फरवरी, 2015 में स्पेन के उत्तर-पश्चिमी शहर सांतियागो दे कोम्पोस्तेला (Santiago de Compostela) पहुँचा था, उससे कुछ ही महीने पहले गालेआनो वहाँ आए थे। वैसे, उनसे उनके लिखे के ज़रिये गहरी पहचान का सिलसिला साल 2010 से ही शुरू हो गया था। मैंने अपना एम. ए. तथा एम. फिल. शोध कार्य उनके अलग-अलग टेक्स्ट्स पर किया था। तब से ऐसा लगता था कि वह मेरे देश, मेरे समाज और ख़ुद मेरे लिए भी लिखते हैं। उनके लेखन का जो हैरत अंगेज़ कर देने वाला दायरा है, वो अगर दुनिया में किसी देश या समाज को अपना लग सकता है, वो हिन्दुस्तान ही हो सकता है। हिंसा और शोषण की जितनी भयावह दास्तानें, बराबरी और बेहतरी की जो ख़्वाहिशें और छटपटाहटें गालेआनो के लिखे से सीधे पढ़ने वाले के बहुत अंदर रूह तक पहुँचती हैं, हमारे अपने समाज से आने वाला कोई भी संवेदनशील इंसान उनसे क़रीबी रिश्ता महसूस करेगा।
2015 के उस दिन से ही, जब गालेआनो की यह ख़ास किताब हाथों में आई, ज़ेहन में यह बात जैसे दर्ज हो गई कि यह किताब भारत के अपने हिंदी-भाषी लोगों में उनकी अपनी ज़बान में पहुँचनी ही चाहिए। किताब के पन्नों को सरसरी तौर पर पढ़ने से ही अंदाज़ा हो गया था कि यह कोई रूमानी ख़याल नहीं, बल्कि जरूरत थी। जिस तरीक़े से गालेआनो इस दुनिया के कितने ही जाने-अनजाने हिस्सों से इतिहास के पन्नों में दर्ज तथा उससे ओझल रह गई औरतों की कहानियाँ सामने लाते हैं, वो हमारे देश-गाँव की अनगिनत नाम-अनाम औरतों की कहानियाँ बन जाती हैं। वही औरतें, जो अपने-अपने मायनों में एक-दूसरे से समय और काल के अलग-अलग छोरों पर रहने के बावजूद कुछ ख़ास मायनों में एक-सी असाधारण हैं। हम इनमें से कइयों को नहीं जानते, क्यूँकि कई तो हमारे इतने आस-पास मौजूद रही हैं, वे साधारण घरों और गलियों की ऐसी औरतें हैं, कि हमने उनका नोटिस ही नहीं लिया है। किसी सरकारी या बौद्धिक इतिहास ने भी उनकी कहानियाँ पूरी बारीकियों में बताने की जरूरत महसूस नहीं की है।
ऐसे में, अर्जेंटीना के एक छोटे से कस्बे की उन औरतों का ज़िक्र कहाँ से आता, जिन्हें समाज रंडियाँ कहता है और जिन्होंने मजदूरों का क़त्लेआम करने वाले फ़ौजियों को अपने कोठे से गरियाते हुए धक्का देकर निकाल दिया था। गालेआनो उन पाँच औरतों का नाम याद रखते और कराते हैं। दूसरी तरफ, इसी देश की सैन्य तानाशाही से उसी के हाथों ग़ायब किये गए अपने बेटे-बेटियों तथा नाती-पोतियों का हिसाब माँगने वाली माँओं तथा दादी-नानियों को भी हमारे सामने ला खड़ा करते हैं। वैसे तो दुनिया इनके बारे में थोड़ा-बहुत जानती है, लेकिन जिस आत्मीयता, नजदीकी और शिद्दत से गालेआनो उनकी टूटन, उनके भीतर के डर और उनके हौसले को अपने शब्दों से महसूसते, छूते और थपकियाँ देते हैं, वह कहीं और मिलना मुश्किल लगता है। गालेआनो के लिखे में वे अनाम, ‘बदनाम’ औरतें तथा वे दादी-नानियाँ सभी अपनी अलग-अलग स्थितियों में एक ही साथ साधारण और असाधारण हैं।
यह तो एक बानगी भर है। किताब के अंदर जाएँ, तो आपको गालेआनो का रचा पूरा का पूरा संसार मिलेगा। यहाँ हज़ारों साल पहले हुई और आज तक हमारी कथाओं, किंवदंतियों, गप्पों और बहसों का हिस्सा रहीं क्लिओपेट्रा, त्लासोल्तेओत्ल, तेओदोरा, हिपातिया तथा दूसरी किरदार आती हैं, तो वहीं पिछली पाँच-छह सदियों की वे औरतें भी जो अपने कहे, लिखे और किए से पूरी दुनिया को उनके लिए, हम सबके लिए बेहतर बनाने के लिए लड़ती रहीं। पूरी ज़िद से, सारे ख़तरे उठाकर, मार दिए जाने तक तथा उसके बाद भी। यहाँ हम दोमितिला से मिलेंगे, जो बोलीबिया के खान मजूरों के इलाके में घूरे पर फ़ेंक दी गई अपनी ज़िंदगी से उठकर उस देश की सैन्य तानाशाही से लोहा ले उसे अपनी दूसरी साथियों के साथ घुटने पर ला देने वाली जुझारू शख़्सियत बन जाती है। हम यहाँ फ्रांसीसी क्रान्ति के बाद स्त्री-अधिकारों की आवाज़ बुलंद करने के ‘जुर्म’ में मौत की सज़ा देने वाली गुलोटीन पर चढ़ा दी गई ओलंपिया द गूजे से रू-ब-रू होते हैं, तो मतदान के अपने अधिकार के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के सुप्रीम कोर्ट तक से भिड़ जाने वाली सुसान एंथनी से भी वाक़िफ़ होते हैं।
गालेआनो उन औरतों की ज़िंदगी और ख़यालातों में भी दाख़िल होने का मौक़ा बनाते हैं, जो कुछ ऐसे जीती, ऐसा करती और कहती हैं, जो हमें इंसानियत तथा सृष्टि की सभी अभिव्यक्तियों के साथ राग-प्रेम के तार जोड़ने की कई मिसालें दे जाता है। यहाँ आप पेरिस शहर की उस माँ से मिलते हैं, जो अपने बेटे की मौत के बाद यह यक़ीन करने लगती है कि वह अब एक कबूतर बन चुका है। इसके बावजूद कहे जाने पर भी वह कबूतरों के झुंड से किसी एक को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती क्यूँकि , बकौल उसके, उसे “क्या हक़ है कि वह अपने बेटे को अपने दोस्तों से जुदा करे”! गालेआनो तो उस बूढ़ी हथिनी की भी बात करते हैं, जो सबसे अक़्लमंद तो है ही, झुंड में सबका ख़याल रखने वाली तथा सबकी स्मृतियाँ संजोने वाली भी है।
यह हमारी त्रासदी है कि हम इन मुख़्तलिफ़ किरदारों को नहीं जानते या जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। इससे इनका महत्व कहीं से भी कम नहीं होता, एक समाज के तौर पर हमारी बदनीयती और हमारा बौनापन ही ज़ाहिर होता है। संकलन में आती दूसरी किरदारों की कहानियाँ बार-बार हमें यही अहसास दिलाती हैं। और इसलिए इन्हें दुनिया की सारी भाषाओं तक पहुँचाया जाना ज़रूरी हो जाता है। और यह हिंदी अनुवाद इसी दिशा में एक छोटी-सी लेकिन संजीदा कोशिश है।
अब कुछ बातें इन कहानियों के हिंदी अनुवाद पर। साल 2011 में मैंने पहली बार गालेआनो का लिखा हिंदी में ढालने की कोशिश की थी। तब यह अहसास हुआ कि गालेआनो जितने तरह के सन्दर्भों को चुटकी में पकड़ लेने वाले अंदाज़ में सामने ला खड़ा कर देते हैं, उसे हिंदी में उसी जीवंतता के साथ लाना बड़ी चुनौती है। तब वो फिर भी बस एक लेख का मामला था जिसका एक ख़ास सरोकार था। इसके बाद जब 2015 में Mujeres (मुखेरेस) हाथों में आई और इसकी कुछ कहानियाँ पढ़ीं, तब यह चुनौती कहीं और ज़्यादा बड़ी और मुश्किल लगी। यहाँ तो लगभग हर कहानी में इतिहास, राजनीति, रोजाना के अहसासात तथा कितने ही और सन्दर्भ एक-दूसरे में गुँथे हुए हैं कि एकबारगी यह सारा कुछ समझ आ जाने वाली हिंदी में रख पाना असंभव ही लगा। अनुवाद करने की ललक सामने खड़ी इस मुश्किल से, हालाँकि, कम नहीं हुई, बल्कि और ज़्यादा तेज़ ही हुई। कहानियों में और ज़्यादा उतरते ही यह भी अहसास हुआ कि इन कहानियों और वहाँ आती औरतों को हमारे हिंदी-भाषी लोगों से मिलाना ही चाहिए।
अनुवाद करते समय लगभग हर कहानी में उस ख़ास किरदार को बनाने वाले इतिहास, आर्थिकी, राजनीति आदि की परतों को स्पेनी से हिंदी में सहज रूप से लाना हमेशा याद रहने वाला अनुभव था। मिसाल के लिए, एक कहानी में लेखक ख़ुद का अनुभव दर्ज करते हुए यह बताते हैं कि कैसे उनके पुराने दिनों का दोस्त लेखकों के पहले से तय मुफ़लिसी वाले भाग्य की मुनादी किया करता था। यहाँ मूल कहानी में hamburguesar यानी हैम्बर्गर या बर्गर खाकर गुज़ारा करने का ज़िक्र आता है। अब हमारे समाज में इस तरह की स्थिति में भी बर्गर खाकर गुज़ारा करने की बात किसी को नहीं सूझ सकती। यह सिर्फ भाषा का नहीं इतिहास और उससे गुँथे और निकलते आर्थिक हालात तथा खान-पान की आदतों को दिखाता है। और ये सारी चीजें भारत में हमारे हिंदी-भाषी समाज में बहुत अलहदा हैं। लेकिन ग़रीबी के हालात में रूखा-सूखा खाकर गुज़ारा करने का अनुभव और वो भी कलाकारों तथा लेखकों के लिए, इस समाज के लिए भी नया नहीं है, भले हम यही बात घास-फूस खाकर ज़िंदा रहने जैसी अभिव्यक्तियों से ज़ाहिर करते हैं। तो इस कहानी का अनुवाद करते समय इस बात को फुटनोट के तौर पर विस्तार से जगह दी गई है। मक़सद यही कि एक आम हिंदी भाषी के लिए यह कहानी उसके अपने आसपास की ऐसी ही कहानियों में एक लगे। गालेआनो भी चाहते कि वो जिस रूहानी भाव से, जिन गहराइयों में उतरकर अपने किरदारों और उनके सन्दर्भों को लाते हैं, दुनिया में कहीं भी कोई उन्हें पढ़े, तो वही भाव महसूसे तथा कुछ पल के लिए ही सही उस कहानी के संसार में शामिल हो तथा बेहतरी की उम्मीदों के साथ वापस आए।
मूल स्पेनी में कई ऐसे मुहावरे भी पेश आए जिन्हें हिंदी में ढालते वक़्त यह बात मालूम हुई कि यहाँ भी हूबहू उन्हीं शब्दों के साथ उन्हीं भावों को लिए हुए मुहावरे मौजूद हैं। मसलन स्पेनी में कहते हैं: estar en el septimo cielo (एस्तार एन एल सेप्तिमो सीएलओ) जिसका शब्दशः अनुवाद “सातवें आसमान पर होना” है, जो हिंदी में भी वैसे ही इस्तेमाल होता है। ऐसा ही एक और मुहावरा है con alma y vida (कोन आल्मा इ बीदा), जिसका शब्दशः मतलब “दिल और जान से है” जिससे भारत में हम एक मुहावरे के तौर पर बख़ूबी परिचित हैं। वहीं दूसरी तरफ़, कुछ कहानियों में रोज़ाना गली-मुहल्लों में खाई जाने वाली ऐसी चीज़ों का जिक्र आया है जिनका अनुवाद समाज, भूगोल, संस्कृति के कई जाने-अनजाने दरवाज़े खोल गया। जैसे कि, एक कहानी ‘वसीयत जिसको कहते हैं’ में स्पेन के हर शहर के हर रेस्त्रां और कैफेटेरिया में मिलने वाले ख़ास मीठे chocolate con churro (चोकोलाते कोन चुर्रो) का ज़िक्र आता है। यह दो अलग-अलग चीज़ों का अद्भुत मेल है, जिसमें एक खाई जाने वाली तो दूसरी पी जाने वाली है। गर्मागर्म चॉकलेट की लपसी और छोटी डंडी की तरह दिखता चुर्रो । चॉकलेट की लपसी तो फिर भी लोग समझ लेंगे, लेकिन चुर्रो को बयान करना दिलचस्प और कठिन दोनों ही था। जो लोग बिहार या उत्तर प्रदेश से होंगे, उन्होंने गाँवों-कस्बों में फोफी नाम की चीज देखी और खाई होगी। अब आप उसी फोफी को नमकीन नहीं मीठा समझिए और उसे खोखला न देखकर अंदर से भरा हुआ, ऊपर से चीनी के छोटे-छोटे टुकड़ों से सजा हुआ, हल्के -गहरे भूरे रंग का देखिए, तब आप चुर्रो को देखने-समझने के काफ़ी क़रीब होंगे। ऐसी सब तफ़सीलें लगभग हर कहानी के फुटनोट में हैं।
इन तफ़सीलों को समझने, इनकी तह में जाने का अनुभव भी काफी दिलचस्प रहा। लगभग हर कहानी में 2-3 तो अक्सर थोड़े लम्बे हो गए फुटनोट्स ही हैं। इनमें हर एक को लिखते समय की गई इतिहास, भूगोल, संस्कृति, खान-पान, रीति-रिवाज़ आदि की लंबी-लंबी विचार यात्राएँ हमेशा ख़ास रहेंगी, उन पर अलग से एक पूरी किताब लिखी जा सकती है!
जिन लोगों ने भी गालेआनो को पढ़ा है, वो बख़ूबी जानते होंगे कि उनके यहाँ छोटे-छोटे वाक्यों, मुहावरों आदि का इस्तेमाल एक अनूठा संसार रचता है। उन्हें पढ़ने वाले इस रचे जा रहे संसार में बेखटके ऐसे दाख़िल होते हैं, जैसे वह गालेआनो के साथ मिलकर यह सब कुछ देख और बयान कर रहे हैं। छू जाने वाली, सहलाने वाली, कभी नींद से झिंझोड़ कर जगाती, कभी प्यारी-सी थपकी देकर अनदेखे संसार में उतारने वाली, कभी पास बैठकर बाँह पकड़कर अन्याय के ख़िलाफ़ खड़ा होने को झकझोरती, गालेआनो की भाषा अपनी अतरंगी कूची से कितने ही रूहानी, सीधा असर करने वाले रंग बिखेरती है। अनुवाद करते समय इन सब अनुभूतियों, रंगों, अहसासों को उसी तरह कम शब्दों तथा छोटे-छोटे वाक्यों में ज़ाहिर करना लगातार एक चुनौती के साथ-साथ दिलचस्प और सिखाने वाला अनुभव रहा। मुझे हमेशा याद रहेगा कि कैसे अक्सर ही किसी कहानी में आए एक ख़ास शब्द को हिंदी में ढालते वक़्त पूरा-पूरा दिन सोचते हुए निकल जाता था।
कई बार तो दो-दो दिन। तब इरादा कभी भी कोई एक शब्द, जो ढीले-ढाले तरीके से भी मुफ़ीद हो, चस्पाँ कर आगे बढ़ जाने का कभी नहीं रहा। और जब वह ख़ास शब्द मिलता, जो अंदर से तस्दीक़ कराता कि हाँ मैं ही वह शब्द हूँ जिसकी तुम ताक में हो, तब उस संतुष्टि और आनंद की तुलना किसी और अनुभूति से नहीं हो सकती। उस ख़ास शब्द तक पहुँचने का सफ़र इस अनुवाद का सबसे अहम और खूबसूरत हिस्सा था। यह सफ़र हर बार भाषा, समाज, संस्कृति, राजनीति, भूगोल और जीवन के तमाम दूसरे ताने-बाने की इतनी गहराइयों में ले जाता था कि यह अहसास अपने-आप हो जाया करता कि मैं जिसे ‘अपनी’ भाषा, ‘अपनी’ संस्कृति कहता रहा हूँ, उसे कितना जानना अभी बाक़ी है। अनुवाद, दरअसल, अगर ‘दूसरी’ से ज़्यादा ख़ुद ‘अपनी’ संस्कृति को जानना नहीं है तो और क्या है? इससे भी आगे बढ़कर यह कहा जाना चाहिए कि यह सिर्फ़ और सिर्फ़ अनुवाद के ज़रिये ही हो सकता है कि हम यह समझें कि वास्तव में सारी संस्कृतियाँ और सारी भाषाएँ एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उनका एक-दूसरे में आना-जाना इस धरती पर इंसानी सफ़र का सबसे बड़ा सच है। फिर हम यह भी देख पाएंगे कि ‘अपनी’ और ‘दूसरी’ या विदेशी (जिसे ‘विरोधी’ या ‘दुश्मन’ बताने में देर नहीं लगती) के तमाम झगड़े कितने अर्थहीन ही नहीं हास्यास्पद भी हैं। गालेआनो अपनी लेखनी और देश-दुनिया में बुलंद की गई अपनी आवाज़ से ताउम्र इस सफ़र को जीते रहे, इसका एक शानदार और रौशन हिस्सा रहे। वह ऐसी दुनिया बनाने के ख़्वाहिश-मंद रहे, जहाँ यह सफ़र लगातार चलता रहे। फिर उनके लिखे का अनुवाद करते समय वही ख़्वाहिश आपके अंदर आकर ले, आपको कुछ करने को कहे तो फिर यह कहा जा सकता है कि गालेआनो के लिखने से शुरू हुई वह कोशिश, वह अभिलाषा एक खूबसूरत मोड़ पर पहुँच रही है। ख़त्म तो ख़ैर वह कभी नहीं होगी।
(यह अनुवादकीय डॉ. पी. कुमार मंगलम द्वारा अनूदित पुस्तक ‘औरतें’ से साभार लिया गया है।)

डॉ. पी. कुमार मंगलम
स्नातक, स्नातकोत्तर (स्पेनी भाषा), एम. फ़िल. एवं पी.एच.डी. (लातिन अमरीकी साहित्य), जे.एन.यू., नई दिल्ली
स्नातकोत्तर कार्यक्रम Crossways in Cultural Narratives (यूरोपीय यूनियन के स्कालरशिप प्रोग्राम के साथ): इंग्लैंड, स्पेन तथा फ्रांस में अध्ययन, 2014-2016
मेक्सिको में पोस्ट-डॉक प्रवास (2019)
जे.एन.यू. तथा दून विश्वविद्यालय में बतौर शोधार्थी एवं अस्थायी शिक्षण
2019 से कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा में स्पेनी भाषा में पूर्णकालिक अध्यापन
‘समयांतर’, ‘बया’, ‘सामयिक वार्ता ‘आदि कई पत्रिकाओं में अनुवाद और लेखों का प्रकाशन। 2015 में किताब की शक़्ल में एदुआर्दो गालेआनो के लेखों का अनुवाद प्रकाशित।
स्पेनी-भाषा समाजों के इतिहास, संस्कृति तथा साहित्य के अध्ययन में गहरी रुचि। स्पेन और लातीनी अमरीका की कुछ बेहद दिलचस्प परिघटनाओं पर भारत के नज़रिए से हिंदी में लेखन की योजना। pkmangalam@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है.
P. Kumar Mangalam is currently serving as Assistant Professor in Spanish at the Central University of Karnataka, Kalaburagi, India. He has obtained his PhD from JNU, New Delhi. He was also awarded a Postdoctoral fellowship of the prestigious Mexican agency GAPA in the year 2019. His paper entitled “Where Defending Mother-Earth and Quests for a Just World are the Same and One: Some Instances from Latin America” has been accepted for the edited volume “Critical Zones: Environmental Humanities in South Asia” to be published by Routledge India.
The post अनुवादक की बात appeared first on Translators of India.
]]>The post विने एवं दार्बेलने की अनुवाद प्रविधियाँ appeared first on Translators of India.
]]>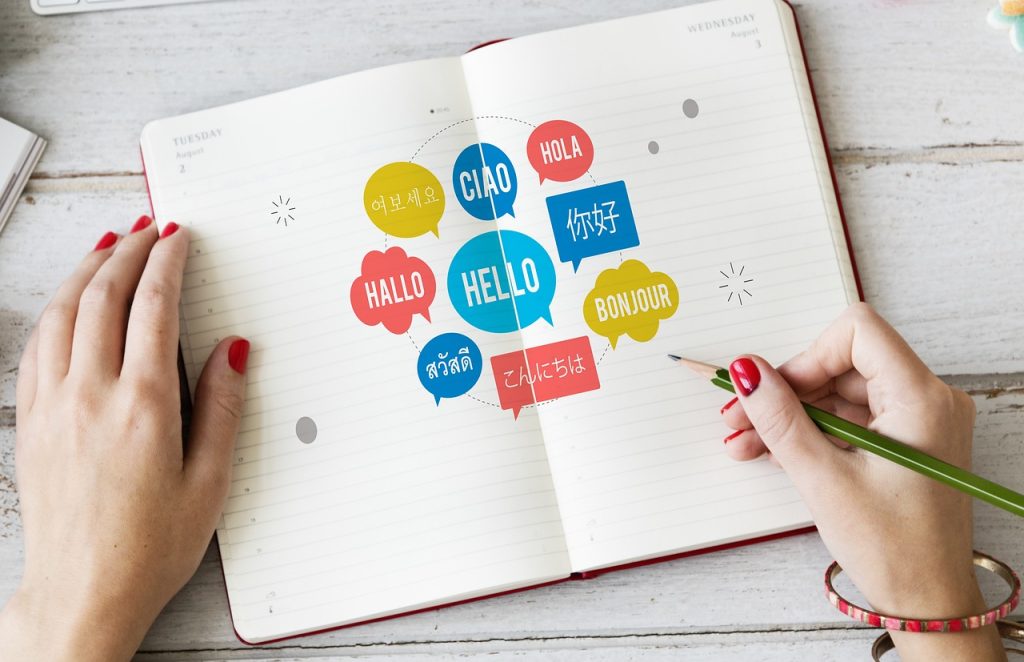
ज़ौं पॉल विने एवं ज़ौं पॉल दार्बेलने ने 1958 में प्रकाशित अपनी फ़्रेंच पुस्तक ‘Stylistique comparée du français et de l’anglais: méthode de traduction’ (स्तिलिस्तिक कौम्पारे द्यु फ़्रांसै ए द लौंग्ले : मेतोद द त्राद्युक्सियों) में अनुवाद प्रविधियों का वर्णन किया है। इस पुस्तक में अनुवाद को केंद्र में रखकर अंग्रेज़ी और फ़्रेंच की भाषिक संरचनाओं की तुलना की गई है। फ़्रांस में इसे तुलनात्मक शैलीविज्ञान की प्रतिनिधि पुस्तकों में से एक माना जाता है। विने एवं दार्बेलने ने इस पुस्तक में अनुवाद की सात प्रविधियों का उल्लेख किया है। यह पुस्तक चार दशक बाद 1995 में अंग्रेज़ी में ‘Comparative Stylistics of French and English : A methodology for translation’ (फ़्रेंच और अंग्रेज़ी का शैलीगत तुलनात्मक अध्ययन : अनुवाद प्रविधि) शीर्षक से अनूदित की गई। इतना समय बीत जाने के बावजूद इस पुस्तक का अंग्रेज़ी में अनूदित किया जाना इसकी प्रासंगिकता का प्रमाण है। अनुवाद प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी इस पुस्तक को उपयोगी माना जाता है।
हर भाषा की अपनी विशिष्ट भाषिक संरचनाएँ होती हैं। इन संरचनाओं की भिन्नता कई बार अनुवाद की चुनौती बनकर सामने आती है। भाषिक संरचनाओं की विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर न केवल भाषिक ग़लतियों से बचा जा सकता है, बल्कि अनुवाद को अधिक सहज और प्रभावी भी बनाया जा सकता है। विने एवं दार्बेलने ने अनुवाद की जिन सात प्रविधियों का उल्लेख किया है, उनका अध्ययन करके अनुवाद प्रशिक्षु अपनी स्रोत और लक्ष्य भाषाओं की भाषिक संरचनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनते हैं। इस सात प्रविधियों में से पहली तीन प्रविधियाँ प्रत्यक्ष अनुवाद से संबंधित हैं और बाकी चार प्रविधियाँ अप्रत्यक्ष अनुवाद से। जो प्रविधियाँ भाषिक संरचनाओं तक सीमित रहती हैं, उन्हें प्रत्यक्ष अनुवाद के अंतर्गत रखा गया है। वहीं, जिन प्रविधियों में भाषिक संरचनाओं से परे जाकर परिवर्तन किए जाते हैं, उन्हें अप्रत्यक्ष अनुवाद में शामिल किया गया है। ये सात प्रविधियाँ सरलता से जटिलता के क्रम में प्रस्तुत की गई। पहली प्रविधि सबसे सरल है और अंतिम सबसे जटिल। इन प्रविधियों का विवरण नीचे प्रस्तुत है :
1. आदान (Borrowing)
लक्ष्य भाषा में उपयुक्त विकल्प मौजूद नहीं होने की स्थिति में स्रोत भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चूँकि ये शब्द बिना किसी परिवर्तन के ग्रहण किए जाते हैं, इन्हें ‘ऋण शब्द’ कहा जाता है। यदि लक्ष्य भाषा की लिपि अलग हो, तो अनुवाद में इन शब्दों के लिप्यंतरित रूपों का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, विज्ञापन आदि क्षेत्रों में ऋण शब्दों का अधिक प्रयोग होता है।
कुछ हिंदी अख़बारों की संपादकीय नीति के कारण कई बार उपयुक्त शब्दों के उपलब्ध होने के बावजूद ऋण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, ‘विज्ञापन’ को ‘एडवर्टाइज़मेंट’ लिखना। जो देश आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, उनकी भाषाओं में विकसित भाषाओं के शब्दों के अनावश्यक प्रयोग की प्रवृत्ति देखी जाती है। यह स्थिति केवल हिंदी, मराठी जैसी भारतीय भाषाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जर्मन और फ़्रेंच में भी अंग्रेज़ी शब्दों की भरमार होने लगी है।
यदि विदेशी भाषा से शब्द ग्रहण करते समय सावधानी नहीं बरती जाए, तो इससे अनुवाद के ग़लत होने की आशंका बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, जब ‘Bodymist’ नाम की डियोडरेंट कंपनी के उत्पाद को जर्मनी के बाज़ार में उपलब्ध कराने के लिए इस नाम का ऋण शब्द के रूप में प्रयोग किया गया, तो ‘mist’ शब्द के कारण समस्या पैदा हो गई। जर्मन में ‘mist’ का अर्थ ‘खाद’ है, इसलिए प्रस्तुत संदर्भ मे जर्मन के बाज़ार में इसका प्रयोग अटपटा साबित हुआ।
2. काल्क (Calque)
विने एवं दार्बेलने ने इस प्रविधि को ‘एक विशिष्ट प्रकार का आदान’ कहा है। ‘काल्क’ (प्रतिलिपि) शब्द की व्युत्पत्ति फ़्रेंच की calquer क्रिया से हुई है, जिसका अर्थ ‘डिज़ाइन, मानचित्र आदि की नकल उतारना’ है। इसमें स्रोत भाषा की अभिव्यक्ति ग्रहण करके उसके घटकों का शाब्दिक अनुवाद किया जाता है। जैसे, अंग्रेज़ी के ‘cold war’ को हिंदी में ‘शीत युद्ध’ लिखा जाता है। यहाँ हिंदी समतुल्य में अंग्रेज़ी के शब्दों को यथावत नहीं लेकर ‘cold’ और ‘war’ के शाब्दिक अनुवादों के माध्यम से ‘शीत युद्ध’ समतुल्य प्रस्तुत किया गया है। काल्क के ज़रिए लक्ष्य भाषा में नई अवधारणाएँ शामिल होती हैं। जैसे, बैंकिंग में ‘चालू खाता’ (current account) और ‘बचत खाता’ (savings account) तथा राजनीति में ‘प्रधानमंत्री’ (prime minister) और ‘मुख्यमंत्री’ (chief minister) जैसे समतुल्य काल्क के उदाहरण हैं। समय के साथ ये समतुल्य इतने प्रचलित हो गए हैं कि इन्हें हिंदी में समतुल्य के बजाय मूल हिंदी शब्द माना जाने लगा है।
3. शब्दानुवाद (Literal Translation)
यह प्रविधि समान भाषिक संरचनाओं या संस्कृतियों वाली भाषाओं में अधिक प्रयुक्त होती है। इसमें बस वही परिवर्तन किए जाते हैं जो लक्ष्य भाषा के व्याकरण के लिए अनिवार्य होते हैं। उदाहरण के लिए, He hit Mohan को हिंदी में “उसने मोहन को मारा” लिखा जाता है। यहाँ हिंदी व्याकरण का पालन करते हुए ‘को’ जोड़ा गया है। ऐसे व्याकरणिक परिवर्तन शाब्दिक अनुवाद के दायरे में शामिल रहते हैं।
4. प्रतिस्थापन (Transposition)
इसमें अर्थ में परिवर्तन किए बिना स्रोत भाषा की व्याकरणिक कोटि को लक्ष्य भाषा की भिन्न व्याकरणिक कोटि से प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसे, “It is raining” को हिंदी में “बारिश हो रही है” लिखा जाता है। यहाँ अंग्रेज़ी की क्रिया (raining) के लिए हिंदी में ‘बारिश’ संज्ञा का प्रयोग किया गया है। “His presence suffices” वाक्य को हिंदी में “उसकी मौजूदगी काफ़ी है” लिखा जा सकता है। इस हिंदी वाक्य में अंग्रेज़ी की ‘suffices’ क्रिया’ को हिंदी में ‘काफ़ी’ विशेषण में परिवर्तित किया गया है।
5. मॉडुलन (Modulation)
जब स्रोत भाषा के कथ्य के रूप में परिवर्तन किया जाता है, उसे मॉडुलन कहते हैं। दूसरे शब्दों मे, इसमें मूल कथ्य को एक नये दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया जाता है। जैसे, “I hurt my toe” का हिंदी अनुवाद “मेरे अँगूठे में चोट लग गई” है। इस वाक्य में कर्तृवाच्य को अकर्मक रूप में बदला गया है। इसी प्रकार, “The meeting was chaired by Manmohan Sharma” को हिंदी में “मनमोहन सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की” लिखकर अंग्रेज़ी के कर्मवाच्य को हिंदी के कर्तृवाच्य में बदला गया है। इस परिवर्तन से लक्ष्य भाषा में संदेश अधिक सहज बनता है।
6. समतुल्यता (Equivalence)
इसमें स्रोत भाषा में वर्णित स्थिति को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने के लिए भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लोकोक्तियों, मुहावरों आदि के अनुवाद में इस प्रविधि का सर्वाधिक प्रयोग होता है। शब्दकोशों में इनके जिन समतुल्यों को शामिल किया जाता है, वे समतुल्यता के उदाहरण होते हैं। जैसे, “rain cats and dogs” को हिंदी में “मूसलाधार बारिश होना” कहते हैं। “Barking dogs seldom bite” के लिए “जो गरजते हैं, वे बरसते नहीं” का प्रयोग भी समतुल्यता का उदाहरण है।
7. अनुकूलन (Adaptation)
अनुवाद की यह प्रविधि तभी अपनाई जाती है जब स्रोत भाषा में वर्णित स्थिति लक्ष्य भाषा की संस्कृति में मौजूद नहीं होती है। विने एवं दार्बेलने इसके लिए अंग्रेज़ी के एक वाक्य का उदाहरण देते हैं : “He kissed his daugther on the mouth.” यदि हम इस उदाहरण को हिंदी के संदर्भ में देखें, तो ‘kissed’ के लिए ‘चूमा’ के बजाय ‘गले लगाया’ का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार, इसका अनुवाद “उसने अपनी बेटी का मुँह चूमा” के बजाय “उसने अपनी बेटी को गले लगाया” होगा। स्रोत भाषा की संस्कृति में पुत्री के मुख पर चुंबन लेने को असहज या अस्वीकार्य नहीं माना जाता है। चूँकि हिंदी में यह स्थिति सहज नहीं मानी जाती है, अनुवादक को एक नई स्थिति का सृजन करना पड़ता है। विने एवं दार्बेलने ने अनुकूलन को ‘एक विशिष्ट प्रकार की समतुल्यता’ कहा है। इस प्रविधि का प्रयोग तभी किया जाता है जब उपर्युक्त सभी प्रविधियों से अर्थ व्यक्त नहीं हो पा रहा हो।
लेखक : सुयश सुप्रभ

नई दिल्ली में रहने वाले सुयश सुप्रभ को मार्केटिंग, बिज़नेस, गेम, टेक्नॉलजी आदि क्षेत्रों में अनुवाद और कॉपी लेखन का 18 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अनुवाद अध्ययन में एमए किया है। वे अनुवाद एजेंसियों और ग़ैर-सरकारी संस्थाओं के लिए अनुवाद करने के साथ तहलका और करियर्स360 जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के लिए काम कर चुके हैं। साथ ही, उन्होंने भाषा और अनुवाद से जुड़े कई लेख लिखे हैं। उनसे suyash.suprabh@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।
Suyash Suprabh is based in New Delhi and has more than 18 years of experience in translation and copywriting in many fields, including marketing, business, games, and technology. He has a postgraduate degree in translation studies. Besides having worked for translation agencies and non-government organizations, he has also worked with renowned Hindi magazines, including Tehelka and Careeres360, and has written many articles on languages and translation. He can be reached at suyash.suprabh@gmail.com.
The post विने एवं दार्बेलने की अनुवाद प्रविधियाँ appeared first on Translators of India.
]]>The post अनुवाद की चुनौतियां appeared first on Translators of India.
]]>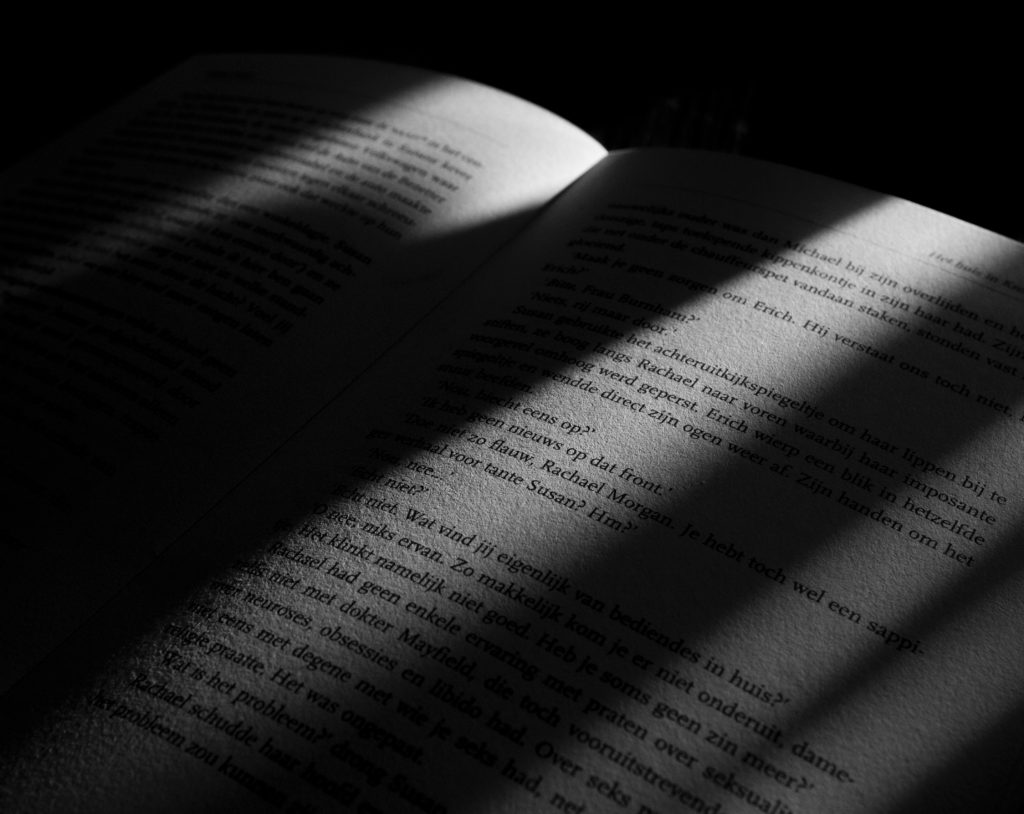
स्टोरीवीवर की कहानियों का अनुवाद हमेशा चुनौती साथ लाता है : हमें ठीक-ठीक मालूम नहीं होता कि कहानी का पाठक दुनिया के किस हिस्से में है, उसकी आयु या शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है, वह प्रस्तुत पाठ को किस उद्देश्य से पढ़ रहा है… अनेक प्रश्न बार-बार कलम रोकते हैं। क्या हमारे शब्द उसके लिए भी वही अर्थ रखते हैं, क्या हमारा किया अर्थान्वय उसके लिए भी कारगर रहेगा? और फिर लेखक के मूल कथ्य और मंतव्य को पकड़ने की चुनौती तो हमेशा ही अनुवादकों के सामने रहती है – अरे मन सम्हल-सम्हल पग धरिये!
एक मोटा-मोटा सूत्र राह दिखाता है : अनूदित सामग्री पढ़ने वाले पाठक के लिए वही मूल रचना है।
लेकिन नामों और रिश्तों का जटिल संसार कभी-कभी बहुत कड़ी परीक्षा लेता है। एक कहानी में दक्षिण भारतीय मुख्य चरित्र, जो एक लड़का था, का नाम सत्या था। हिंदी मे यह लड़कियों का नाम होता है; तो नामों के मूल रूप बनाए रखने की ताकीद के बावजूद मैंने उसका नाम सत्य कर दिया क्योंकि मुझे हिंदी के पाठकों को भ्रम में न डालना ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा। हाल ही में गोआनी मूल के ईसाई लेखक की लिखी सुंदर और बहुत रोचक कविता-कहानी में शवयात्रा के समय बजने वाले बैंड (भारत में कम ही जगह इस तरह का चलन है) का उल्लेख आया। इसे हिंदी के बाल-पाठक को समझाने के लिए हमें लंबी-चौड़ी टिप्पणी देनी पड़ती जो पढ़ने का मज़ा ही किरकिरा कर देती। तो हल निकाला शवयात्रा का उल्लेख गोल करके; पाठ की रोचकता बरकरार रही, उसकी गुणवत्ता हल्की नहीं हुई।
लेकिन कई बार तकनीकी शब्दावली की यांत्रिकता आड़े आती है : प्रचलित शब्द गोल/गोला से पता नहीं चलता कि वह किसी पिंड का संकेत दे रहा है या द्विआयामी आकृति का : गेंद भी गोल है, और नंगी आंख से धरती से दिखता चांद भी! अब अगर हम सायकिल के पिंडाकार पहियों की बात कहना चाहें तो कैसे कहेंगे? एक और बड़ी समस्या पशु-पक्षियों-कीट-पतंगों-वनस्पतियों के नाम हिंदी में बताते हुए आती है। इस संदर्भ में ‘ताल का जादू’ के हिंदी अनुवाद की याद आती है। इसमें उल्लिखित कई पक्षियों और कीटों के नाम मुझे नहीं पता थे। हमारी प्रचलित शब्दावली में, कई कारणों से इनमें से बहुत के नाम उपलब्ध नहीं हैं; किसी वैज्ञानिक शब्दावली में मिल भी जाएं तो शेर-बाघ-तेंदुए के बीच अंतर न जानने वाले हमारे पाठकों के लिए वे इतने अपरिचित होते हैं कि अंग्रेज़ी नाम देना भी ठीक ही लगता है – जैगुआर कहने पर यह संभावना बनी रहेगी कि कोई जानकार उसे इसका अर्थ समझा सकता है (वैसे जैगुआर अमेरिका में पाए जाने वाले तेंदुए हैं)। बेसिल का अर्थ आमतौर पर तुलसी लगाया जाता है लेकिन तुलसियां भी कम से कम छह तरह की होती हैं। बेसिल में यह तथ्य निहित है, तुलसी में नहीं।
हर नया पाठ अनुवादक के लिए नई चुनौती लाता है। हर नया अनुवाद भाषा के क्षितिज को कुछ आगे सरकाता है।
स्टोरीवीवर से साभार

मधु बी. जोशी कई दशकों से अनुवादक, कवयित्री, कहानीकार और स्तंभकार के रूप में अंग्रेज़ी और हिंदी के साहित्यिक जगत को समृद्ध करती आई हैं। वे तकनीकी अनुवाद को अपनी आय और साहित्यिक अनुवाद को रचनात्मक संतुष्टि का ज़रिया मानती हैं। उनके द्वारा अनूदित कृतियों में ‘बधिया स्त्री’ और ‘यह जीवन खेल में’ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आप उनसे madhubalajoshi@yahoo.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।
Over the last several decades, Madhu B. Joshi has enriched the Hindi and English literary worlds through her contributions as a translator, poet, story writer, and columnist. She views technical translation as a source of income that allows her to do literary translations of her choice. “Badhiya Stree” and “Yeh Jeevan Khel Mein” are among her most notable translations. She can be reached at madhubalajoshi@yahoo.co.in.
The post अनुवाद की चुनौतियां appeared first on Translators of India.
]]>The post व्यवहार से सिद्धांत और सिद्धांत से व्यवहार की ओर appeared first on Translators of India.
]]>
अनुवाद के क्षेत्र में लगभग एक दशक तक सक्रिय रहने के बाद इसके सैद्धांतिक पक्ष को ठीक से समझने में मेरी दिलचस्पी जगी। सबसे पहले तो यह सवाल दिमाग़ में आया कि अनुवाद करते समय हम भाषा, वर्तनी आदि से जुड़े जो विकल्प चुनते हैं उनका कोई सुव्यवस्थित अध्ययन हुआ है या नहीं। मुझे इस सवाल का जवाब अनुवाद अध्ययन में एमए करते समय नाइडा, न्यूमार्क, वर्मीयर जैसे अनुवाद सिद्धांतकारों के अकादमिक लेखन में मिला। जैसे-जैसे अनुवाद के सिद्धांतों में मेरी रुचि बढ़ती गई, मुझे अनुवाद के विस्तृत दायरे के बारे में और बहुत कुछ जानने को मिला। भारत में अनुवाद के इतिहास को ठीक से समझने में मुझे देवशंकर नवीन की पुस्तक ‘अनुवाद अध्ययन का परिदृश्य‘ से बहुत मदद मिली।
कई बार हम किसी धारणा को सिर्फ़ इसलिए सही मान लेते हैं कि अधिकतर लोग उसका समर्थन करते हैं। केवल सहज-सरल अनुवाद को अच्छा अनुवाद मानने की सोच भी ऐसी धारणाओं में से एक है। अकादमिक विषय के सिद्धांत की एक अच्छी बात यह होती है कि उसमें किसी बात को उसका समर्थन करने वालों की संख्या के आधार पर ही सही नहीं मान लिया जाता है। अनुवाद चिंतक लॉरेन्स वेनुती ने अनुवाद के सहज-सरल होने को उसका एकमात्र गुण मानने की सोच पर सवाल खड़ा किया है। अनुवाद में पाठ के विदेशीकरण और घरेलूकरण से जुड़े वेनुती के लेखन से हमें पता चलता है कि पाठक की सहूलियत का मामला उतना सरल नहीं है जितना हम उसे समझते आए हैं। सच तो यह है कि अनुवाद में सहजता लाने के सचेत प्रयास के कारण कई बार पाठक को अनुवाद में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जो उसके अनुभव-संसार का दायरा बढ़ाए। वेनुती ने अमेरिकी प्रकाशन जगत में सरल अंग्रेज़ी अनुवाद पर ज़ोर दिए जाने को अमेरिका की वर्चस्वकारी संस्कृति से जोड़कर देखा है। अनुवाद में स्रोत पाठ की संस्कृति की विशिष्टताओं को जगह न देना सांस्कृतिक श्रेष्ठता के बोध से जुड़ा है जिसमें अन्य संस्कृतियों के बारे में जानने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती है। वेनुती के लेखन में इस प्रवृत्ति की आलोचना दिखती है।
अनुवाद की दुनिया में क़दम रखने के बाद अनुभवी अनुवादकों से मुझे यह मालूम हो गया था कि अनुवाद भाव का होता है न कि शब्द का। लेकिन एक भाषा में कही गई बात को किसी दूसरी भाषा में व्यक्त करना हमेशा संभव नहीं होता है। चाहे साड़ी या धोती जैसे पहनावे से जुड़े शब्दों का अनुवाद करना हो या श्राद्ध, मुंडन जैसी धार्मिक-सांस्कृतिक अवधारणाओं को विदेशी पाठकों के लिए बोधगम्य बनाना हो, अनुवादक की चुनौतियों का कोई अंत नहीं होता है। जब आप ऐसे शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उनकी व्याख्या करते हैं, तो अनुवाद में मूल पाठ जैसी सहजता नहीं रह जाती। यह एक आम धारणा है कि केवल शब्दकोश की मदद से कोई भी व्यक्ति अनुवाद कर सकता है, जबकि सच यह है कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की सामाजिक-सांस्कृतिक जटिलताओं को ठीक से नहीं जानने वाले व्यक्ति से अच्छे अनुवाद की उम्मीद नहीं की जा सकती है। दो भाषाओं के पाठ असल में सममूल्य होते ही नहीं है। उनमें सममूल्यता की जगह समतुल्यता का संबंध होता है। यही वजह है कि नाइडा ने अनुवाद में निकटतम और सहजतम समतुल्यता की बात कही है न कि एक भाषा के कथ्य के सममूल्य अर्थ को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की।
नाइडा ने अपनी पुस्तक ‘टूवर्ड ए साइंस ऑफ़ ट्रांसलेटिंग‘ में बाइबिल के उन संदर्भों का उल्लेख किया है जो समतुल्यता से जुड़ी जटिलताओं को सामने लाते हैं। उदाहरण के लिए, बाइबिल में इस बात का उल्लेख है कि लंबे बाल रखना पुरुषों को शोभा नहीं देता है। लेकिन इक्वाडोर की जिवारो जनजाति के लोगों को यह बात अटपटी लगेगी क्योंकि वे लंबे बाल रखते हैं। इस जनजाति की औरतें छोटे बाल रखती हैं। दक्षिण अफ़्रीका के कुछ हिस्सों के लोग अपने मुखिया का स्वागत करने के लिए उसके रास्ते में पड़े पत्तों और शाखाओं को साफ़ कर देते हैं। बाइबिल में यह लिखा गया है कि जब ईसा मसीह येरूशलम जा रहे थे तब श्रद्धालु उनके रास्ते पर पत्ते और शाखाएँ फेंककर उनका स्वागत कर रहे थे। जहाँ लोग रास्ते में पड़े पत्ते और शाखाएँ साफ़ करने को स्वागत से जोड़कर देखते हैं, उनके लिए इस प्रसंग को समझना मुश्किल है। इस तरह, हम देखते हैं कि समतुल्यता को केवल शब्द के स्तर पर नहीं समझा जा सकता है, बल्कि इसे विभिन्न संस्कृतियों की मान्यताओं, अवधारणाओं आदि के बड़े दायरे में देखना होगा।
कई अनुवादकों का मानना है कि अनुवाद अध्ययन से अनुवादक को किसी तरह की मदद नहीं मिलती है। वे कुछ अच्छे अनुवादकों के नाम गिनाते हुए कहते हैं कि उन्होंने अनुवाद सिद्धांतों की जानकारी के बिना इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। उनकी इस बात से यहाँ तक मेरी सहमति है कि अनुवादक अपने कौशल के लिए सिद्धांत पर निर्भर नहीं होते हैं। लेकिन जब बात अनुवाद अध्ययन को सिरे से ख़ारिज करने तक पहुँच जाती है तो मैं असहमति जताना ज़रूरी समझता हूँ। अकादमिक दुनिया में अनुवाद अध्ययन की स्थिति बेहतर होने से अनुवादक से जुड़े मसलों के प्रति बेहतर समझ पैदा करने में मदद मिलेगी। अधिकतर लोगों को यह पता ही नहीं है कि किसी भाषा की सामाजिक-सांस्कृतिक विशिष्टताओं को दूसरी भाषा में अच्छे ढंग से व्यक्त करने के लिए अनुवादक को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर अनुवाद की जटिलताओं और सभ्यता के विकास में इसके योगदान की विस्तृत जानकारी स्कूल के स्तर पर ही दे दी जाए, तो पढ़-लिखे लोगों की अनुवाद के प्रति अतार्किक सोच को बदलना संभव हो जाएगा।
आज अनुवाद अध्ययन में कॉर्पस भाषाविज्ञान, स्कोपस सिद्धांत, शब्दावली प्रबंधन आदि की पढ़ाई पर ध्यान देकर अनुवादक की व्यावसायिक और व्यावहारिक ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही, औपनिवेशिकता, जेंडर आदि से जुड़े विमर्श के माध्यम से अनुवाद के वैचारिक दायरे का विस्तार किया जा रहा है। ज़रूरत बस अनुवाद के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्षों के बीच संवाद में तेज़ी लाने की है। ऐसा तभी होगा जब पेशेवर अनुवादकों और अकादमिक दुनिया के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए सांस्थानिक स्तर पर प्रयास किए जाएँगे।

नई दिल्ली में रहने वाले सुयश सुप्रभ को मार्केटिंग, बिज़नेस, गेम, टेक्नॉलजी आदि क्षेत्रों में अनुवाद और कॉपी लेखन का 17 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अनुवाद अध्ययन में एमए किया है। वे अनुवाद एजेंसियों और ग़ैर-सरकारी संस्थाओं के लिए अनुवाद करने के साथ तहलका और करियर्स360 जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के लिए काम कर चुके हैं। साथ ही, उन्होंने भाषा और अनुवाद से जुड़े कई लेख लिखे हैं। उनसे suyash.suprabh@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।
Suyash Suprabh is based in New Delhi and has more than 18 years of experience in translation and copywriting in many fields, including marketing, business, games, and technology. He has a postgraduate degree in translation studies. Besides having worked for translation agencies and non-government organizations, he has also worked with renowned Hindi magazines, including Tehelka and Careeres360, and has written many articles on languages and translation. He can be reached at suyash.suprabh@gmail.com.
The post व्यवहार से सिद्धांत और सिद्धांत से व्यवहार की ओर appeared first on Translators of India.
]]>The post अनुवाद की कुछ व्यावहारिक समस्याएं appeared first on Translators of India.
]]>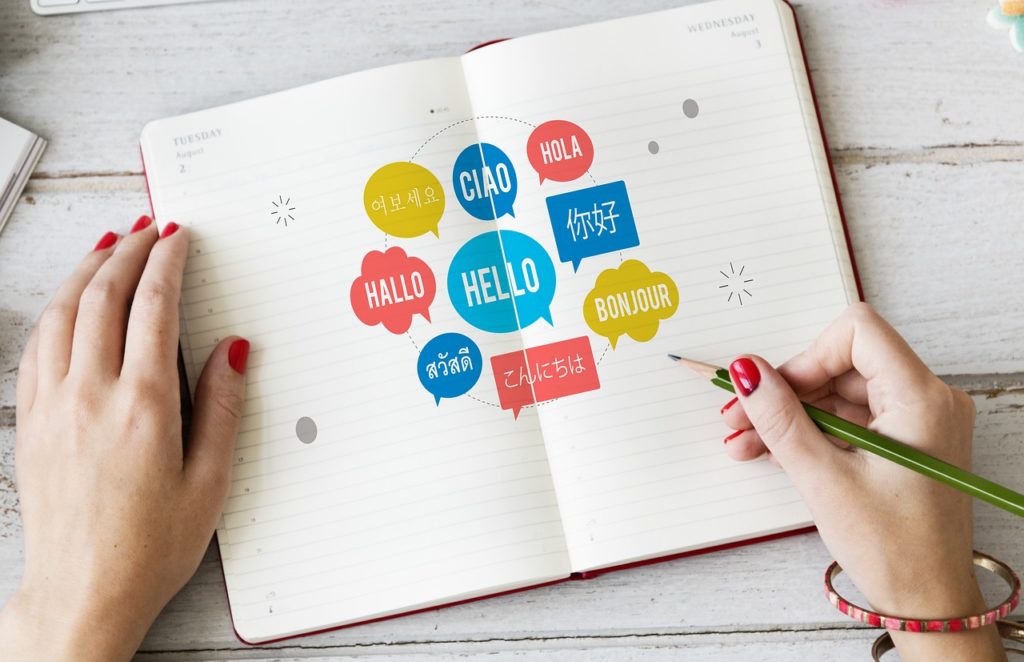
आम तौर पर माना जाता है कि एक भाषा की रचना को उसके मूल भाव और पाठ से विचलित हुए बिना, दूसरी भाषा के पाठकों के लिए सुगम, सरल भाषा में प्रस्तुत करना ही अनुवाद है। लेकिन अनुवाद क्या सचमुच ही इतनी सरल प्रक्रिया है? अनुवाद को सरल क्रिया मानना ही शायद उसके दोयम दर्जे की गतिविधि माने जाने का आधार है और शायद इसीलिए अक्सर अनुवादकों को उनके काम का श्रेय (और कभी-कभी उचित मज़दूरी भी) नहीं मिल पाता। हम जानते हैं कि ईसा से ढाई हज़ार बरस पहले मिस्र में प्रमुख अनुवादक का पद हुआ करता था, शासक की एक पदवी ‘अनुवादकों का मार्गदर्शक’ थी और अनुवादक एक सम्मानित व्यावसायिक वर्ग माने जाते थे, लेकिन इतना ही सच यह भी है कि हमें उन अनुवादकों के नाम नहीं मालूम जिन्होंने साम्राज्य भर में राजादेशों को समान रूप से समझा जाना संभव बनाने के लिए अनुवाद किए। असल में उनके नाम दर्ज ही नहीं किए गए। ओल्ड टेस्टामेंट के हिब्रू से ग्रीक में अनुवाद करने वाले लोगों के बारे में हम बस यह जानते हैं कि वे यहूदियों के बारह कबीलों के प्रतिनिधि थे, हर कबीले के 6 प्रतिनिधि यानी कुल 72 लोग, लेकिन उनके नामों के विवरण उपलब्ध नहीं हैं। बहरहाल, हम पक्के ढंग से जानते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट का हिब्रू से ग्रीक में अनुवाद करवाने वाला मिस्र का यूनानी शासक टॉलेमी द्वितीय था।
एक दार्शनिक कह चुके हैं कि दो व्यक्ति एक ही किताब को अलग-अलग ढंग से पढ़ते हैं। अक्सर ही अनुवाद के बारे में (और प्रकारांतर से अनुवादक के बारे में) शिकायत रहती है कि उसने मूल रचना के साथ पूरा न्याय नहीं किया। दूसरी ओर, विश्व साहित्य से हमारा परिचय अनुवाद के कारण ही संभव हो पाया है। अनुवाद ने संस्कृतियों और समाजों के बीच संवाद के पुल बनाए हैं। बहुत बार एक संस्कृति के कठिन तत्वों को उनसे बिलकुल अपरिचित संस्कृति से आए पाठकों के लिए बोधगम्य बनाने के लिए अनुवादक, जो दोनों संस्कृतियों/भाषाओं के बीच के उस संधिस्थल के नागरिक होते हैं जिसे ‘नो मैन्स लैंड’ कहा जाता है, निकटतम साम्य रचने वाले तत्वों का उपयोग कर लेते हैं जो पूरी तरह वही नहीं हो सकते जो मूल रचना में थे। इसे मूल पाठ से विचलन, और इस तरह अनुवाद कर्म में दोष माना जाता है। लेकिन साहित्य और साहित्यिक पुरस्कारों की दुनिया बहुत हद तक अनुवाद पर टिकी है। क्या आयरिश कवि डब्ल्यू. बी. येट्स के अनुवाद (रोचक है कि इस समर्थ कवि को टैगोर के 10 बरस बाद नोबेल पुरस्कार मिला) के बिना टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिलने की कल्पना भी की जा सकती थी? रसिकों और अनुवादकों के बीच आज भी येट्स के अनुवाद पर बहस जारी है।
क्या अनुवादक पूरी तरह अकिंचन हो सकता है?
अनुवादक से अपेक्षा रहती है कि अनूदित पाठ में उसकी सत्ता की झलक तक न रहे। यह अपने आप में एक असंभव किस्म की मांग है जो चाहती है कि कोख किराये पर देने वाली स्त्री की तरह अनुवादक भी अपने श्रम के उत्पाद पर अपने अस्तित्व के चिह्न न छोड़े। आदर्श रूप से अनुवादक अपनी मानसिक बुनावट के अनुसार किसी पाठ का अर्थान्वय अपने लिए करने के बाद उसे एक ऐसे अमूर्त, आदर्श और कल्पित पाठक के लिए व्यक्त करते हैं जिसका अस्तित्व असल में है ही नहीं, जिसे अनुवादक ने अपनी सुविधा के लिए गणित के ‘एक्स’ की तरह सिरजा है और प्रमेय/समस्या के हल हो जाने पर जो पूरी तरह त्याज्य होता है। लेकिन इसी अमूर्त पाठक (जो अनूदित पाठ के सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध होने पर अनेक ठोस, वास्तविक, सापेक्ष लोगों में बदल जाता है) की ग्रहणशीलता तय करती है कि अनूदित पाठ को कैसे आंका जाएगा। एक बहुत सरल, स्थूल उदाहरण की सहायता से बताएं तो अनुवाद का कर्म मेंहदी लगाने जैसा है (यहां मूल पाठ को अपनी भाषा की माटी में खड़े पौधे पर लगी मेंहदी की पत्तियां माना गया है जिनके गुणधर्म को दूसरी भाषा/संस्कृति में स्थानांतरित करने का काम अनुवादक का है)। मेंहदी पहले पीसी जाती है जिससे उसका भौतिक गुण बदलता है, फिर उस हथेली को साफ़ किया जाता है जिस पर मेंहदी लगनी है, फिर उस पर मेंहदी लगा दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में मेंहदी तोड़ने, पीसने और लगाने वाले व्यक्ति ने खुद का विलोपन करने का पूरा प्रयास किया होता है लेकिन क्या यह विलोपन मेंहदी लगवाने वाले के लिए भी काम करता है? मानवीय अनुभव की सीमाओं के बीच अनुवादक के व्यक्तित्व का विलोपन क्या सचमुच संभव है?
क्या अनुवादक को संपादक की भूमिका में आना चाहिए?
कुछ स्थितियों में मूल पाठ में विचारों और अवधारणाओं को राजनीतिक-सामाजिक कारणों से व्यापक प्रसार के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। ऐसे में अनुवादक, जो एक ओर मूल लेखक का प्रतिनिधि है और दूसरी ओर अनूदित पाठ की ग्राह्यता सुनिश्चित करने को संकल्पबद्ध है, क्या करे इस प्रश्न का पूरा विस्तार समझने के लिए उस दुभाषिये की कल्पना करें जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प और उत्तर कोरियाई तानाशाह किम इल जोंग के बीच बैठा है। अगर वह कुछ त्वरित संपादन न करे तो हमारे संसार को इतिहास बनते देर न लगे। लेकिन तब वह अनुवाद कर्म की संहिता का उल्लंघन कर रहा होगा। प्राचीन और सांस्कृतिक स्तर पर जटिल पाठों (जैसे पंचतंत्र और एलिस इन वंडरलैंड) को बच्चों के लिए अनूदित करते हुए अनुवादकों के सामने अक्सर ही ऐसे निर्णय लेने की स्थिति आती है।
अनुवादक किसका पक्षधर रहे, अपनी आचारसंहिता का या मूल पाठ का या सत्ता का?
आज की राजनीतिक-सामाजिक स्थितियों में अनुवादकर्म बहुत ही जटिल, कठिन हो चुका है। मूल पाठ और अपनी आचारसंहिता के प्रति निष्ठावान बने रहते हुए क्या आतंकवादी घटना के विदेशी आरोपी के दुभाषिये देश-विदेश में मौजूद उसके अज्ञात साथियों का साथ दे रहे होंगे, क्या वे आम जनता के बीच अलगाववादी विचारधारा के प्रसार में सहायक सिद्ध होंगे? अब इसी स्थिति को दूसरे कोण से देखें : मूल पाठ और अपनी आचारसंहिता के प्रति निष्ठावान बने रहते हुए क्या अंतरराष्ट्रीय/विदेशी परिवीक्षकों के लिए देश के असंतुष्ट वर्गों के दुभाषिये देश के हितों (ये हमेशा ही सत्ता द्वारा परिभाषित किए जाते हैं) के विरुद्ध काम कर रहे होंगे? इसी के साथ एक और भी प्रश्न उठता है- क्या अनुवादक/दुभाषिया गोपनीयता को हर स्थिति में बनाए रखे?
कुछ ऐसी ही स्थिति में ओल्ड टेस्टामेंट का ग्रीक में अनुवाद करने वाले यहूदी अनुवादकों ने एक अनूठा उपाय निकाला था : उन्होंने ग्रीक में अनूदित पाठों की ही एक-दूसरे से तुलना करने पर ज़ोर दिया (क्योंकि अनूदित पाठ की हिब्रू मूल पाठ से तुलना वही कर सकते थे) और घोषित किया कि दैवी प्रेरणा के फलस्वरूप अनुवाद एकदम सही हुए हैं।
अनुवादक भाव को प्राथमिकता दे या शैली को?
भावपूर्ण, गीतात्मक पाठों के अनुवादक के सामने अक्सर ही यह दुविधा आती है। हम जानते हैं कि सांस्कृतिक संदर्भों में समानार्थकता प्राप्त कर पाना कभी-कभी असंभव होता है। इसका एक उदाहरण लोकगीतों और लोकगाथाओं का अनुवाद है : भाव पर पकड़ बनती है तो शैली छूट जाती है और शैली पकड़ में आती है तो भाव की सघनता हल्की होती दिखती है।
ये अनुवादकों के सामने खड़े होने वाले कुछ मोटे-मोटे सामान्य प्रश्न हैं, वैसे तो हर पाठ अपनी ही खास चुनौतियां लिए होता है जिनके लिए नई रणनीतियां बनानी होती हैं।

मधु बी. जोशी कई दशकों से अनुवादक, कवयित्री, कहानीकार और स्तंभकार के रूप में अंग्रेज़ी और हिंदी के साहित्यिक जगत को समृद्ध करती आई हैं। वे तकनीकी अनुवाद को अपनी आय और साहित्यिक अनुवाद को रचनात्मक संतुष्टि का ज़रिया मानती हैं। उनके द्वारा अनूदित कृतियों में ‘बधिया स्त्री’ और ‘यह जीवन खेल में’ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आप उनसे madhubalajoshi@yahoo.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।
Over the last several decades, Madhu B. Joshi has enriched the Hindi and English literary worlds through her contributions as a translator, poet, story writer, and columnist. She views technical translation as a source of income that allows her to do literary translations of her choice. “Badhiya Stree” and “Yeh Jeevan Khel Mein” are among her most notable translations. She can be reached at madhubalajoshi@yahoo.co.in.
The post अनुवाद की कुछ व्यावहारिक समस्याएं appeared first on Translators of India.
]]>The post दुखवा का से कहे अनुवाद appeared first on Translators of India.
]]>
वस्तु एवं विचार के विनिमय हेतु अनुवाद का आविष्कार मानव सभ्यता के साथ ही शुरू हुआ और भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी के डैने फैलने से पहले तक इसकी नैष्ठिक पवित्रता बरकरार रही। इस दीर्घ यात्रा में यह धर्म-प्रचार, ज्ञान-विस्तार और शासन-संचालन का भी अभिन्न अंग बना रहा। आगे चलकर भारतीय ग्रन्थों के अनुवाद में अपनाई गई फिरंगी कुटिलता के कारण अनुवाद-कर्म की धारणा पहली बार शक के दायरे में आई। साम्राज्य-विस्तार की धारणा से अनुवाद करवाने की उनकी कलुषित नीति को भारत के राष्ट्रवादी बौद्धिकों ने उन्हीं दिनों उजागर कर दिया। अनुवाद की विश्वसनीयता जैसे विचार सर्वप्रथम उन्हीं दिनों अस्तित्व में आए। मगर यह बहुत पुरानी बात है।
नई बात यह है कि भूमण्डलीकरण के इस उदार वातावरण में अनुवाद का बाजार गर्म है। इससे भी अधिक नई बात यह है कि अनुवाद के बाजार के इस वर्द्धिष्णु ग्राफ को देखकर हमारे स्वदेशी बन्धु बड़े उल्लसित हैं। इस बाजार में वे अपने लिए बड़ी सम्भावनाओं की जगह ढूँढने में लिप्त हैं क्योंकि हमारे देश का शिक्षित समाज अनुवाद को लेकर बहुत बड़े भ्रम में है। उन्हें लगता है कि दो भाषाओं का सामान्य ज्ञान रखने वाला हर व्यक्ति अनुवाद कर सकता है। भ्रम यह भी है कि स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा का ज्ञान कम भी हो, तो क्या फर्क पड़ता है? डिक्शनरी तो है न! और उससे भी बड़ा सहायक, गूगल ट्रान्सलेट वेबसाइट तो है ही!…भाषा और अनुवाद के बारे में ऐसी अवहेलनापूर्ण धारणा शायद ही दुनिया के किसी कोने में हो! देश भर के कई सेक्टरों में अबूझ अनूदित पाठ की अराजकता अकारण ही नहीं है। अनुवाद के आँगन में कूद पड़े ऐसे विद्वानों को कैसे समझाया जाए कि दो भाषाओं में वार्तालाप की शक्ति भर जुटा लेने से अनुवाद की क्षमता नहीं आ जाती? उन्हें यह समझना चाहिए कि अनुवाद हेतु न केवल दोनों भाषाओं की संस्कृति, प्रकृति, प्रयुक्ति, पद्धति…का ज्ञान आवश्यक है; बल्कि पाठ के विषय, लक्षित पाठक समूह के भाषा-बोध और उनके जीवन में अनूदित पाठ की प्रयोजनीयता भी उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं। धनार्जन की लिप्सा से अलग हटकर तनिक अपने पूर्वजों की निष्ठा को याद करते तो उन्हें सब स्पष्ट हो जाता। अनुवाद के आविष्कार-काल से लेकर बीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण तक के भारतीय अनुवाद चिन्तकों एवं उद्यमियों के सारे प्रयास मानवीय, राष्ट्रीय एवं ज्ञान के प्रचार-प्रसार की धारणा से प्रेरित होते थे। अनुवाद तब तक कमाई का साधन नहीं बना था। ज्ञानाकुल समाज के हित में लोग राष्ट्रवादी भावना से अनुवाद करते थे; मान्यता, पुरस्कार मिल गया तो वाह-वाह, वर्ना सामाजिक प्रतिष्ठा को कौन रोक लेगा! किन्तु व्यापारिकता के प्रवेश ने इनकी लुटिया डुबो दी।
कुछ बरस पीछे चलकर सरकारी प्रयासों का जायजा लें तो दिखेगा कि भारतीय भाषाओं में अनूदित सामग्री जुटाने हेतु भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पी.वी. नरसिंह राव के कार्य-काल में ‘विशेष कोष’ की स्थापना हुई थी। परवर्ती काल में इस दिशा में और भी महत्त्वपूर्ण काम हुआ। जून 13, 2005 को एक उच्च-स्तरीय सलाहकार संस्था ‘राष्ट्रीय ज्ञान आयोग’ का गठन हुआ। भारत के प्रधानमन्त्री को ज्ञान-व्यवस्था-संरक्षण के क्षेत्र में सलाह देने हेतु इसकी सिफारिशों की मुख्य चिन्ता का विषय था कि इक्कीसवीं सदी की आधुनिकता की वैश्विक दौड़ का मुकाबला ज्ञान-सम्पन्नता से ही सम्भव है; क्योंकि अब आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख संसाधन ज्ञान है। स्पष्टत: भारत को अपनी समृद्ध विरासत, राष्ट्रीय निजता और विलक्षण ज्ञान-परम्परा की ओर अनुरागपूर्वक सावधान होना था। संघ लोक सेवा आयोग के सन् 2007–08 की वार्षिक रिपोर्ट का नतीजा निकला कि मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विषयों की विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई में 80-85 प्रतिशत शिक्षार्थी भारतीय भाषाओं में ही सहज रहते हैं, उसमें भी प्रमुखता हिन्दी की रहती है। स्पष्टत: भारतीय ज्ञान एवं शोध को प्रोन्नत करना अनिवार्य था और इस हेतु आने वाले समय में अनुवाद की भूमिका सुनिश्चित थी। मातृभाषा के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु पाठ्यक्रम की पुस्तकों का सभी मातृभाषाओं में अनुवाद करवाने की दिशा में पहल हुई; विभिन्न विषयों की कई दर्जन पुस्तकों का अनुवाद हेतु चयन हुआ; राष्ट्रीय अनुवाद मिशन का गठन हुआ; और भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर को इसकी जिम्मेदारी दी गई। ऐसी बात की सूचना फैलते ही अनुवादकों की सूची में शामिल होने के लिए आखेटक लोग छान-पगहा तोड़ने लगे। विचार हो कि वहाँ के प्रभारी अनुवाद हेतु आवण्टित बजट पर आक्रामक नजर गड़ाए इन उद्यमियों से अनुवाद की इज्जत कैसे बचाएँ? जोर-जबर्दस्ती से कतार में आ गए अनुवादकों से पाठ्यक्रम की बोधगम्यता, अनुवाद एवं भाषा की सहजता की रक्षा कैसे करें?
तनिक भारतीय पुस्तक बाजार की ओर रुख करें तो साफ दिखेगा कि इस समय भारत में लगभग उन्नीस हजार पुस्तक प्रकाशक हैं; जिनमें आई.एस.बी.एन. का इस्तेमाल करीब साढ़े बारह हजार प्रकाशक करते हैं। संशोधित संस्करणों के अलावा यहाँ प्रति वर्ष अनुमानत: नब्बे हजार के करीब पुस्तकें छपती हैं, इनमें आधे से अधिक हिन्दी और अंग्रेजी की होती हैं; शेष अन्य भारतीय भाषाओं की। इस संख्या का एक बड़ा हिस्सा अनूदित पुस्तकों का होता है। ये पुस्तकें भारतीय भाषाओं के पारस्परिक अनुवाद से लेकर विदेशी भाषाओं से भारतीय भाषाओं में अनुवाद तक की होती हैं। ज्ञानाकुल पाठक समुदाय के कारण इन अनूदित पुस्तकों का व्यापार भी अच्छा-खासा होता है। अंग्रेजी भाषा की किताबों के प्रकाशन के क्षेत्र में भारत की गिनती दुनिया में तीसरे स्थान पर होती है। पहले दो देश हैं–अमेरिका और इंग्लैंड। किन्तु विडम्बना है कि भारत में पनपी ‘अनुवाद एजेन्सी’ और ‘हम भी अनुवाद कर कमा सकते हैं’ की संस्कृति ने इस कर्म की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। न जाने ऐसा करते हुए भारतीय शिक्षितों का विवेक कहाँ गायब हो जाता है!
असल में भारत में अनुवाद-कर्म से जुड़े लोगों के साथ एक बड़ी विडम्बना है; इनके लिए समुचित मानदेय की कोई मानक व्यवस्था नहीं है। मोल-भाव से सारी बातें तय होती हैं। यह सौदा पूरी तरह मुवक्किल की मजबूरी और अनुवादक के कौशल पर निर्भर करता है। अनुवादक जितना अधिक ऐंठ ले, या मुवक्किल जितने कम में पटा ले। अधिकांश सरकारी संस्थाएँ आज भी पचास पैसे प्रति शब्द से अधिक अनुवाद-शुल्क नहीं देतीं; प्राइवेट संस्थाएँ उन्हीं का अनुकरण करती हैं। इस दर पर एक श्रेष्ठ अनुवादक का दैनिक भत्ता चार सौ से अधिक नहीं बनता। और यह काम भी निरन्तरता में नहीं मिलता; लिहाजा काम पाने के लिए अनुवादक को किसी न किसी बिचौलिये की तलाश रहती है। ये बिचौलिये अनुवादकों का भरपूर शोषण करते हैं, पर बिचौलिये से अनुवादक कटे तो उन्हें काम लाकर कौन दे? इस विचित्र परिस्थिति में भारतीय सांगठनिक क्षेत्र के नियन्ता तनिक सोचें कि जिस अनुवादक को वे एक हमाल की मजदूरी भी नहीं मुहैया कराते, उनसे कैसे अनुवाद की अपेक्षा करेंगे; भारतीय अनुवाद को कौन-सी दिशा दिखाएँगे और ऐसे अनुवादकर्मियों के सहारे राष्ट्रीय ज्ञान-गौरव की विरासत की रक्षा कैसे कर पाएँगे।
भूमण्डलीकृत बाजार के विस्तार से अब मानवीय उद्यम का हर आयास ‘इवेंट’ हो गया है। जीवन-यापन में बदस्तूर ‘इवेंट मैनेजमेंट’ का नया दौर आ गया है। शादी करवानी है, श्राद्ध करवाना है, पार्टी करवानी है, बच्चे को ट्यूशन पढ़वाना है, अनुवाद करवाना है…हर काम के लिए एजेन्सी है। किन्तु अनुवाद के क्षेत्र में एजेन्सी चला रहे व्यक्तियों को तनिक बुद्धि-विवेक और निष्ठा से काम लेना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि अनुवाद-कर्म व्यापार नहीं, एक मिशन है। अनुवाद हेतु दी जाने वाली राशि मेहनताना या मूल्य नहीं, मानदेय कहलाती है; ज्ञान के विकास में निष्ठा से लगे किसी उद्यमी के सम्मान में दी जाने वाली मानद राशि। संस्थाओं-संगठनों का भी दायित्व बनता है कि वे एजेन्सियों को न्यूनतम भुगतान पर अनुवादक तलाशने के लिए मजबूर न करें। फिर अनुवाद के अखाड़े में कूदने से पहले अनुवादकों को भी आत्म-मूल्यांकन करना चाहिए; इस क्षेत्र में आने की इच्छा ही है, तो कौशल जुटाएँ। गूगल ट्रान्सलेट अथवा मशीनी अनुवाद का बेशक सहयोग लें, किन्तु अनुवाद को ‘मशीनी’ न बनाएँ। श्रेष्ठ अनुवादक को वांछित पारितोषिक देने हेतु भूमण्डलीकृत बाजार तथा उनकी भाषा की सराहना करने हेतु विशाल उपभोक्ता समाज तैयार बैठा है। सरकारी नौकरी के अलावा जनसंचार, पर्यटन, व्यापार, फिल्म, प्रकाशन…हर क्षेत्र में अनुवाद की तूती बजती है। सभी देशी-विदेशी फिल्मकार भारतीय भाषाओं में अपनी फिल्म की डबिंग करवाना चाहते हैं; विभिन्न ज्ञान-शाखाओं में बड़े-बड़े विचारकों की पुस्तकें प्रकाशक छापना चाह रहे हैं; सभी उद्योगपति अपने उत्पाद का विज्ञापन सभी भाषाओं में करवाना चाह रहे हैं…इन सभी कार्यों की अपेक्षित योग्यता के बिना जो इस क्षेत्र में हाथ डालते हैं, वे सचमुच अपने देश के उपभोक्ता समाज के साथ गद्दारी करते हैं।
संसदीय कार्यवाही के निर्वचन हेतु चयनित इंटरप्रेटर का तो चयन ही इतना ठोक-ठठाकर होता है कि वहाँ के अनुवाद में किसी दुविधा की गुंजाइश सामान्यतया नहीं होती; किन्तु प्रशासनिक महकमों के प्रपत्रों, वार्षिक रपटों के हिन्दी अनुवाद; या सामाजिक जागरूकता फैलाने वाले नारों के सर्वभाषिक अनुवाद का जैसा उदाहरण सामने आता है; मालूम ही नहीं चलता कि अनुवाद हुआ किस भाषा में है? इस समय सभी संस्थानों की वेबसाइट के हिंदी अनुवाद पर जोर दिया जा रहा है। सारी संस्थाएँ मुस्तैदी से सरकारी फरमान के अनुपालन में यह काम एजेन्सी को सौंपकर निश्चिन्त हो रही हैं। धनलोलुप विवेकहीन एजेन्सी को तो कमाना है, वह न्यूनतम कोटेशन के अनुवादक के आखेट में जुट जाती है। अब बेचारे अनुवादक क्या करें! उपलब्ध अवसर का लाभ वे क्यों न उठाएँ! गूगल देवता के चरण में पाठ को रखकर वे भी प्रसाद उठा लेते हैं और एजेन्सी को सौंप देते हैं। एजेन्सी उस पाठ का मूल्यांकन जिस विद्वान से करवाती है; उन्हें क्या पड़ी है कि उसमें खोट निकालें; एक बार खोट निकाल दें तो अगली बार उन्हें काम नहीं मिलेगा। वे उसे बेहतरीन अनुवाद का तमगा दे देते हैं। चारों घर इन्जोर (उजाला) हो गया। धज्जियाँ तो भाषा की उड़ीं, जिसका कोई खेवनहार नहीं! ऐसी रामभरोसे धारणा से संचालित अनुवाद-उद्योग के गर्म बाजार पर संवेदना प्रकट करने के अलावा अन्य कुछ किया नहीं जा सकता। व्यापारिक क्षेत्र में अनुवाद के पाँव जिस तरह पसरे हैं, उसमें मामला एक सीमा तक ठीक कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ अनूदित पाठ का सीधा सम्बन्ध भुगतान करने वालों के निजी हित से है। भाषा की बोधगम्यता का परीक्षण करके ही वे भुगतान करते हैं। किन्तु जहाँ कहीं पाठ की सम्प्रेषणीयता का तत्काल परीक्षण नहीं होता, वहाँ अनुवाद की बड़ी दुर्गति है।
(यह पोस्ट देवशंकर नवीन के ब्लॉग से साभार ली गई है)

देवशंकर नवीन ने अनुवाद चिंतक, अनुवादक और शिक्षक, तीनों भूमिकाओं में अनुवाद को समृद्ध किया है। उन्होंने 200 से अधिक लेखों और ‘अनुवाद अध्ययन का परिदृश्य’ जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक के ज़रिए अनुवाद के विभिन्न पहलुओं की गहरी पड़ताल की है। वे मैथिली और हिंदी के लेखक और आलोचक के साथ ‘राजकमल चौधरी रचनावली’ के संपादक के रूप में भी जाने जाते हैं। अभी वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में प्रोफ़ेसर के पद पर कार्यरत हैं। आप उनसे deoshankarn@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।
In all three of his capacities as a translation theorist, translator, and teacher, Deoshankar Naveen has made significant contributions to translation. He has extensively examined various aspects of translation through more than 200 articles in newspapers and magazines and an important book titled “Anuvaad Adhyayan ka Paridrishya.” Apart from being a Hindi and Maithili writer and critic, he is also known for his role as the editor of “Rajkamal Chaudhary Rachnavali.” At present, he is a professor at the Center of Indian Languages at Jawaharlal Nehru University. He can be reached at deoshankarn@gmail.com.
The post दुखवा का से कहे अनुवाद appeared first on Translators of India.
]]>The post अनुवाद : विविध प्रसंग appeared first on Translators of India.
]]>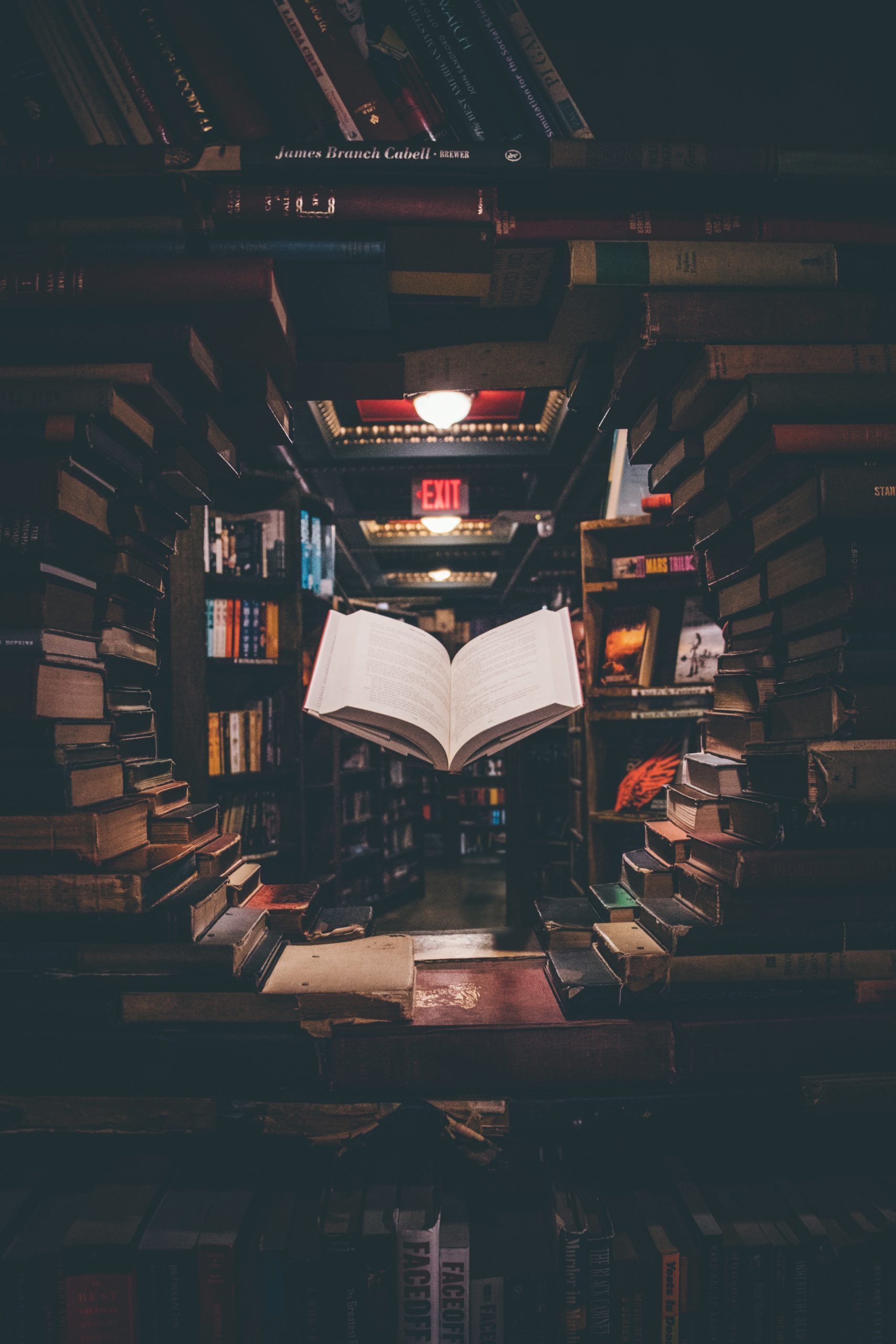
अनुवाद सदा से मनुष्यों के बीच संप्रेषण का आधार रहा है।
भारत जैसे बहुभाषी देश में औसत रूप से चैतन्य लोग एकाधिक भाषाओं में सामान्य संवाद करते रहे हैं। यहां घरों में एकाधिक भाषाओं का उपयोग भी व्यापक रहा है और भाषाओं का अलिखित वरीयताक्रम भी। पुराने संस्कृत नाटकों में प्रमुख चरित्रों और स्त्रियों और निम्नवर्गीय चरित्रों का अलग-अलग भाषाओं में बोलना और भक्तिकाल में सधुक्कड़ी की व्यापक स्वीकार्यता, भाषाविद् गणेश देवी के शब्दों में, भारत की ‘अनुवाद चेतना’ के प्रमाण हैं। भारत में भाषांतर, तर्जुमा, रूपांतर, विवर्तन, लिप्यंतरण आदि अनुवाद के अनेक रूपों का प्रचलन और भारतीय भाषाओं का साझा सूत्र संस्कृत अनुवाद को ऐसा सहज कर्म बना देते हैं कि कभी-कभी हम जान भी नहीं पाते कि कोई रचना या अवधारणा अनुवाद का परिणाम है।
हूण-शक-यवन-अरब-फारसी-यूरोपियन अपने साथ नयी भाषाएं और जीवनदृष्टियां लाए जिन्होंने भारत में पहले से प्रचलित विचारों को प्रभावित किया और औपचारिक अनुवाद की आवश्यकता भी तैयार की। अनुवाद की दृष्टि से दो महत्वपूर्ण काल- मुगलकाल और ब्रिटिशकाल थे जब भारतीय साहित्य के बड़े पैमाने पर अनुवाद हुए, विदेशी भाषाओं से भी भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुए। फिलहाल भारत सरकार ने भी एक महत्वाकांक्षी अनुवाद परियोजना की घोषणा की है जो अगर सफल हुई तो इक्कीसवीं सदी भारत में अनुवाद का तीसरा महत्वपूर्ण काल सिद्ध होगी।
बाइबल के अनुवादों ने भाषा के मानकीकरण की आवश्यकता खड़ी की तो भारतीय भाषाओं के व्याकरण और कई मामलों में, खासतौर पर आदिवासी भाषाओं की, लिपियां भी नियत हुईं। यह काम यूरोपियन विद्वानों ने किया। भारत में भाषा विचार की संवाहक मानी जाती थी और संदर्भ के अनुसार नये शब्द गढ़ना और शब्दों के अलग-अलग अर्थ लगाना आम प्रचलन था। इस तरह अनुवाद एक व्यक्तिनिष्ठ क्रिया थी जो अनुवादक के व्यक्तित्व की परिचायक भी थी। मोटे तौर पर भारत में, एक अच्छा अनुवाद मूल पाठ के रस और ध्वनि को संप्रेषित करता था (दरअसल यह भी अनिवार्य नहीं था। अनुवादक अक्सर ही पुनर्पाठ भी करते थे और इस प्रक्रिया में मूल पाठ से काफी विचलन भी हो जाता था। भारत में प्रचलित अनेक रामायणें और महाभारत इसके उदाहरण हैं। मूल पाठ की दूसरी भाषा में जस की तस प्रस्तुति पश्चिम से आई अवधारणा है)। इसलिए अनुवादक का मूल पाठ और अनूदित पाठ की भाषाओं के अलावा उन से जुड़ी संस्कृतियों से भी सुपरिचित होना जरूरी बना। यहां एक समस्या सामने आती हैः अलग-अलग भाषा-संस्कृति से जुड़े पाठकों के लिए अनूदित पाठ की ग्रहणीयता। इसके प्रमुख उदाहरण श्री अरविंद द्वारा संस्कृत से अंग्रेजी में किए गए और टैगोर द्वारा अपनी ही बांगला कविताओं के अनुवाद हैं जिन्हें भारतीय पाठकों ने दुरूह और मूल पाठ से अलग पाया।
एक और समस्या (जो कम से कम अंग्रेजी में अनुवाद के मामले में दिखती है) है अनुवादक का अक्सर भारतीय भाषा की रचना के साथ अतिरेकी किस्म की छूटें लेना। यह भाषाओं के सत्ता समीकरण के चलते होता है। भाषाओं के सत्ता समीकरण के चलते ही भारतीय भाषाओं में एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद बिना अंग्रेजी की मध्यस्थता के कठिन होता जा रहा है।
अनुवाद को मूल लेखन से हीन मानने की प्रवृत्ति कोई नयी बात नहीं है।
इस के पीछे वह उपनिवेशवादी मानसिकता काम करती है जो मानती है कि हमारी अपनी संस्कृति, ज्ञान और भाषा से श्रेष्ठ कुछ कहीं नहीं है, जो भी उस से इतर है वह बर्बर या हीन है, उस से न सीखने की जरूरत है और न उसे सिखाने की। और इसलिए दूसरी भाषाओं की कृतियों का अपनी भाषा में अनुवाद करना हो या अपनी भाषा की कृतियों का दूसरी भाषाओं में, अनुवादकर्म को मौलिक लेखन से हीन माना गया। प्राचीन ग्रीक और रोमन इस विचार के पोषक थे।
लेकिन जब राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना हो तब अनुवाद ही वैतरणी पार करवाता है। अनुवाद संस्कृतियों और भाषाओं के बीच सेतु रचता है। जब मिस्त्र में रोमन साम्राज्य को स्थानीय यहूदी समाज (ईसा यहूदी ही थे) के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और औपनिवेशिक शासकवर्ग और उपनिवेश के बीच कुछ सद्भाव तैयार करने की जरूरत पड़ी तो ईसा से ढाई सदी पहले, टॉलेमी ने यहूदी धर्मग्रंथ का हिब्रू से ग्रीक में अनुवाद करवाया जिसे ईसाई परंपरा में ओल्ड टैस्टामेंट कहा जाता है।
सीरिया के प्राचीन नगर एब्ला में मिली 2500 ईस्वीपूर्व और 2250 ईस्वीपूर्व के बीच की 1800 मिट्टी की पट्टिकाओं पर सुमेरियन और स्थानीय एब्ला भाषा में अंकित दस्तावेज इस नगर के समृद्ध इतिहास की गवाह हैं।
बहुभाषी अंकनों का सब से प्रसिद्ध उदाहरण तीन लिपियों, प्राचीन मिस्त्री चित्रलिपि, मिस्त्री लिपि और प्राचीन ग्रीक में जारी 196 ईस्वीपूर्व का एक आदेश रोजेट्टा स्टोन है जो अपने आप में किंवदंती बन चुका है। यह लिपि के विकास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है।
——————————————————–
अनुवाद के लिखित इतिहास की दृष्टि से मिस्त्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ईसा से 3000 बरस पहले स्थापित हुआ यह राज्य अनेक भाषाई और जातीय समूहों का संगठन था। बाद में यह लंबे समय तक फारसियों और फिर रोमनों के अधीन रहा। जाहिर है कि राजकाज दुभाषियों और अनुवाद के बिना संभव नहीं हो सकता था, दरबार, मंदिर और बंदरगाह अनुवाद के महत्वपूर्ण ग्राहक थे। ईसा से पांच सदी पहले मिस्त्र आए ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने वहां के दुभाषियों और अनुवादकों को एक सम्मानित जाति बताया। ईसा के जन्म से कम से कम एक हजार बरस पहले ‘प्रमुख अनुवादक’ का पद मिस्त्र में विद्यमान था। बेबीलोन के प्रशासक के फराओ को लिखे एक पत्र में अनुवादकों के राजनयिक दल में शामिल होने का उल्लेख है। असीरियनों, हेट्टों और बेबिलोनवासियों से मिस्त्री व्यापार फला-फूला तो विदेशी भाषाओं में किताबत करने वालों के प्रशिक्षण के लिए बाकायदा व्यवस्था बनी। सिकंदर की मिस्त्र पर विजय के बाद ग्रीक अनुवाद की जरूरत बढ़ी। बहुत से राज्यादेश दो या अधिक भाषाओं में जारी किए जाते थे।
अनुवाद का व्यावहारिक अर्थ है किसी विचार को दूसरी भाषा में व्यक्त करना।
यह कोई बहुत सूत्रबद्ध गतिविधि नहीं है। इसका मोटा-मोटा संचालक निर्देश बस यही है कि अनूदित पाठ में मूल पाठ का अर्थ, भाव और सौंदर्य (बिलकुल इसी वरीयताक्रम में) बने रहें। लेकिन दिक्कत यह है कि हर भाषा में कुछ शब्द और अवधारणाएं ऐसी होती हैं कि उन्हें दूसरी भाषा में अनूदित करना टेढ़ी खीर और यहां तक कि असंभव माना जाता है (उदाहरण के लिए, हिंदी या किसी भी भारतीय भाषा के ऐसे वाक्यांशों का अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए अनुवादक अक्सर पनाह मांग जाते हैं जिनमें सामाजिक संबंधों, खासतौर पर जीजा-देवर, भाभी-साली का उल्लेख हो!) ऐसी स्थिति में अनुवादक अक्सर अपने विवेक से काम लेते हुए उपयोगी पाठ तैयार कर लेते हैं।
लेकिन, अनुवाद को दोयम दर्जे का काम घोषित करते हुए भी आलोचक उसकी कमियों को इंगित करने में काफी मेहनत करते हैं। बाइबल की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर बहस का आधार आरामेइक और हिब्रू शब्दों से लैटिन में हुए ‘गलत’ अनुवाद हैं।
बहसें विवादों में बदलती हैं तो नये पंथ बनते हैं….. कैथोलिक और प्रोटैस्टैंट मतों के विभाजन ने ईसाई यूरोप पर चर्च की निर्विवाद जकड़ को तोड़ने के साथ ही नए सत्ता-समीकरण भी गढ़े।
हमारी दुनिया को एक सूत्र में पिरोता अनुवाद
चौदहवीं सदी में जब इतालवी लेखक और पुनर्जागरण युग के महत्वपूर्ण मानवतावादी ज्योवानी बोकात्चियो ने मौखिक परंपरा और लैटिन और फ्रेंच स्रोतों से पाई कुछ कहानियों को अपने ढंग से ‘डेकामेरॉन’ नाम की किताब के रूप में प्रस्तुत किया तो यह जनसामान्य के दैनंदिन ज्ञान और नैतिकता पर चर्च के एकाधिकार के मुखर प्रतिरोध का सूत्रपात करने वाली घटना बनी (उससे पहले तक लोकसाहित्य किताबों के रूप में नहीं छपता था। यूरोप में ग्रीक और लैटिन, हमारे देश में संस्कृत की तरह, शास्त्रीय ज्ञान की भाषाएं मानी जाती थीं)। जल्दी ही बोकात्चियो की कृति के अंग्रेजी सहित यूरोप की सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद और रूपांतरण प्रकाशित हुए, यहां तक कि लोक ने उसे एक महत्वपूर्ण शैक्षिक उपकरण का दर्जा तक दिया।
बोकात्चियो को ये कहानियां भले ही यूरोप की परंपरा से मिलीं लेकिन इन का उत्स फारस, अरब और भारत जैसे देश थे जहां ये सदियों से मौखिक और लिखित परंपराओं में प्रचलित थीं। भारत से फारस और अरब होते हुए यूरोप पहुंचे बनजारे पंचतंत्र, कथासरित्सागर, जातक कथाओं का समृद्ध कोश साथ ले गए थे। वे जिस राह से गुजरे कहानियों के बीज बोते चले जिन्होंने स्थानीय बोली-मिट्टी में जड़ें पकड़ लीं। अरब, ग्रीक और भारतीय व्यापारी समुदायों के मेलजोल ने भी साहित्य और ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगभग पूरे संसार में उपयोग हो रहे आधुनिक रोमन अंक, गणित, रेखागणित और खगोलशास्त्र के महत्वपूर्ण सूत्र और ज्योतिष की कुछ अवधारणाएं इस आदान-प्रदान के साक्ष्य हैं।
साहित्य और ज्ञान के प्रसार में, अपरिहार्य लेकिन अनदेखी सी कर दी गई, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अनुवाद की रही। उदाहरण के लिए, पंचतंत्र की जिन कहानियों के कथासूत्रों का बोकात्चियो ने उपयोग किया वे उन तक पुराने फारसी, अरबी, हिब्रू अनुवादों की एक प्राचीन परंपरा द्वारा पहुंचे थे। ईसा की पहली सदी में लिखी गई यहूदी धर्मग्रंथ तालमुद की टीकाओं में पंचतंत्र के कथासूत्रों के उपयोग का विस्तृत दस्तावेजीकरण उपलब्ध है। पशु-पक्षियों के माध्यम से नीति का ज्ञान देने वाली ईसप की कहानियां जातक कथाओं और पंचतंत्र से उठाई गई मानी जाती रही हैं। आधुनिक अध्येताओं ने पाया कि ईसप की कहानियों के सूत्र प्राचीन सुमेर और अक्काद साहित्य में ईसा से तीन हजार बरस पहले मौजूद थे। इस खोज ने एक नये प्रश्न को जन्म दिया है- ये कहानियां भारत से ग्रीस पहुंचीं या ग्रीस से भारत?
बहरहाल, अपनी लंबी यात्राओं और अपसरण में इन कहानियों में जो नहीं बदला वह है इनका नीति का बोध करवाने वाला चरित्र और प्रकार्य। समाजशास्त्री फूको का कहना है कि शिक्षा निरपेक्ष गतिविधि बिलकुल नहीं है, कोई भी समाज व्यवस्था उन्हीं मूल्यों को समर्थन देती है जो उसकी राजनीतिक-सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति में साधन बनते हैं। अनुवाद के साथ भी कुछ ऐसा ही है। सत्ता केवल अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने में सहायक अनुवाद और ज्ञान को प्रश्रय देती है। पंचतंत्र की कथाएं स्थिति के अनुरूप चुनाव को आदर्श विकल्प के रूप में प्रस्तुत करती हैं। वे उस नैतिकता की पक्षधर नहीं हैं जिसकी आकांक्षा रखना आज हम एक आदर्श के रूप में सीखते हैं, वे तो खुद को केंद्र में रखते हुए हर हाल में खुद को बचा ले जाने की सीख देती हैं। ये कहानियां राजपुत्रों को सफल-समर्थ शासक बनने को प्रेरित करने के लिए चुनी गई थीं। इनकी चरम परिणति राजपुरुषों के आदर्श व्यवहार और आचरण के बारे में राजनीतिक विचारक मैकियावेली के लेखन में होती दिखती है।
16वीं सदी में पोप पायस छठे ने लैटिन में ईसप की कहानियों को कविता के रूप में प्रस्तुत करने वाला एक संग्रह तैयार करवाया ताकि ‘बच्चे एक ही किताब से शुद्ध भाषा और नीति सीख लें।’ 17वीं सदी में फ्रांस के राजा लुइ 16वें ने अपने 6 बरस के बेटे को शिक्षित करने के लिए 38 कहानियों की शिक्षाओं को निरूपित करने वाले मूर्तिशिल्प बनवाए। और तो और, 1730 में बच्चों के लिए, इन नीतिकथाओं के ला फांतें के किए फ्रेंच रूपांतरण पर आधारित, लोकप्रिय धुनों से सजी संगीत नाटिकाएं भी प्रकाशित हुईं जिनका उद्देश्य और लक्ष्य था ‘बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप शिक्षा देना और उन्हें उन भोंडे गीतों से विमुख करना…जो उनकी निश्पापता को भ्रष्ट करते हैं।’ यूरोपियन उपनिवेशवादियों का अपने शैक्षिक उद्यमों के माध्यम से एशिया और अफ्रीका में ईसप की कहानियों को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध करवाना ऐतिहासिक विडंबना थी क्योंकि इन के कथासूत्र इन समाजों के लोकसाहित्य में पहले ही उपस्थित थे।
भाषाविदों-यात्रियों-व्यापारियों-मिशनरियों के उद्यम से आज ईसप की कहानियों के रूप में जातक कथाओं और पंचतंत्र के अनुवाद-रूपांतरण भारतीय, पश्चिमी और मध्य एशियाई भाषाओं के अलावा चीनी, जापानी और मेक्सिको की लोकभाषा नाउत्ल में भी उपलब्ध हैं।
————
धर्म के चेहरे को बदलने और उसे अधिक लोकोन्मुख और सर्वसुलभ बनाने में अनुवाद की भूमिका के दो बड़े उदाहरण हैं रामायण और बाइबल के 16वीं सदी में आए संस्करण। इन ग्रंथों ने अपनी भाषा और युग को नए शब्द, नए मुहावरे और नई अवधारणाएं तो दी हीं, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की प्रक्रिया को भी प्रभावित किया। आज अगर धर्म पर सार्वजनिक बहस संभव है तो उसकी पीठिका इन्हीं अनुवादों ने तैयार की है।
बाइबल के शुरुआती जर्मन और अंग्रेजी अनुवाद करने वाले मार्टिन लूथर और विलियम टिंडेल हिब्रू-ग्रीक और लैटिन जैसी शास्त्रीय भाषाओं के अधिकारी विद्वान और धर्मशास्त्री थे (बाइबल के उनके अनुवाद इस ग्रंथ के हिब्रू-ग्रीक पाठों पर आधारित थे) तो रामायण का पुनर्पाठ करने वाले तुलसीदास संस्कृत के अधिकारी विद्वान और धर्मशास्त्री थे। लेकिन अपने युग और समाज के लिए, अभी तक अभिजातवर्ग तक सीमित रहे और ज्ञान के समानार्थक बन चुके शास्त्रीय ग्रंथों को लोक के लिए सुलभ बनाने के लिए तीनों ने ही जन की भाषा को आधार बनाया। धर्मध्वजवाहकों ने इन अनुवादों को धर्मविरुद्ध घोषित किया क्योंकि वे धर्मग्रंथों के एक वर्ग विशेष द्वारा ही लिखे-पढ़े और व्याख्या किए जाने की परंपरा से जबर्दस्त विचलन थे।
इन तीनों अनुवादों ने अभिजातवर्ग का विशेषाधिकार बन चुके शास्त्रीय ज्ञान को जनसाधारण के लिए सुलभ बनाकर विशेषाधिकार और ज्ञान पर एकाधिकार को एक झटके में तोड़ दिया।
दरअसल इस आंदोलन की शुरुआत पहले ही जर्मन बोलियों में लैटिन स्तोत्रों के अनुवाद और भारतीय बोलियों में भक्ति और ज्ञान के पदों की रचना से हो चुकी थी। इनमें से बहुत सी रचनाओं में विचार के स्तर पर शास्त्रीय धर्मग्रंथों की अनुगूंज सुनाई देती है लेकिन सच यह भी है कि इनके रचनाकार, कम से कम भारत में, ज्यादातर परंपरागत शास्त्रीय ज्ञान से दूर रखे गए वर्गों से थे।
ये सभी रचनाएं पुरोहित वर्ग के अनुष्ठानों को मुक्ति का साधन बताने के विरुद्ध स्वर उठाते हुए मनुष्य के व्यक्तिगत कर्म को, मनुष्य के देवताओं को समर्पण के बरक्स मनुष्य के जीवमात्र के प्रति करुणाभाव को सर्वोच्च मान रही थीं जिससे पुरोहित की जरूरत और वैधता ही संदेह के दायरे में आ गई। जीवमात्र के प्रति करुणाभाव कोई नई अवधारणा नहीं थी। ईसाई संत फ्रांसिस और बुद्ध ने करुणा का उपदेश बहुत पहले दिया ही था लेकिन पुरोहितवर्ग ने उसे ईश्वर और ईसा का विशेष लक्षण बना दिया था।
यूरोप में बाइबल के अनुवादों को यूरोप की राजसत्ताओं पर रोमन कैथोलिक चर्च की कड़ी जकड़ को तोड़ने वाली घटना माना जाता है जिसने आखिर अरब में ईसाई और मुसलमान सेनाओं के बीच चलने वाले धर्मयुद्धों को लगभग खत्म कर दिया। भक्ति काव्य ने हिंदू धर्म के आधार, चतुर्वर्ण की अवधारणा पर पुनर्विचार किए जाने की जरूरत को रेखांकित किया और यह क्रम अब भी जारी है।
—————
अनुवाद जैसा निरापद, निरीह लगने वाला कर्म अपने साधक के लिए खतरनाक क्यों और कैसे बन जाता है?
जवाब हैः जब वह व्यवस्थित धर्म और राजनीति के निशाने पर आता है। 14वीं सदी में वल्गेट के नाम से जानी जाने वाली लैटिन बाइबल के पहले अंग्रेजी अनुवादक जॉन वायक्लिफ की चर्च से तनातनी उनके जीवनकाल में तो चलती ही रही, उनके मर जाने के बाद पोप मार्टिन पांचवें के आदेश पर उनके अवशेष कब्र से निकाल कर जलाए गए। विलियम टिंडेल को ईशनिंदक बता कर सूली चढ़ाया गया।
हमारे देश में, तुलसीदास जीवनभर वाराणसी के विद्वत्वर्ग के कोपभाजन बने रहे। मार्टिन लूथर के सिर पर इनाम था। दारा शिकोह के किए संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद औरंगजेब के लिए उसे धर्मद्रोही घोषित करने का कुछ स्वीकार्य सा लगता कारण बने।
16वीं सदी के पूर्वार्ध में चर्च की छद्म न्याय-गवेषण प्रक्रिया इंक्विजिशन पर प्रश्न उठाने वाले फ्रेंच मुद्रक, अनुवादक और लेखक एतीन दोल को ईशनिंदक और धर्मविरोधी घोषित करके उनकी छापी किताबों के साथ जिंदा जला दिया गया था। अब माना जाता है कि चर्च को उन्हें राह से हटाना जरूरी लगा क्योंकि वे धर्मग्रंथों को लैटिन के बजाय अपनी भाषा में पढ़ने की वकालत कर रहे थे।
1991 में सलमान रश्दी की सैटेनिक वर्सेज के जापानी अनुवादक हितोशी इगाराशी की हत्या इस कड़ी में सब से नया उदाहरण है। सैटेनिक वर्सेज के खिलाफ अयातुल्ला खुमैनी के फतवे के बाद हुई उनकी हत्या आज भी एक अनसुलझी गुत्थी है। कहा जाता है कि सैटेनिक वर्सेज के गड़े मुर्दे को फिर से न जिलाने के चक्कर में जापान की सरकार ने उनके बांगलादेशी हत्यारे के प्रत्यार्पण का प्रयास तक नहीं किया।
——————
लैटिन से अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले कुछ शुरुआती अनुवादक अपने-अपने क्षेत्रों में बहुत नाम कमा चुके थे। राजा अल्फ्रेड (849-899) कुशल प्रशासक और सेनानायक होने के साथ ही शिक्षा और साक्षरता के संवर्धक भी थे। उन्होंने महत्वपूर्ण लैटिन ग्रंथों के अनुवाद करवाने के साथ ही खुद भी कुछ धार्मिक पाठों के अनुवाद किए। जेफ्री चॉसर (1343-1400) राजनयिक, दार्शनिक, खगोलशास्त्री और कवि के साथ ही अपने युग के महत्वपूर्ण अनुवादक भी थे। अंग्रेजी की पहली किताब ‘हिस्टरी ऑफ ट्रॉय’ के मुद्रक विलियम कैक्सटन (1415-1491) ने ही उसे फ्रेंच से अंग्रेजी में अनूदित भी किया था। उन्होंने कुल 25 किताबों का अनुवाद किया।
————————-
भारत में राजा अल्फ्रेड का समकक्ष उदाहरण दारा शिकोह हैं। औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह अपने पिता शाहजहां के घोषित उत्तराधिकारी और इलाहाबाद और गुजरात के सूबेदार थे। आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले इस विद्वान राजपुरुष ने खुद उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। कहा तो यह भी जाता है कि दारा ने तुलसीकृत रामचरितमानस का भी फारसी में अनुवाद किया था। कुछ बरस पहले जम्मू के एक व्यापारी को अपने घर में 1889 में रावलपिंडी के मुंशी चिरागदीन सिराजदीन प्रेस से छपी ‘रामायण नज्म खुशतर’ की प्रति मिली जो दारा का किया तुलसीकृत रामचरितमानस का फारसी अनुवाद है।
—————–
रेनेसां को अनुवाद का युग कहा जाता है। यूरोप की प्रमुख भाषाओं में प्राचीन ग्रीक और लैटिन ग्रंथों के अनुवाद हुए तो भारत में भी मुगल शासकों ने संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद करवाए। अकबर ने बहुभाषी अधिकारी विद्वानों से वाल्मीकि रामायण, महाभारत, राजतरंगिणी, अथर्ववेद, द्वात्रिंशत पुत्तलिका आदि के फारसी अनुवाद करवाए। उन के नवरत्नों में से एक, अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद किया तो अबुल फजल के भाई और अकबर के दरबारी फैजी ने नल-दमयंती आख्यान का।
अनुवाद की प्रक्रिया ने दुनिया को नयी लिपियां, भाषाएं और साहित्य दिए। चौथी सदी में बिशप अलफिला ने बाइबल का ग्रीक से गॉथिक भाषा में अनुवाद किया जो हमारी बहुत सी बोलियों की तरह, पूर्वी यूरोप के बड़े भूभाग में लिखी नहीं, केवल बोली जाती थी। तो हुआ यह कि बिशप अलफिला को गोथिक की लिपि तैयार करनी पड़ी। उन्हीं के लगभग समकालीन संत मेस्रॉप माशटॉट्स को भी इन्हीं कारणों से, यही कवायद आर्मीनियन भाषा के साथ करनी पड़ी।
भारत और अफ्रीका में बहुत सी आदिवासी भाषाओं की लिपियां भी ऐसे ही नियत हुईं। लिपियां बनीं तो इन भाषाओं के मौखिक साहित्य का दस्तावेजीकरण हुआ और इन में लिखे जा रहे साहित्य के दूसरे भाषाभाषियों द्वारा पढ़े जाने का क्रम बना जिससे भाषाओं के बीच संवादसेतु बने।
तोलेदो में अरबी ग्रंथों के लैटिन अनुवाद के दौरान बहुभाषी जनता और अतिथि विद्वानों के बीच संवाद से तैयार हुई खिचड़ी भाषा ने अंततः स्पेनिश की विशिष्ट कैस्टिलियन बोली का रूप लिया। कुछ ऐसी ही कहानी भारत में उर्दू और कैरिबियन द्वीपों की खास अंग्रेजी और दुनियाभर में अनेक क्रियोल बोलियों के विकास की है।
————–
अरबों के किए अनुवादों ने शास्त्रीय ग्रीक ज्ञान को बचाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 8वीं से 10वीं सदियों के बीच ईरान में जुंदिशपुर में एक बड़ी अनुवाद परियोजना चली जहां ग्रीकभाषी ईसाई, हिब्रूभाषी यहूदी और संस्कृतभाषी भारतीय विद्वान अरबी अनुवादकों के साथ मिलकर अपनी-अपनी भाषाओं के ग्रंथों के अरबी अनुवाद तैयार करते थे। 9वीं सदी में, इस्लामी स्वर्णयुग के चरम पर, खलीफा हारून अल-रशीद ने बगदाद में बैत अल-हिकमत की स्थापना की जहां कला, वास्तुशिल्प, खगोल, रसायनशास्त्र, चिकित्सा, संगीत, दर्शन, समाजशास्त्र और नीति के ग्रंथों के अरबी में अनुवाद हुए। हारून अल-रशीद के राज्य की सीमाएं चीन, अविभाजित भारत, तुर्की और भूमध्यसागर तक फैली थीं। शास्त्रीय ग्रीस, फारस, भारत के साथ वैचारिक संवाद ने अरब मुस्लिम जगत को हिंदू, जरथुस्त्री, बौद्ध और ईसाई दृष्टियों से परिचित करवाया। परिणामस्वरूप, ग्रीक दार्शनिकों और गणितज्ञों के साथ ही भारतीय चिकित्साशास्त्र, गणित, चीनी रसायनशास्त्र, फारस के प्रशासन और कृषि के ग्रंथों के अरबी में अनुवाद हुए।
11वीं सदी के अंतिम दौर में अरबों से स्पेन छीन लिए जाने पर तोलेदो ईसाई और इस्लामी जगतों को जोड़ने वाली कड़ी बना। स्पेन आठवीं सदी के दूसरे दशक से अरब उपनिवेश था और यहां अरबी, हिब्रू और लैटिन में पढ़ने-लिखने की समृद्ध परंपरा थी। इस्लामी स्वर्णयुग में अनूदित ग्रीक दार्शनिकों की रचनाओं के अलावा भारतीय, फारसी और चीनी दार्शनिकों और वैज्ञानिकों का लेखन भी अनुवाद के माध्यम से उपलब्ध होने के कारण यहां के अरबी पढ़ने-लिखने वालों को वह प्राचीन ज्ञान सहज उपलब्ध रहा जो यूरोप और बाकी जगहों पर उपलब्ध नहीं था। यही कारण था कि 10वीं सदी के अंत से यूरोप के अध्येता यहां आते रहे। 12वीं सदी के पूर्वार्ध में यहां के आर्कबिशप मुहम्मद रजा की पहल पर अरबी पांडुलिपियों से दर्शन, इतिहास, खगोल, संगीत, रसायनशास्त्र, चिकित्सा, गणित, रेखागणित, बीजगणित, ज्योतिष और काव्य के लैटिन में अनुवाद किए गए। पश्चिम के इतिहास में यह अनुवाद की सबसे बड़ी परियोजना थी।
—————-
एक भारतीय पहल ने दिखाया है कि अनुवाद और प्रौद्यौगिकी का मेल खतरे में पड़ी भाषाओं के लिए संजीवनी सिद्ध हो सकता है। प्रथम बुक्स के खुले डिजिटल मंच स्टोरीवीवर पर लेखक, अनुवादक, संपादक और चित्रांकन विशेषज्ञ बच्चों के लिए उपयोगी सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। इस सामग्री को कोई भी क्रिएटिव कॅामन लायसेंस के अंतर्गत डाउनलोड और इस्तेमाल कर सकता है।
हिमाचल प्रदेश में एक तिब्बती स्कूल में अंग्रेजी के अध्यापक तेनजिन धारग्याल बच्चों के लिए तिब्बती में पाठ्यसामग्री उलब्ध न होने से परेशान थे। फेसबुक पर स्टोरीवीवर के बारे में जानने पर उन्होंने फेसबुक पर अपने मित्रों-सहकर्मियों को इस स्रोत के बारे में बताया और सुझाव दिया कि इन में से कुछ कहानियों को तिब्बती में अनुवाद करके कक्षा में इस्तेमाल किया जाए, संभव हो तो एक रचनात्मक गतिविधि के रूप में छात्रों को भी अनुवाद के काम से जोड़ा जाए। धर्मशाला के तिब्बती स्कूल के मुख्याध्यापक तेनजिन दोर्जी ला और उनके छात्रों ने दो कहानियों का अनुवाद किया, धर्मशाला स्थित लायब्रेरी ऑफ टिबेटन वर्क्स एंड आर्काइव्स के डॅा चॅाक और तेनजिन धारग्याल के ही स्कूल में पढ़ा रहे जिग्मे वांग्डेन ने भी कुछ अनुवाद किए। तेनजिन धारग्याल और बहुत से दूसरे तिब्बती अध्यापक अपने छात्रों को ये कहानियाँ पढ़ने को दे रहे हैं।
वर्ल्ड कोंकणी सेंटर और कोंकणी भाषा मंडल भी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, उत्तरी केरल, दादरा एवं नागर हवेली और विदेशों में फैले कोंकणी बच्चों के लिए बाल साहित्य उपलब्ध करवाने के लिए कहानियों के कोंकणी अनुवाद के अलावा मौलिक कहानियाँ भी स्टोरीवीवर पर अपलोड कर रहे हैं।
बिहार में बहुत सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली सूरजपुरी बोली कभी बंगाल से वहां आकर बसे मुसलमान समुदाय की भाषा है जिस पर बांग्ला का बहुत असर दिखता है। यह जल्द ही विगत इतिहास का हिस्सा बन जाती लेकिन कुछ प्रयासधर्मी लोग स्टोरीवीवर का उपयोग करके बच्चों के लिए सूरजपुरी को जिलाए रखने के उद्यम में लगे हैं।
सदियों पहले गुजरात के सौराष्ट्र से मदुरै, तमिलनाडु में आ बसा छोटा सा गुजराती समाज देवनागरी लिपि के माध्यम से सौराष्ट्री बोली को बचाए हुए था। आज 19 लाख से भी कम जनसंख्या वाला यह समाज कर्नाटक और आंध्र-तेलंगाना के अलावा देश-विदेश में फैला है। बच्चों के लिए सौराष्ट्री में साहित्य उपलब्ध न होना इस समाज के लिए एक बड़ी समस्या बन रहा था। पवित्रा सोलै जवाहर ने भी स्टोरीवीवर का उपयोग बच्चों के लिए किताबें लिखने और अनूदित करने के लिए किया। जल्द ही ये किताबें छपे रूप में भी बच्चों को मिलने लगेंगी।
कुर्दी भाषा बोलने-बरतने वाले लोग राजनीतिक और सैन्य परिस्थितियों के कारण दुनिया भर में बिखर रहे हैं। उनकी भाषा पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। ईरान के करमानशाह जिले के भाषाविज्ञानी मुहम्मद रजा बहादुर लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी दक्षिणी कुर्दी के माध्यम से साक्षरता बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

मधु बी. जोशी कई दशकों से अनुवादक, कवयित्री, कहानीकार और स्तंभकार के रूप में अंग्रेज़ी और हिंदी के साहित्यिक जगत को समृद्ध करती आई हैं। वे तकनीकी अनुवाद को अपनी आय और साहित्यिक अनुवाद को रचनात्मक संतुष्टि का ज़रिया मानती हैं। उनके द्वारा अनूदित कृतियों में ‘बधिया स्त्री’ और ‘यह जीवन खेल में’ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आप उनसे madhubalajoshi@yahoo.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।
Over the last several decades, Madhu B. Joshi has enriched the Hindi and English literary worlds through her contributions as a translator, poet, story writer, and columnist. She views technical translation as a source of income that allows her to do literary translations of her choice. “Badhiya Stree” and “Yeh Jeevan Khel Mein” are among her most notable translations. She can be reached at madhubalajoshi@yahoo.co.in.
The post अनुवाद : विविध प्रसंग appeared first on Translators of India.
]]>The post Gendered Languages in Game Localization appeared first on Translators of India.
]]>
What makes gendered languages hard to handle in game localization?
1. Lack of context
If you’re translating games, you already know that the lack of context is very common and can cause many problems. One of these problems is a lack of knowledge about the gender of things mentioned, like when a character says “look at that!” Translating may appear easy in such situations. However, the word ‘that’ could have diverse meanings, depending on the gender it represents. In Arabic, for example, there are at least 3 options to convey the word “that”, depending on what it refers to and its grammatical number.
2. Space
When your target language has more than one pronoun to refer to the addressee depending on their gender, it could be a nightmare because some games address all genders, and if you’re translating from English, “you” is just a three-character word that applies to all genders of all numbers. This could result in exceeding the character limit.
3. Placeholders
It’s very common to deal with placeholders in game localization. They could cause a problem when your target language requires adding prefixes depending on the gender of the word replaced by the placeholder. So, you need to know that placeholder and its number if it’s needed to convey an accurate meaning of the sentence.
4. Multiple characters in the game
Problems arise when there is a game that has many characters and there is no specific script for which characters will be in a particular situation. Sometimes you can start a mission in the game and some characters die during the mission. The text should be neutral to suit whatever happens in the mission because you will never know which characters survive or their gender and number.
How can such a problem be handled carefully?
The only possible solution is to use a gender-neutral style as much as you can. If your target language depends on using direct speeches and pronouns, try to tweak the sentence to convey the meaning. For some languages, resorting to nouns instead of adjectives is a good option.
By Eman Abdo

Eman Abdo is an English to Arabic translator specializing in localization and transcreation, mainly in marketing and game localization. She is also the author of Egypt Localization Guide and the force behind the localization of so many apps and games in Arabic and a gamer at core aspiring to change the way Arabic is represented globally. You can reach her at emanabdo.eman12@gmail.com.
The post Gendered Languages in Game Localization appeared first on Translators of India.
]]>The post A Translator’s World: Challenges and Surprises appeared first on Translators of India.
]]>
Perhaps you want to get into it but are doubtful whether to go for it or not. Well! I can’t tell you what to do, but I can share with you what I feel as a translator.
It’s different
It was not like this before. I was busy doing something else that involved similar kinds of jobs every day. Yes, I needed to perform some research and there were also follow-ups involved, but once a process was set up, I could follow it again and again, until a new challenge came up. But once I entered a translator’s world, I realized that there was a world of difference!
We work with doctors, and firefighters too
Every project and every file comes with a challenge. Since the original text can be from any part of the world, there are challenges arising from that. The language is culturally influenced, which can be very much different from my culture, and there may be phrases that would make me do a lot of research. It can be too technical, and then I need to call someone from that field. I remember calling a doctor last week to understand something from just a 200-word long text. I called a fire officer last year when I was translating a manual. Sometimes, I look up pictures on the internet to understand the meaning, especially when it is related to tools and procedures. I watch YouTube videos to understand a process, which then helps me figure out the real meaning of the text.
Choosing the right language is too complicated
One can be a translator, a good one. But when it comes to communicating something, along with translation skills, the sense of what kind of language to use also matters. This means, again, that I need to take advice from some specialist in a particular field about what is commonly used in their industry. In the end, we are writing for their understanding and not teaching the language.
It’s not just about the language
After stepping into the world of a translator, I have realised that it’s not just about the language. It’s about cultures, religions, philosophy, psychology, and so much more. Somewhere in the world, the sunshine can be beautiful and soothing, but in some other part, it may cause a headache. While doing a translation, I have to connect myself to the writer and start feeling good about the smell of coffee, even if I hate that smell.
Dictionaries do not help sometimes
When I worked in informal language, I realised that not every word we use is found in the dictionaries. Sometimes a combination of words emerges as a new word. One has to dive deep and see how the word is formed to understand it. People create new words, even by adding two words from two different languages.
I walk in the dark and find the light
You cannot predict what it’s going to be. Once you have a text in hand, you never know how much time it may take and how much research will be required. You can just get an idea, but when you actually work on it, new problems arise, and you have to find their solutions in your own way. There is no roadmap for every challenge. I make so many decisions, do this or that, and somehow just reach the destination—which is a translation with a similar meaning.
There is a performance appraisal every day
Every project, every single file, is reviewed, and whether you will receive the next project or not will depend upon your performance on this project. One has to be very careful about everything that is delivered—every day—or it may become the reason for losing a hardly-earned client.
Now, let’s see what the surprises are when you choose translation as your career:
Recognition and satisfaction
It’s overwhelming to listen to a book summary, on a book summary app, which is written by me. I feel immense pride in seeing people taking online courses that have been translated by me. I get surprised to see a website content translated by me.
It has different colours
One has different things to do every day: translation, localization, transcreation, writing, review, etc. One day you write about weight loss, and the next day you feel like the leanest body trying hard to gain weight.
It gives you intellectual friends
People related to language and literature are intellectual beings. They have their own opinions and excellent language skills to express those opinions. It’s wonderful when your profession lets you get in touch with such individuals. I am so fond of and also proud of the fact that I am in contact with such individuals.
No limit to expansion
You can learn new things every day and keep expanding the area of your work. Today you may do only legal translations, but tomorrow you can prepare yourself for general-investment-related texts by studying their basics—if you are interested. This is how you can keep expanding your area of knowledge and translation. Your earning capacity increases as you expand your knowledge or become an expert in a particular field.
By Vinita Sharma Dubey

Vinita Sharma Dubey has been in the translation industry for the last five years. Her childhood dream of working at a radio station came true when she was selected as an announcer. In addition to writing many radio scripts, she had the chance to learn the correct language. She developed the habit of writing and speaking perfect Hindi while working at a Hindi radio station. A multifaceted professional with expertise in marketing, business, gaming, technology, marketing, agriculture, she has worked for many agencies, direct clients, and NGOs. She enjoys what she does and believes in striving hard to deliver a perfect translation, and likes to guide the newcomers who approach her for the same. One can reach her via email at vinita2508@yahoo.com.
The post A Translator’s World: Challenges and Surprises appeared first on Translators of India.
]]>The post गुणवत्ता के नाम पर होने वाले शोषण से बचें appeared first on Translators of India.
]]>
आजकल अनुवाद कंपनियों द्वारा अनुवाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भाषिक गुणवत्ता आश्वासन (Linguistic Quality Assurance) नाम की यांत्रिक प्रक्रिया का बहुत प्रयोग किया जा रहा है, जिसे संक्षेप में एलक्यूए भी कहते हैं। आप किसी गणितीय गणना की यंत्र द्वारा जांच कर सकते हैं। विज्ञान के अनेक विषयों में सूत्रों की सटीकता की जांच भी यंत्रों द्वारा संभव है। लेकिन कुछ निश्चित एल्गोरिदम फ़ीड करके किसी कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा अनुवाद की गुणवत्ता की जांच सैद्धांतिक रूप से ही गलत है। विशेष रूप से हिंदी भाषा के लिए तो इनका कोई सार्थक उपयोग नहीं है।
एलक्यूए के लिए जिस टूल का उपयोग किया जाता है उसमें गुणवत्ता के ऐसे-ऐसे मानदंडों का समावेश किया जाता है कि किसी भी अनुवाद के उपरांत क्यूए रन करने पर आपको 500-600 क्यूए चेतावनियां मिलना आम बात है। इनमें 70-80 प्रतिशत चेतावनियां वर्तनी को लेकर होती हैं। कारण सीधा सा है, किसी भी टूल में सही वर्तनी वाले हिंदी शब्दों का कोई कोश नहीं भरा होता है। इसलिए हिंदी के हर शब्द की वर्तनी गलत ही बताई जाती है। इसी प्रकार यदि लिंग-भेद के कारण किसी अंग्रेजी वाक्य के हिंदी अनुवाद में एक बार पुल्लिंग क्रिया और दूसरी बार स्त्रीलिंग क्रिया का प्रयोग होता है तो क्यूए टूल द्वारा उसे असंगत अनुवाद करार दे दिया जाता है।
ये कुछ उदाहरण तो इस प्रक्रिया और प्रयुक्त टूल की निरर्थकता के संबंध में दिए गए हैं। लेकिन हम अनुवादकों के लिए कहीं बड़ा विषय है इस एलक्यूए प्रक्रिया द्वारा अनुवादकों का शोषण! जैसा कि सभी जानते हैं, अनुवाद की पारंपरिक प्रक्रिया में अनुवाद के बाद प्रूफरीडिंग का चरण आता है। प्रायः प्रूफरीडिंग की दर अनुवाद दर की आधी होती है। जैसे, यदि अनुवाद दर 2 रुपये प्रति शब्द है तो प्रूफरीडिंग की दर 1 रुपया प्रति शब्द होगी।
लेकिन अनुवाद कंपनियों ने इस एलक्यूए की प्रक्रिया को लाकर प्रूफरीडिंग चरण को समाप्त कर दिया है। जहां प्रूफरीडिंग में प्रति घंटा 500-600 शब्दों की प्रूफरीडिंग अपेक्षित हुआ करती थी, अब एलक्यूए में 1000 से लेकर 6000 शब्द प्रति घंटा का मानदंड अलग-अलग कंपनियों द्वारा तय किया गया है। औसतन 3000 शब्द प्रति घंटा भी मानें और अनुवादक की प्रति घंटा दर 500 रुपये है, तो उसे एलक्यूए के लिए प्रति शब्द 17 पैसे की दर से भुगतान किया जाएगा। इस आलेख के माध्यम से मेरा यही कहना है कि अनुवाद कंपनियों की घातक चालों में न फंसें। एक तो किसी भी भाषिक गुणवत्ता या संपादन या समीक्षा के लिए प्रति घंटा दर 1000 रुपये से कम न रखें दूसरे प्रति घंटा शब्द सीमा किसी भी स्थिति में 1000 शब्द प्रति घंटा से अधिक स्वीकार न करें।
लेखक : विनोद शर्मा

बीएसएनएल में सेवारत रहते हुए 1991 में अंग्रेजी में एमए किया, लगातार 1993 में हिंदी में एमए किया फिर 1995 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से अनुवाद में पीजी डिप्लोमा किया। 1995 से 1997 तक शौकिया अनुवाद कार्य किया। जुलाई 1997 से विधिवत पेशेवर अनुवादक के रूप में कार्य शुरू किया, लेकिन विकीपीडिया, रोजेटा फाउंडेशन, ट्रांलेटर्स विदाउट बॉर्डर्स आदि के लिए स्वैच्छिक अनुवाद भी चलता रहा। 2005 से कैट टूल्स से परिचय हुआ। सबसे पहले एसडीएलएक्स, फिर वर्डफास्ट पर काम करना शुरू किया। उसके बाद तो अनुवाद यात्रा चलती रही। नए-नए टूल्स शामिल होते रहे, नए-नए विषयों और क्षेत्रों में, नए-नए फाइल प्रकारों से होते हुए ये सफर जो चला तो चलता ही रहा। 2010 से 2020 तक दबिगवर्ड कंपनी के लिए गूगल रिव्यूअर के रूप में नियमित कार्य किया।
An Engineer with a passion for languages went on to complete Masters both in English and Hindi in 1991 and 1993 respectively. He did not stop here, completed a PG Diploma in Translation from IGNOU in 1995. Started with amateur translation for Wikipedia, Rosseta Foundation and Translators without Borders. Turned professional in 1997 and never stopped. Started using CAT tools in 2005 with SDLX, Wordfast, Idiom and since then no looking back. Worked as Google Reviewer through thebigword from 2010 to 2020. Specialization in Medical, Legal and Technical fields. Working mostly with foreign companies only.
The post गुणवत्ता के नाम पर होने वाले शोषण से बचें appeared first on Translators of India.
]]>