The post अनुवाद की चुनौतियां appeared first on Translators of India.
]]>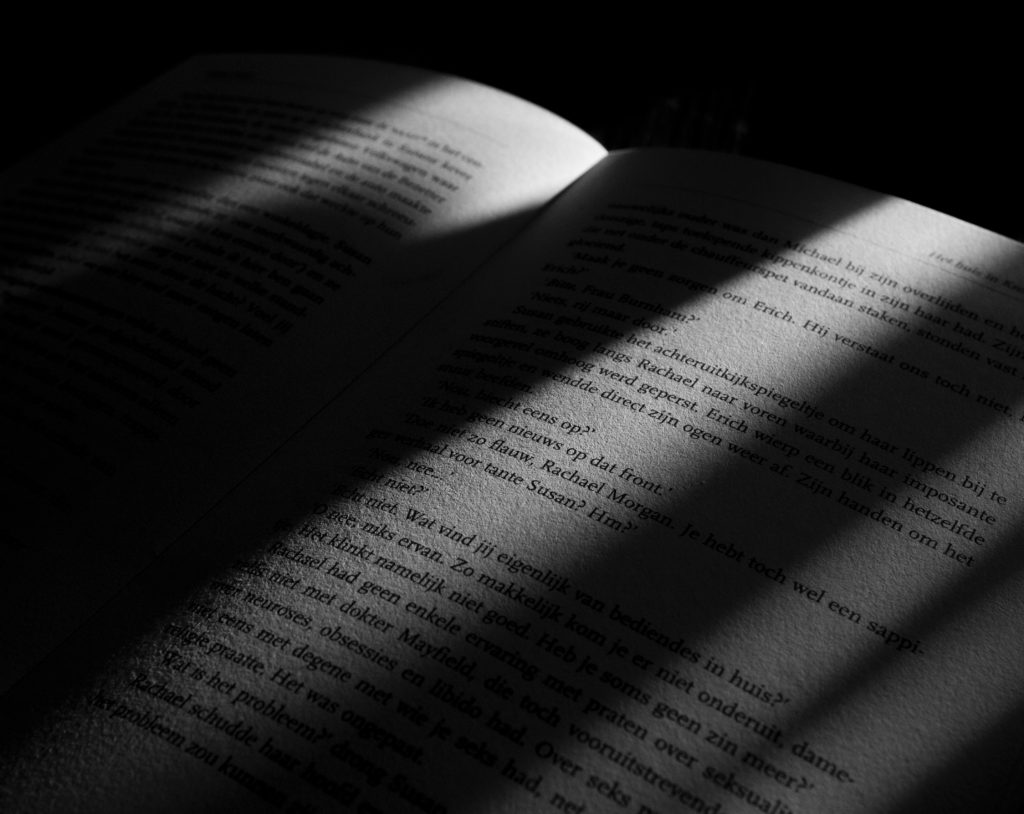
स्टोरीवीवर की कहानियों का अनुवाद हमेशा चुनौती साथ लाता है : हमें ठीक-ठीक मालूम नहीं होता कि कहानी का पाठक दुनिया के किस हिस्से में है, उसकी आयु या शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है, वह प्रस्तुत पाठ को किस उद्देश्य से पढ़ रहा है… अनेक प्रश्न बार-बार कलम रोकते हैं। क्या हमारे शब्द उसके लिए भी वही अर्थ रखते हैं, क्या हमारा किया अर्थान्वय उसके लिए भी कारगर रहेगा? और फिर लेखक के मूल कथ्य और मंतव्य को पकड़ने की चुनौती तो हमेशा ही अनुवादकों के सामने रहती है – अरे मन सम्हल-सम्हल पग धरिये!
एक मोटा-मोटा सूत्र राह दिखाता है : अनूदित सामग्री पढ़ने वाले पाठक के लिए वही मूल रचना है।
लेकिन नामों और रिश्तों का जटिल संसार कभी-कभी बहुत कड़ी परीक्षा लेता है। एक कहानी में दक्षिण भारतीय मुख्य चरित्र, जो एक लड़का था, का नाम सत्या था। हिंदी मे यह लड़कियों का नाम होता है; तो नामों के मूल रूप बनाए रखने की ताकीद के बावजूद मैंने उसका नाम सत्य कर दिया क्योंकि मुझे हिंदी के पाठकों को भ्रम में न डालना ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा। हाल ही में गोआनी मूल के ईसाई लेखक की लिखी सुंदर और बहुत रोचक कविता-कहानी में शवयात्रा के समय बजने वाले बैंड (भारत में कम ही जगह इस तरह का चलन है) का उल्लेख आया। इसे हिंदी के बाल-पाठक को समझाने के लिए हमें लंबी-चौड़ी टिप्पणी देनी पड़ती जो पढ़ने का मज़ा ही किरकिरा कर देती। तो हल निकाला शवयात्रा का उल्लेख गोल करके; पाठ की रोचकता बरकरार रही, उसकी गुणवत्ता हल्की नहीं हुई।
लेकिन कई बार तकनीकी शब्दावली की यांत्रिकता आड़े आती है : प्रचलित शब्द गोल/गोला से पता नहीं चलता कि वह किसी पिंड का संकेत दे रहा है या द्विआयामी आकृति का : गेंद भी गोल है, और नंगी आंख से धरती से दिखता चांद भी! अब अगर हम सायकिल के पिंडाकार पहियों की बात कहना चाहें तो कैसे कहेंगे? एक और बड़ी समस्या पशु-पक्षियों-कीट-पतंगों-वनस्पतियों के नाम हिंदी में बताते हुए आती है। इस संदर्भ में ‘ताल का जादू’ के हिंदी अनुवाद की याद आती है। इसमें उल्लिखित कई पक्षियों और कीटों के नाम मुझे नहीं पता थे। हमारी प्रचलित शब्दावली में, कई कारणों से इनमें से बहुत के नाम उपलब्ध नहीं हैं; किसी वैज्ञानिक शब्दावली में मिल भी जाएं तो शेर-बाघ-तेंदुए के बीच अंतर न जानने वाले हमारे पाठकों के लिए वे इतने अपरिचित होते हैं कि अंग्रेज़ी नाम देना भी ठीक ही लगता है – जैगुआर कहने पर यह संभावना बनी रहेगी कि कोई जानकार उसे इसका अर्थ समझा सकता है (वैसे जैगुआर अमेरिका में पाए जाने वाले तेंदुए हैं)। बेसिल का अर्थ आमतौर पर तुलसी लगाया जाता है लेकिन तुलसियां भी कम से कम छह तरह की होती हैं। बेसिल में यह तथ्य निहित है, तुलसी में नहीं।
हर नया पाठ अनुवादक के लिए नई चुनौती लाता है। हर नया अनुवाद भाषा के क्षितिज को कुछ आगे सरकाता है।
स्टोरीवीवर से साभार

मधु बी. जोशी कई दशकों से अनुवादक, कवयित्री, कहानीकार और स्तंभकार के रूप में अंग्रेज़ी और हिंदी के साहित्यिक जगत को समृद्ध करती आई हैं। वे तकनीकी अनुवाद को अपनी आय और साहित्यिक अनुवाद को रचनात्मक संतुष्टि का ज़रिया मानती हैं। उनके द्वारा अनूदित कृतियों में ‘बधिया स्त्री’ और ‘यह जीवन खेल में’ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आप उनसे madhubalajoshi@yahoo.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।
Over the last several decades, Madhu B. Joshi has enriched the Hindi and English literary worlds through her contributions as a translator, poet, story writer, and columnist. She views technical translation as a source of income that allows her to do literary translations of her choice. “Badhiya Stree” and “Yeh Jeevan Khel Mein” are among her most notable translations. She can be reached at madhubalajoshi@yahoo.co.in.
The post अनुवाद की चुनौतियां appeared first on Translators of India.
]]>The post अनुवाद की कुछ व्यावहारिक समस्याएं appeared first on Translators of India.
]]>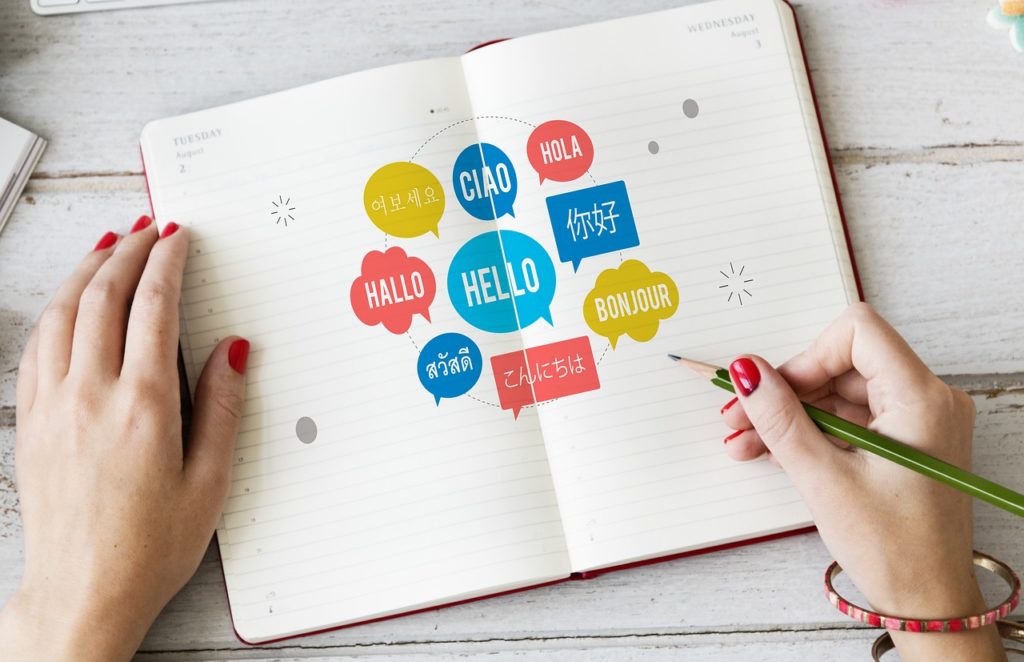
आम तौर पर माना जाता है कि एक भाषा की रचना को उसके मूल भाव और पाठ से विचलित हुए बिना, दूसरी भाषा के पाठकों के लिए सुगम, सरल भाषा में प्रस्तुत करना ही अनुवाद है। लेकिन अनुवाद क्या सचमुच ही इतनी सरल प्रक्रिया है? अनुवाद को सरल क्रिया मानना ही शायद उसके दोयम दर्जे की गतिविधि माने जाने का आधार है और शायद इसीलिए अक्सर अनुवादकों को उनके काम का श्रेय (और कभी-कभी उचित मज़दूरी भी) नहीं मिल पाता। हम जानते हैं कि ईसा से ढाई हज़ार बरस पहले मिस्र में प्रमुख अनुवादक का पद हुआ करता था, शासक की एक पदवी ‘अनुवादकों का मार्गदर्शक’ थी और अनुवादक एक सम्मानित व्यावसायिक वर्ग माने जाते थे, लेकिन इतना ही सच यह भी है कि हमें उन अनुवादकों के नाम नहीं मालूम जिन्होंने साम्राज्य भर में राजादेशों को समान रूप से समझा जाना संभव बनाने के लिए अनुवाद किए। असल में उनके नाम दर्ज ही नहीं किए गए। ओल्ड टेस्टामेंट के हिब्रू से ग्रीक में अनुवाद करने वाले लोगों के बारे में हम बस यह जानते हैं कि वे यहूदियों के बारह कबीलों के प्रतिनिधि थे, हर कबीले के 6 प्रतिनिधि यानी कुल 72 लोग, लेकिन उनके नामों के विवरण उपलब्ध नहीं हैं। बहरहाल, हम पक्के ढंग से जानते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट का हिब्रू से ग्रीक में अनुवाद करवाने वाला मिस्र का यूनानी शासक टॉलेमी द्वितीय था।
एक दार्शनिक कह चुके हैं कि दो व्यक्ति एक ही किताब को अलग-अलग ढंग से पढ़ते हैं। अक्सर ही अनुवाद के बारे में (और प्रकारांतर से अनुवादक के बारे में) शिकायत रहती है कि उसने मूल रचना के साथ पूरा न्याय नहीं किया। दूसरी ओर, विश्व साहित्य से हमारा परिचय अनुवाद के कारण ही संभव हो पाया है। अनुवाद ने संस्कृतियों और समाजों के बीच संवाद के पुल बनाए हैं। बहुत बार एक संस्कृति के कठिन तत्वों को उनसे बिलकुल अपरिचित संस्कृति से आए पाठकों के लिए बोधगम्य बनाने के लिए अनुवादक, जो दोनों संस्कृतियों/भाषाओं के बीच के उस संधिस्थल के नागरिक होते हैं जिसे ‘नो मैन्स लैंड’ कहा जाता है, निकटतम साम्य रचने वाले तत्वों का उपयोग कर लेते हैं जो पूरी तरह वही नहीं हो सकते जो मूल रचना में थे। इसे मूल पाठ से विचलन, और इस तरह अनुवाद कर्म में दोष माना जाता है। लेकिन साहित्य और साहित्यिक पुरस्कारों की दुनिया बहुत हद तक अनुवाद पर टिकी है। क्या आयरिश कवि डब्ल्यू. बी. येट्स के अनुवाद (रोचक है कि इस समर्थ कवि को टैगोर के 10 बरस बाद नोबेल पुरस्कार मिला) के बिना टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिलने की कल्पना भी की जा सकती थी? रसिकों और अनुवादकों के बीच आज भी येट्स के अनुवाद पर बहस जारी है।
क्या अनुवादक पूरी तरह अकिंचन हो सकता है?
अनुवादक से अपेक्षा रहती है कि अनूदित पाठ में उसकी सत्ता की झलक तक न रहे। यह अपने आप में एक असंभव किस्म की मांग है जो चाहती है कि कोख किराये पर देने वाली स्त्री की तरह अनुवादक भी अपने श्रम के उत्पाद पर अपने अस्तित्व के चिह्न न छोड़े। आदर्श रूप से अनुवादक अपनी मानसिक बुनावट के अनुसार किसी पाठ का अर्थान्वय अपने लिए करने के बाद उसे एक ऐसे अमूर्त, आदर्श और कल्पित पाठक के लिए व्यक्त करते हैं जिसका अस्तित्व असल में है ही नहीं, जिसे अनुवादक ने अपनी सुविधा के लिए गणित के ‘एक्स’ की तरह सिरजा है और प्रमेय/समस्या के हल हो जाने पर जो पूरी तरह त्याज्य होता है। लेकिन इसी अमूर्त पाठक (जो अनूदित पाठ के सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध होने पर अनेक ठोस, वास्तविक, सापेक्ष लोगों में बदल जाता है) की ग्रहणशीलता तय करती है कि अनूदित पाठ को कैसे आंका जाएगा। एक बहुत सरल, स्थूल उदाहरण की सहायता से बताएं तो अनुवाद का कर्म मेंहदी लगाने जैसा है (यहां मूल पाठ को अपनी भाषा की माटी में खड़े पौधे पर लगी मेंहदी की पत्तियां माना गया है जिनके गुणधर्म को दूसरी भाषा/संस्कृति में स्थानांतरित करने का काम अनुवादक का है)। मेंहदी पहले पीसी जाती है जिससे उसका भौतिक गुण बदलता है, फिर उस हथेली को साफ़ किया जाता है जिस पर मेंहदी लगनी है, फिर उस पर मेंहदी लगा दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में मेंहदी तोड़ने, पीसने और लगाने वाले व्यक्ति ने खुद का विलोपन करने का पूरा प्रयास किया होता है लेकिन क्या यह विलोपन मेंहदी लगवाने वाले के लिए भी काम करता है? मानवीय अनुभव की सीमाओं के बीच अनुवादक के व्यक्तित्व का विलोपन क्या सचमुच संभव है?
क्या अनुवादक को संपादक की भूमिका में आना चाहिए?
कुछ स्थितियों में मूल पाठ में विचारों और अवधारणाओं को राजनीतिक-सामाजिक कारणों से व्यापक प्रसार के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। ऐसे में अनुवादक, जो एक ओर मूल लेखक का प्रतिनिधि है और दूसरी ओर अनूदित पाठ की ग्राह्यता सुनिश्चित करने को संकल्पबद्ध है, क्या करे इस प्रश्न का पूरा विस्तार समझने के लिए उस दुभाषिये की कल्पना करें जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प और उत्तर कोरियाई तानाशाह किम इल जोंग के बीच बैठा है। अगर वह कुछ त्वरित संपादन न करे तो हमारे संसार को इतिहास बनते देर न लगे। लेकिन तब वह अनुवाद कर्म की संहिता का उल्लंघन कर रहा होगा। प्राचीन और सांस्कृतिक स्तर पर जटिल पाठों (जैसे पंचतंत्र और एलिस इन वंडरलैंड) को बच्चों के लिए अनूदित करते हुए अनुवादकों के सामने अक्सर ही ऐसे निर्णय लेने की स्थिति आती है।
अनुवादक किसका पक्षधर रहे, अपनी आचारसंहिता का या मूल पाठ का या सत्ता का?
आज की राजनीतिक-सामाजिक स्थितियों में अनुवादकर्म बहुत ही जटिल, कठिन हो चुका है। मूल पाठ और अपनी आचारसंहिता के प्रति निष्ठावान बने रहते हुए क्या आतंकवादी घटना के विदेशी आरोपी के दुभाषिये देश-विदेश में मौजूद उसके अज्ञात साथियों का साथ दे रहे होंगे, क्या वे आम जनता के बीच अलगाववादी विचारधारा के प्रसार में सहायक सिद्ध होंगे? अब इसी स्थिति को दूसरे कोण से देखें : मूल पाठ और अपनी आचारसंहिता के प्रति निष्ठावान बने रहते हुए क्या अंतरराष्ट्रीय/विदेशी परिवीक्षकों के लिए देश के असंतुष्ट वर्गों के दुभाषिये देश के हितों (ये हमेशा ही सत्ता द्वारा परिभाषित किए जाते हैं) के विरुद्ध काम कर रहे होंगे? इसी के साथ एक और भी प्रश्न उठता है- क्या अनुवादक/दुभाषिया गोपनीयता को हर स्थिति में बनाए रखे?
कुछ ऐसी ही स्थिति में ओल्ड टेस्टामेंट का ग्रीक में अनुवाद करने वाले यहूदी अनुवादकों ने एक अनूठा उपाय निकाला था : उन्होंने ग्रीक में अनूदित पाठों की ही एक-दूसरे से तुलना करने पर ज़ोर दिया (क्योंकि अनूदित पाठ की हिब्रू मूल पाठ से तुलना वही कर सकते थे) और घोषित किया कि दैवी प्रेरणा के फलस्वरूप अनुवाद एकदम सही हुए हैं।
अनुवादक भाव को प्राथमिकता दे या शैली को?
भावपूर्ण, गीतात्मक पाठों के अनुवादक के सामने अक्सर ही यह दुविधा आती है। हम जानते हैं कि सांस्कृतिक संदर्भों में समानार्थकता प्राप्त कर पाना कभी-कभी असंभव होता है। इसका एक उदाहरण लोकगीतों और लोकगाथाओं का अनुवाद है : भाव पर पकड़ बनती है तो शैली छूट जाती है और शैली पकड़ में आती है तो भाव की सघनता हल्की होती दिखती है।
ये अनुवादकों के सामने खड़े होने वाले कुछ मोटे-मोटे सामान्य प्रश्न हैं, वैसे तो हर पाठ अपनी ही खास चुनौतियां लिए होता है जिनके लिए नई रणनीतियां बनानी होती हैं।

मधु बी. जोशी कई दशकों से अनुवादक, कवयित्री, कहानीकार और स्तंभकार के रूप में अंग्रेज़ी और हिंदी के साहित्यिक जगत को समृद्ध करती आई हैं। वे तकनीकी अनुवाद को अपनी आय और साहित्यिक अनुवाद को रचनात्मक संतुष्टि का ज़रिया मानती हैं। उनके द्वारा अनूदित कृतियों में ‘बधिया स्त्री’ और ‘यह जीवन खेल में’ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आप उनसे madhubalajoshi@yahoo.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।
Over the last several decades, Madhu B. Joshi has enriched the Hindi and English literary worlds through her contributions as a translator, poet, story writer, and columnist. She views technical translation as a source of income that allows her to do literary translations of her choice. “Badhiya Stree” and “Yeh Jeevan Khel Mein” are among her most notable translations. She can be reached at madhubalajoshi@yahoo.co.in.
The post अनुवाद की कुछ व्यावहारिक समस्याएं appeared first on Translators of India.
]]>The post Gendered Languages in Game Localization appeared first on Translators of India.
]]>
What makes gendered languages hard to handle in game localization?
1. Lack of context
If you’re translating games, you already know that the lack of context is very common and can cause many problems. One of these problems is a lack of knowledge about the gender of things mentioned, like when a character says “look at that!” Translating may appear easy in such situations. However, the word ‘that’ could have diverse meanings, depending on the gender it represents. In Arabic, for example, there are at least 3 options to convey the word “that”, depending on what it refers to and its grammatical number.
2. Space
When your target language has more than one pronoun to refer to the addressee depending on their gender, it could be a nightmare because some games address all genders, and if you’re translating from English, “you” is just a three-character word that applies to all genders of all numbers. This could result in exceeding the character limit.
3. Placeholders
It’s very common to deal with placeholders in game localization. They could cause a problem when your target language requires adding prefixes depending on the gender of the word replaced by the placeholder. So, you need to know that placeholder and its number if it’s needed to convey an accurate meaning of the sentence.
4. Multiple characters in the game
Problems arise when there is a game that has many characters and there is no specific script for which characters will be in a particular situation. Sometimes you can start a mission in the game and some characters die during the mission. The text should be neutral to suit whatever happens in the mission because you will never know which characters survive or their gender and number.
How can such a problem be handled carefully?
The only possible solution is to use a gender-neutral style as much as you can. If your target language depends on using direct speeches and pronouns, try to tweak the sentence to convey the meaning. For some languages, resorting to nouns instead of adjectives is a good option.
By Eman Abdo

Eman Abdo is an English to Arabic translator specializing in localization and transcreation, mainly in marketing and game localization. She is also the author of Egypt Localization Guide and the force behind the localization of so many apps and games in Arabic and a gamer at core aspiring to change the way Arabic is represented globally. You can reach her at emanabdo.eman12@gmail.com.
The post Gendered Languages in Game Localization appeared first on Translators of India.
]]>The post अनुवाद के अनुभव appeared first on Translators of India.
]]>
अपने प्रारंभिक अनुवाद मैंने राज्य संदर्भ केंद्र, जयपुर (प्रौढ़ शिक्षा) के लिए किए थे, केंद्र से छपने वाली पत्रिका ‘अनौपचारिका’ के लिए। इसके पहले कुछ अनुवादों से मेरा परिचय एक पाठक के रूप में ही हुआ था। याद आता है कि पहला अनुवाद जो मैंने बचपन में पढ़ा वह फ्रांसीसी लेखक जूल्स वर्न की एक किताब का था। मूल शीर्षक क्या रहा होगा, पता नहीं पर उसके गुजराती में पढ़े अनुवाद का शीर्षक था ‘साहसिकों नी सृष्टि’। वयस्क होने पर तमिल, मलयाली, मराठी, बांग्ला के कुछ लेखकों की रचनाओं के अनुवाद हिंदी और अंग्रेज़ी, दोनों ही भाषाओं में पढ़े। और इस निष्कर्ष पर पहुँची कि भारतीय लेखकों की रचनाएँ अनूदित रूप में पढ़ने की मजबूरी हो, और अगर वे हिंदी में उपलब्ध हों, तो उसी में पढ़ना अधिक सुख देता है।
बचपन में कोलकाता के घर में माँ-पापा और उनके मित्रों से हिंदी, बांग्ला, अंग्रेज़ी और गुजराती सुनी और कुछ-कुछ सीखी होगी। याद है कि पापा से संस्कृत के श्लोक और गीता के सस्वर पाठ सुने थे। बाल शिक्षा मंदिर, मेरा पहला स्कूल, वह मॉन्तेसरी बाल शाला थी, जिसे माँ-पापा ने शायद 1951 में स्थापित किया था। उसमें गाई जाने वाली प्रार्थनाओं में एक सिंधी प्रार्थना ‘जित कित वसे भी तूं, तेरी मकान आला’ की धुन और कुछ पंक्तियाँ आज तक मन में गूँजती हैं। मेरे इस पहले स्कूल की एकाध सहपाठी सखियाँ तमिल और तेलगु भाषी थीं। उनसे कुछ शब्द और दस तक की गिनती सीखने की स्मृति अब भी पूरी तरह क्षीण नहीं हुई है।
मेरा पहला अनुवाद
अपनी आयु के चौथे दशक के मध्य में पहुँचने पर जब अनुवाद करने की पेशकश सामने आई तब शायद यह फिक्र दिमाग के आसपास फटकी तक नहीं कि अनुवाद का कौशल है भी या नहीं। ज़ाहिर है कि ये प्रारंभिक प्रयास अटपटे रहे होंगे और उन्हें संपादकों ने संशोधित कर सँवार दिया होगा। अधिकांश शुरुआती लेख प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित थे। इस कड़ी में पहला लेख संभवत: रॉबी किड का था जो अमरीका के प्रख्यात प्रौढ़ शिक्षाविद थे। रॉबी किड के उस आलेख का एक कथन मन पर कुछ यों खुद गया कि भूले नहीं भूलता। शायद इसलिए क्योंकि उस समय स्वैच्छिक संस्थाएँ स्वैच्छिक ही थीं, उनका गैर-सरकारी संगठनों वाला स्वरूप तब तक पूरी तरह अवतरित नहीं हो पाया था। स्वैच्छिक काम के विषय में किड का कथन था : किसी अच्छे काम की शुरुआत करने की पहली आवश्यकता उसके लिए धन व संसाधन जुटाने की नहीं, वरन दृढ़ संकल्प और स्पष्ट परिकल्पना की होती है। संकल्प नेक हो और और परिकल्पना व्यावहारिक तो धन और संसाधन स्वतः जुटते जाते हैं। उनका यह मंत्र संभवत: स्वप्ररेणा से, कई लोगों को अपनाते और सफलतापूर्वक लागू करते मैंने देखा भी था।
मेरी पहली किताब
इन प्रारंभिक आलेखों के बाद पहली पुस्तक जिसके अनुवाद की ज़िम्मेदारी मुझे अनायास ही सौंपी गई वह थी : ‘तोत्तो चान: अ गर्ल बाय द विंडो’। घटना शायद अस्सी के दशक के मध्य की होगी। हमारे मित्र श्री अरविंद गुप्ता जापान यात्रा पर गए और शिक्षा संबंधी जिस नायाब किताब की चर्चा उन्होंने वहाँ सुनी, वह तोत्तो चान थी। पुस्तक का अंग्रेज़ी अनुवाद तब छप चुका था। उन्होंने उसे खरीदा, पढ़ा और बेहद प्रभावित हुए। भारत लौटने के बाद अपनी जयपुर यात्रा के दौरान उन्होंने पुस्तक का उल्लेख राज्य संदर्भ केंद्र के तत्कालीन निदेशक श्री रमेश थानवी से किया। इस सुझाव के साथ कि उसका अनुवाद हो और ‘अनौपचारिका’ में उसे धारावाहिक रूप में छापा जाए।
जापान की विख्यात टेलिविज़न कलाकार व बाद में यूनिसेफ की सद्भावना दूत, तेत्सुको कुरोयानागी द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जापानी शिक्षाविद सोसाकु कोबायाशी द्वारा 1937 में स्थापित तोमोए गाकुएन स्कूल में अध्ययन करती थीं। युद्ध के दौरान 1945 में तोक्यो में हुई बमबारी में तोमोए जल कर राख हो गया, पर कुरोयानागी के मन पर तोमोए और अपने गुरु कोबायाशी की स्मृतियाँ अमिट रहीं। ‘तोत्तो चान’ पहले एक पत्रिका में धारावाहिक के रूप में 1979 से 1980 के दौरान छपी। 1982 में कुरोयानागी के ये आलेख पुस्तक के रूप में छपे और उसने जापानी प्रकाशन जगत में नया कीर्तिमान स्थापित किया। किसी महिला, वह भी एक टेलिविज़न कलाकार द्वारा लिखी पुस्तक का बेस्टसेलर बन जाना जापान के लिए एक अभूतपूर्व घटना थी।
बहरहाल, थानवी जी ने अनुवाद की ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी, संभवतः इसलिए क्योंकि मेरे पिता उन दिनों अस्वस्थ थे। आंशिक पक्षाघात के कारण वे जीवन में पहली बार पूरी तरह बिस्तर पर थे। आठ साल की बिटिया और लगभग अस्सी बरस के अस्वस्थ पिता की देखरेख का दायित्व मुझ पर देख उन्होंने सुझाया कि मैं घर पर रहते हुए ही सुविधानुसार अनुवाद करूँ। पूरी पुस्तक का अनुवाद पहले किया न था इसलिए यह अनुभव अपने आप में खास था ही, पर साथ ही एक दूसरा मीठा अनुभव भी साथ आ जुड़ा। इन कुछ कठिन दिनों में फुर्सत और तसल्ली से बैठ काम कर पाने की सुविधा निकल ही नहीं पाती थी। दिन के किसी भी वक्त बीस-पच्चीस मिनट भी मिलते तो उनके सदुपयोग की जुगत भिड़ानी पड़ती। अरविंद भाई ने किफायत की मजबूरी में ए-4 साइज़ के हर पृष्ठ पर पुस्तक के चार-चार पन्ने ज़ीरॉक्स करवाए थे। भाग्य से तब चालीसिया चश्मा भी नहीं चढ़ा था, सो आँखों को कुछ थकान के सिवा खास असुविधा भी महसूस नहीं हुई।
जिस मीठे अनुभव का ज़िक्र करना ज़रूरी है वह यह था कि बिटिया और पापा को भी तो ‘तोत्तो चान’ की स्कूली जीवन की कथा में रस आने लगा था। सो हर शाम, रात के खाने से पहले, तीन पीढ़ियों की एक अद्भुत गोष्ठी होती। दिन भर जितना हिस्सा अनूदित हो पाता, वह मैं पढ़ कर सुनाती। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि अनुवाद का दूसरा प्रारूप भी उसी दिन तैयार होता गया। वह यों कि पढ़कर सुनाते वक्त मैं जहाँ भी अटकती, लड़खड़ाती या देखती कि बिटिया या पापा बात समझ नहीं पाए हैं, फौरन भाँप लेती कि वाक्य को सुधारने या नए सिरे से लिखने की ज़रूरत है। ‘तोत्तो चान’ के अनुवाद के दौरान अनूदित अंशों को ज़ोर से पढ़कर किसी को सुनाने और तब संशोधन करने की जो विधि मैंने सीखी उसका उपयोग बाद में कई गंभीर पुस्तकों के अनुवादों के संपादन में अपनी सखी कवयित्री व चित्रकार तेजी ग्रोवर के साथ किया।
‘तोत्तो चान’ का हिंदी अनुवाद पहले ‘अनौपचारिका’ में धारावाहिक व पलाश (मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग की पत्रिका) में विशेषांक के रूप में छपा। इसके बाद जब लोक जुंबिश कार्यक्रम में किताबों की खरीद की जा रही थी तो किसी ने उसकी कुछ हज़ार प्रतियाँ छाप डालीं। अंततः जब नेशनल बुक ट्रस्ट ने 1996 में इसका हिंदी अनुवाद छापा और अधिक लोगों के हाथ वह पहुँचा तो कई लोगों को यह भ्रांति हुई कि मैंने यह अनुवाद कुरोयानागी की मूल जापानी पुस्तक से किया होगा। मौखिक रूप से तो अपने मित्रों और परिचितों को कई बार बता चुकी हूँ कि दुर्भाग्य से मैं जापानी भाषा से पूरी तरह अनभिज्ञ हूँ। मैंने यह अनुवाद डॉरोथी ब्रिटोन के अंग्रेज़ी अनुवाद से ही किया था। कुरोयानागी ने 1984 में अपने संशोधित आमुख में डॉरोथी के अनुवाद का उल्लेख करते हुए लिखा था कि ‘उनका बेहतरीन अनुवाद उसी लय-ताल और भावनाओं को सँजोए हुए है जो मूल कृति में हैं।’ उन्होंने यह भी जोड़ा कि डॉरोथी का अनुवाद जापान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली अंग्रेज़ी पुस्तक सिद्ध हुई। और उसकी चार लाख प्रतियाँ बिकीं। हिंदी अनुवाद के विषय में ऐसा कोई आँकड़ा मेरे पास नहीं है, सिवा इसके कि 2011 में इस संस्करण की आठवीं आवृत्ति छप चुकी थी।
एजुकेशनल क्लासिक्स
‘तोत्तो चान’ के बाद गत दो दशकों में कई पुस्तकों का अनुवाद करने का सौभाग्य मिलता रहा। इनमें अनेक ऐसी पुस्तकें थीं जो शिक्षा के क्षेत्र में ‘वर्ल्ड क्लासिक्स’ में गिनी जाती हैं – सिल्विया एशटन वॉर्नर की ‘टीचर’, जॉर्ज डेनिसन की “लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन’, जॉन होल्ट की ‘हाऊ चिल्ड्रन फेल’, ‘एस्केप फ्रॉम चाइल्डहुड’ औरॉ ‘व्हॉट डू आई डू मनडे’ (अप्रकाशित) तथा ए.एस. नील की ‘समरहिल’। इसके अलावा कुछ ऐसी पुस्तकें भी अनूदित कर सकी जो संभवत: उतनी विख्यात नहीं हैं, पर शिक्षा जगत में उन लेखकों के अद्वितीय प्रयोगों का अद्भुत दस्तावेज़ हैं। इनमें पहली है जुलिया वेबर गॉर्डन की ‘माय विलेज स्कूल डायरी’, दूसरी डेनियल ग्रीनबर्ग की ‘फ्री एट लास्ट: सडबरी वैली स्कूल’। याद आता है कि सिल्विया, डेनिसन तथा होल्ट की एक पुस्तक का अनुवाद मध्य प्रदेश की संस्था किशोर भारती के ‘चिल्ड्रन्स एक्टिविटी प्रोग्राम’ के लिए किया था। उन दिनों तेजी ग्रोवर इस कार्यक्रम को सँभालती थीं और उन्होंने शिक्षा की श्रेष्ठ पुस्तकों को चिह्नित कर उनका तर्जुमा करवाने का बीड़ा उठाया था। अरविंद भाई की प्रेरणा भी इसमें शामिल थी।
किताबें मन के करीब
शिक्षा से जुड़ी दो अन्य पुस्तकों, जिन्होंने अनुवाद करते समय व्यक्तिगत रूप से मन पर छाप छोड़ी और खूब सोचने की सामग्री दी, का उल्लेख करने का लोभ हो रहा है। दोनों ही अब तक प्रकाशित नहीं हो पाई हैं। इनमें पहली रचना पॉरोमेश आचार्य की है। ब्रिटिश राज की स्थापना के समय बंगाल की देशज शिक्षा का जो स्वरूप था, उसका शोध आचार्य जी ने किया और अपने शोध ग्रंथ को बांग्ला में ही लिखा। इस कारण क्योंकि उन्हें लगा कि अंग्रेज़ी में लिखने पर वह बंगाल के एक सीमित वर्ग को ही उपलब्ध हो सकेगी जो उचित न होगा। बांग्ला लिपि वर्षों पहले कोलकाता में अपनी प्राथमिक शिक्षा के दौरान सीखी थी। बांग्ला बोलने के अवसर तो मिलते रहे थे पर उसे पढ़ने के नहीं। अनुवाद अंग्रेज़ी से हिंदी में ही करती रही थी। सो, बांग्ला के दुरूह संयुक्ताक्षरों से खूब जूझना पड़ा। एकलव्य की टुलटुल बिस्वास की मदद न मिली होती तो शायद हताशा में हथियार डाल देती। दूसरी पुस्तक जो मुझे बेहद महत्वपूर्ण भी लगती है, कमला मुकुंदा की है। कमला सेंटर फॉर लर्निंग, बंगलूरू में काम करती हैं। उनकी रचना ‘व्हॉट डिड यू आस्क इन स्कूल टुडे’ बाल मनोविज्ञान पर है। कमला ने जब ‘सेंटर फॉर लर्निंग’ में काम करना शुरू किया तो पाया कि शिक्षक और बच्चों के माता-पिता के मन में तमाम ऐसे सवाल रहते हैं जिन्हें परंपरागत रूप से मनोवैज्ञानिक संबोधित करते रहे हैं, उन पर शोध भी करते रहे हैं। पर वे जिस भाषा में उन सवालों के जवाब देते हैं वह बच्चों के माता-पिता तो क्या प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों तक के पल्ले नहीं पड़ती। सो कमला ने यह बीड़ा उठाया और सरल-सुगम भाषा-शैली में उपरोक्त किताब की रचना की। एकलव्य ने अभी-अभी उसे प्रकाशित किया है।
वैकल्पिक शिक्षा से परिचय
इन शिक्षाविदों के शिक्षा-दर्शन व दृष्टि को हिंदी भाषी पाठकों, खास तौर से स्कूली शिक्षकों, को उपलब्ध करवाने का जो महती प्रयास तमाम लोगों ने किया और आज भी कर रहे हैं, उसमें अंशदान कर पाने का जो संतोष मुझे मिला वह आज भी मेरी सबसे बडी पूँजी है। इन पुस्तकों को दरअसल कितने शिक्षकों/पाठकों ने पढ़ा, उनको इनसे कुछ प्रेरणा मिली या नहीं, अपने शिक्षा कर्म में उन्हें कोई मदद मिली या नहीं, वे कुछ सार्थक तलाश पाए या नहीं यह जान पाने का कोई उपाय मेरे पास नहीं था, न आज है। पर इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि आज शिक्षा के नाम पर जो ‘रटंत विद्या’ और परीक्षा आधारित मूल्यांकन का प्रचलन है, उससे भिन्न, वैकल्पिक पर वास्तविक शिक्षा मुहैया करवाने की चेष्टा करने वाले उपरोक्त ‘गुरुओं’ से मेरा परिचय अनुवाद-कर्म के कारण ही हो सका। अन्यथा स्कूली शिक्षा के विषय में मेरे निजी अज्ञान का क्षेत्र आज और भी बड़ा और भारी होता।
बाल साहित्य
शिक्षा से जुड़ी पुस्तकों के अनुवाद के अलावा बाल साहित्य के अनुवाद का सुखद सौभाग्य भी मिला। इस क्रम में कुछ अंग्रेज़ी और दो बांग्ला रचनाओं को अनूदित करने का मौका मिला। इस प्रकार के अनुवाद का सुख भिन्न ही होता है। इस कड़ी में मेरी चहेती एक पुस्तक थी श्री सुकुमार राय की रचना “हॉजोबॉरोलॉ’। बचपन में जिस लेखक, कवि व चित्रकार की रचनाएँ पढ़-सुन-देख कर हँसी से लोटपोट हुआ करती थी, और तब बड़े होने पर हिंदी में बच्चों के लिए हास्य रचनाओं की कमी पर दुखी, उनकी किताब का अनुवाद अपनी बुज़ुर्ग मित्र मुकुलिका सेन के आग्रह पर किया था। मुकुल दीदी तब आई.ए.एस. पद से सेवा निवृत्त हो चुकी थीं और मेरी ही तरह सुकुमार राय को बेहद पसंद करती थीं। एकलव्य ने सहर्ष ‘हॉजोबॉरोलॉ’ का अनुवाद ‘ऊल-जलूल’ शीर्षक से छापा था। ‘ऊल-जलूल’ को छापते समय एकलव्य ने अनुवाद के अंत में लेखक परिचय भी छापा जो सुकुमार राय के पुत्र सुविख्यात फिल्मकार सत्यजीत राय ने स्वयं लिखा था। क
बाल साहित्य के अनुवादों में ताज़ा अनुवाद नॉर्वीजी बाल साहित्यकार थूरब्योर्न एग्नर की किताब का है। एग्नर की मूल नॉर्वीजी रचना के अंग्रेज़ी अनुवाद का शीर्षक था ‘व्हैन रॉबर्स केम टू कार्डिमम टाउन’। एग्नर की यह रचना नॉर्वे में 1955 में छपी और तब से ही लोकप्रिय रही है। पुस्तक के हिंदी अनुवाद ‘जब लुटेरे इलायचीपुर आए’ के विमोचन के दौरान कुछ ऐसे नॉर्वीजी स्त्री-पुरुषों से मुलाकात हुई जिनकी बचपन में उसे चाव से पढ़ने और उसका रस लेने की स्मृतियाँ आज तक ताज़ा हैं। पुस्तक के रसीले गद्य के अलावा उसके दो अन्य आकर्षण हैं। एक तो एग्नर के अद्भुत चित्र जो बच्चों ही नहीं वयस्कों का भी मन मोहते हैं। दूसरे, उसकी कविताएँ। लगभग सभी प्रमुख पात्रों के गीत हैं जिनकी स्वर-लिपि तक मूल पुस्तक और उसके अंग्रेज़ी अनुवाद में दी गई है। नार्वीजी मित्रों ने बताया कि गर्मियों में कई शहरों में इनकी प्रस्तुतियाँ की जाती हैं। इस अनुवाद में सबसे बड़ी समस्या इन गीत-कविताओं को लेकर ही थी। कविता में मेरी कोई गति नहीं है यह जानती ही थी। ज़ाहिर था कि छंदबद्ध कविताएँ लिखने में दक्ष किसी कवि मित्र का सहारा लिए बिना पुस्तक के साथ न्याय नहीं हो सकता था। विरासत फाउंडेशन के विनोद जोशी ने तब श्री गोपाल प्रसाद मुद्गल का नाम सुझाया। उनके लिखे गीतों ने अनुवाद में प्राण फूँक दिए। यह कहने में संकोच नहीं कि उनके रचे गीत अंग्रेज़ी पाठ पर आधारित होने के बावजूद उनसे बेहतर बन पड़े हैं।
कैसे लेख-अनुवाद हैं बेहतर?
यह प्रश्न कभी-कभार मुझसे भी पूछा गया कि अनुवाद कैसे किया जाता है या ‘अच्छा’ अनुवाद कैसे किया जाता है। मुझे आज तक इन सवालों के सटीक जवाब सूझे नहीं हैं। उत्तरों की तलाश मुझे भी रही है। पर ‘अच्छे’ अनुवाद को लेकर एक निजी मान्यता सामने रखने का कई बार साहस किया है जिसकी अक्सर प्रतिकूल प्रतिक्रिया ही मिली है। वही साहस एक बार फिर से करती हूँ, इस आशा के साथ कि शायद कोई सुधि पाठक मान्यता को खारिज भी करे तो कुछ ऐसे तर्कों के साथ कि हमारी साझी समझ स्पष्ट हो सके। तो निजी मान्यता यह है कि जिस लेख-आलेख, कथा-उपन्यास का अनुवाद किया जा रहा हो वह जितनी सरल-सरस-सुंदर भाषा-शैली में होगा उसका तर्जुमा उतना ही सरल-सरस और सुंदर बन पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, ‘अच्छे’ अनुवाद के श्रेय का अधिकांश भाग मूल लेखक को ही जाना चाहिए।
तो विवाद यहीं शुरू हो जाता है, क्योंकि सामने वाला तब यह कहता है कि “वाह! बड़ी चतुर हैं आप। बड़ी सिफत से कमज़ोर अनुवाद का ठीकरा भी मूल लेखक के मत्थे फोड़ डाला।” पर मैं दरअसल श्रेय साझा करने की ही बात कर रही थी, अपनी भाषागत कमज़ोरियों को कमतर दर्शाने की नहीं। अंग्रेज़ी से अनुवाद करते समय, खासकर जब ‘कॉम्प्लेक्स’ और ‘कम्पाउंड’ वाक्य अनुवादक के सामने हों तो एक भारी द्वंद्व स्वत: उपस्थित हो जाता है। लेखक की भाषा-शैली का सम्मान करते हुए उस वाक्य को अपूर्ण विराम (कोलन जो अंग्रेज़ी में बात के विस्तार से पहले काम में लिया जाता है) तथा अपूर्ण अर्ध विराम (सेमी कोलन जब अंग्रेज़ी में बात को कई टुकड़ों में रखा जाता है) के साथ अनूदित किया जाए, या फिर खड़ी पाई का उपयोग कर उन लंबे व दुरूह वाक्यों को खंडित कर दिया जाए। अनुवादक और संपादक इस बारे में एकमत नहीं हैं। कई संप्रेषणीयता को सर्वोपरि मान मूल लेखक की भाषा-शैली को गौण मानते हैं, तो दूसरे भाषा-शैली का उचित सम्मान करते हुए विचारों को यथासंभव प्रभावी रूप से संप्रेषित करने की सलाह देते हैं, फिर चाहे वाक्य विन्यास को हिंदी के अनुरूप कुछ संशोधित ही क्यों न करना पड़े।
जो समस्या ऐसे में अनुवादक के सामने आती है वह यह है कि मूल लेखक की भाषा-शैली को नज़रअंदाज़ करते ही वह पुस्तक/आलेख न केवल अपना मूल आकर्षण खोने लगता है, बल्कि अपनी ‘मुरकियाँ’ और लयकारी को खो कुछ सपाट-सा बन जाता है। एक अर्थ में वह रचना मूल लेखक की कुछ कम और अनुवादक की कुछ अधिक बनने लगती है। दूसरी ओर विचारों का संप्रेषण ही तो अनुवाद का प्रयोजन है, अगर वह ही न हो सका तो अनुवाद ही निरर्थक हो जाता है। तो अनुवादक के सामने चुनौती यह है कि वह लेखक की भाषा-शैली को साधने की चेष्टा के साथ ही साथ उसके मंतव्य को सटीकता से संप्रेषित करने की चेष्टा करे।
पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा : सुप्रसिद्ध अनुवादक। शिक्षा और बाल साहित्य के क्षेत्र में अनेक पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया है। जयपुर में रहती हैं। यह लेख भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर द्वारा प्रकाशित पत्रिका ‘भाषा परिचय’ के अंक – सितंबर, 2014 से साभार लिया गया है।
The post अनुवाद के अनुभव appeared first on Translators of India.
]]>