The post अनुवादक की बात appeared first on Translators of India.
]]>
तो आख़िरकार गालेआनो की किताब मुखेरेस (Mujeres) का हिंदी अनुवाद आपके सामने है। “आख़िरकार” शब्द यहाँ जोड़ना जरूरी है। ज़रूरी यह बताने के लिए है कि मैंने मूल किताब 2015 में ही स्पेन में रहने के दौरान ख़रीदी थी। उन्हीं दिनों गालेआनो 75 की उम्र में कैंसर से लड़ते हुए इस दुनिया से विदा हुए थे। यह मेरा दुर्भाग्य ही था कि जब मैं फरवरी, 2015 में स्पेन के उत्तर-पश्चिमी शहर सांतियागो दे कोम्पोस्तेला (Santiago de Compostela) पहुँचा था, उससे कुछ ही महीने पहले गालेआनो वहाँ आए थे। वैसे, उनसे उनके लिखे के ज़रिये गहरी पहचान का सिलसिला साल 2010 से ही शुरू हो गया था। मैंने अपना एम. ए. तथा एम. फिल. शोध कार्य उनके अलग-अलग टेक्स्ट्स पर किया था। तब से ऐसा लगता था कि वह मेरे देश, मेरे समाज और ख़ुद मेरे लिए भी लिखते हैं। उनके लेखन का जो हैरत अंगेज़ कर देने वाला दायरा है, वो अगर दुनिया में किसी देश या समाज को अपना लग सकता है, वो हिन्दुस्तान ही हो सकता है। हिंसा और शोषण की जितनी भयावह दास्तानें, बराबरी और बेहतरी की जो ख़्वाहिशें और छटपटाहटें गालेआनो के लिखे से सीधे पढ़ने वाले के बहुत अंदर रूह तक पहुँचती हैं, हमारे अपने समाज से आने वाला कोई भी संवेदनशील इंसान उनसे क़रीबी रिश्ता महसूस करेगा।
2015 के उस दिन से ही, जब गालेआनो की यह ख़ास किताब हाथों में आई, ज़ेहन में यह बात जैसे दर्ज हो गई कि यह किताब भारत के अपने हिंदी-भाषी लोगों में उनकी अपनी ज़बान में पहुँचनी ही चाहिए। किताब के पन्नों को सरसरी तौर पर पढ़ने से ही अंदाज़ा हो गया था कि यह कोई रूमानी ख़याल नहीं, बल्कि जरूरत थी। जिस तरीक़े से गालेआनो इस दुनिया के कितने ही जाने-अनजाने हिस्सों से इतिहास के पन्नों में दर्ज तथा उससे ओझल रह गई औरतों की कहानियाँ सामने लाते हैं, वो हमारे देश-गाँव की अनगिनत नाम-अनाम औरतों की कहानियाँ बन जाती हैं। वही औरतें, जो अपने-अपने मायनों में एक-दूसरे से समय और काल के अलग-अलग छोरों पर रहने के बावजूद कुछ ख़ास मायनों में एक-सी असाधारण हैं। हम इनमें से कइयों को नहीं जानते, क्यूँकि कई तो हमारे इतने आस-पास मौजूद रही हैं, वे साधारण घरों और गलियों की ऐसी औरतें हैं, कि हमने उनका नोटिस ही नहीं लिया है। किसी सरकारी या बौद्धिक इतिहास ने भी उनकी कहानियाँ पूरी बारीकियों में बताने की जरूरत महसूस नहीं की है।
ऐसे में, अर्जेंटीना के एक छोटे से कस्बे की उन औरतों का ज़िक्र कहाँ से आता, जिन्हें समाज रंडियाँ कहता है और जिन्होंने मजदूरों का क़त्लेआम करने वाले फ़ौजियों को अपने कोठे से गरियाते हुए धक्का देकर निकाल दिया था। गालेआनो उन पाँच औरतों का नाम याद रखते और कराते हैं। दूसरी तरफ, इसी देश की सैन्य तानाशाही से उसी के हाथों ग़ायब किये गए अपने बेटे-बेटियों तथा नाती-पोतियों का हिसाब माँगने वाली माँओं तथा दादी-नानियों को भी हमारे सामने ला खड़ा करते हैं। वैसे तो दुनिया इनके बारे में थोड़ा-बहुत जानती है, लेकिन जिस आत्मीयता, नजदीकी और शिद्दत से गालेआनो उनकी टूटन, उनके भीतर के डर और उनके हौसले को अपने शब्दों से महसूसते, छूते और थपकियाँ देते हैं, वह कहीं और मिलना मुश्किल लगता है। गालेआनो के लिखे में वे अनाम, ‘बदनाम’ औरतें तथा वे दादी-नानियाँ सभी अपनी अलग-अलग स्थितियों में एक ही साथ साधारण और असाधारण हैं।
यह तो एक बानगी भर है। किताब के अंदर जाएँ, तो आपको गालेआनो का रचा पूरा का पूरा संसार मिलेगा। यहाँ हज़ारों साल पहले हुई और आज तक हमारी कथाओं, किंवदंतियों, गप्पों और बहसों का हिस्सा रहीं क्लिओपेट्रा, त्लासोल्तेओत्ल, तेओदोरा, हिपातिया तथा दूसरी किरदार आती हैं, तो वहीं पिछली पाँच-छह सदियों की वे औरतें भी जो अपने कहे, लिखे और किए से पूरी दुनिया को उनके लिए, हम सबके लिए बेहतर बनाने के लिए लड़ती रहीं। पूरी ज़िद से, सारे ख़तरे उठाकर, मार दिए जाने तक तथा उसके बाद भी। यहाँ हम दोमितिला से मिलेंगे, जो बोलीबिया के खान मजूरों के इलाके में घूरे पर फ़ेंक दी गई अपनी ज़िंदगी से उठकर उस देश की सैन्य तानाशाही से लोहा ले उसे अपनी दूसरी साथियों के साथ घुटने पर ला देने वाली जुझारू शख़्सियत बन जाती है। हम यहाँ फ्रांसीसी क्रान्ति के बाद स्त्री-अधिकारों की आवाज़ बुलंद करने के ‘जुर्म’ में मौत की सज़ा देने वाली गुलोटीन पर चढ़ा दी गई ओलंपिया द गूजे से रू-ब-रू होते हैं, तो मतदान के अपने अधिकार के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के सुप्रीम कोर्ट तक से भिड़ जाने वाली सुसान एंथनी से भी वाक़िफ़ होते हैं।
गालेआनो उन औरतों की ज़िंदगी और ख़यालातों में भी दाख़िल होने का मौक़ा बनाते हैं, जो कुछ ऐसे जीती, ऐसा करती और कहती हैं, जो हमें इंसानियत तथा सृष्टि की सभी अभिव्यक्तियों के साथ राग-प्रेम के तार जोड़ने की कई मिसालें दे जाता है। यहाँ आप पेरिस शहर की उस माँ से मिलते हैं, जो अपने बेटे की मौत के बाद यह यक़ीन करने लगती है कि वह अब एक कबूतर बन चुका है। इसके बावजूद कहे जाने पर भी वह कबूतरों के झुंड से किसी एक को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती क्यूँकि , बकौल उसके, उसे “क्या हक़ है कि वह अपने बेटे को अपने दोस्तों से जुदा करे”! गालेआनो तो उस बूढ़ी हथिनी की भी बात करते हैं, जो सबसे अक़्लमंद तो है ही, झुंड में सबका ख़याल रखने वाली तथा सबकी स्मृतियाँ संजोने वाली भी है।
यह हमारी त्रासदी है कि हम इन मुख़्तलिफ़ किरदारों को नहीं जानते या जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। इससे इनका महत्व कहीं से भी कम नहीं होता, एक समाज के तौर पर हमारी बदनीयती और हमारा बौनापन ही ज़ाहिर होता है। संकलन में आती दूसरी किरदारों की कहानियाँ बार-बार हमें यही अहसास दिलाती हैं। और इसलिए इन्हें दुनिया की सारी भाषाओं तक पहुँचाया जाना ज़रूरी हो जाता है। और यह हिंदी अनुवाद इसी दिशा में एक छोटी-सी लेकिन संजीदा कोशिश है।
अब कुछ बातें इन कहानियों के हिंदी अनुवाद पर। साल 2011 में मैंने पहली बार गालेआनो का लिखा हिंदी में ढालने की कोशिश की थी। तब यह अहसास हुआ कि गालेआनो जितने तरह के सन्दर्भों को चुटकी में पकड़ लेने वाले अंदाज़ में सामने ला खड़ा कर देते हैं, उसे हिंदी में उसी जीवंतता के साथ लाना बड़ी चुनौती है। तब वो फिर भी बस एक लेख का मामला था जिसका एक ख़ास सरोकार था। इसके बाद जब 2015 में Mujeres (मुखेरेस) हाथों में आई और इसकी कुछ कहानियाँ पढ़ीं, तब यह चुनौती कहीं और ज़्यादा बड़ी और मुश्किल लगी। यहाँ तो लगभग हर कहानी में इतिहास, राजनीति, रोजाना के अहसासात तथा कितने ही और सन्दर्भ एक-दूसरे में गुँथे हुए हैं कि एकबारगी यह सारा कुछ समझ आ जाने वाली हिंदी में रख पाना असंभव ही लगा। अनुवाद करने की ललक सामने खड़ी इस मुश्किल से, हालाँकि, कम नहीं हुई, बल्कि और ज़्यादा तेज़ ही हुई। कहानियों में और ज़्यादा उतरते ही यह भी अहसास हुआ कि इन कहानियों और वहाँ आती औरतों को हमारे हिंदी-भाषी लोगों से मिलाना ही चाहिए।
अनुवाद करते समय लगभग हर कहानी में उस ख़ास किरदार को बनाने वाले इतिहास, आर्थिकी, राजनीति आदि की परतों को स्पेनी से हिंदी में सहज रूप से लाना हमेशा याद रहने वाला अनुभव था। मिसाल के लिए, एक कहानी में लेखक ख़ुद का अनुभव दर्ज करते हुए यह बताते हैं कि कैसे उनके पुराने दिनों का दोस्त लेखकों के पहले से तय मुफ़लिसी वाले भाग्य की मुनादी किया करता था। यहाँ मूल कहानी में hamburguesar यानी हैम्बर्गर या बर्गर खाकर गुज़ारा करने का ज़िक्र आता है। अब हमारे समाज में इस तरह की स्थिति में भी बर्गर खाकर गुज़ारा करने की बात किसी को नहीं सूझ सकती। यह सिर्फ भाषा का नहीं इतिहास और उससे गुँथे और निकलते आर्थिक हालात तथा खान-पान की आदतों को दिखाता है। और ये सारी चीजें भारत में हमारे हिंदी-भाषी समाज में बहुत अलहदा हैं। लेकिन ग़रीबी के हालात में रूखा-सूखा खाकर गुज़ारा करने का अनुभव और वो भी कलाकारों तथा लेखकों के लिए, इस समाज के लिए भी नया नहीं है, भले हम यही बात घास-फूस खाकर ज़िंदा रहने जैसी अभिव्यक्तियों से ज़ाहिर करते हैं। तो इस कहानी का अनुवाद करते समय इस बात को फुटनोट के तौर पर विस्तार से जगह दी गई है। मक़सद यही कि एक आम हिंदी भाषी के लिए यह कहानी उसके अपने आसपास की ऐसी ही कहानियों में एक लगे। गालेआनो भी चाहते कि वो जिस रूहानी भाव से, जिन गहराइयों में उतरकर अपने किरदारों और उनके सन्दर्भों को लाते हैं, दुनिया में कहीं भी कोई उन्हें पढ़े, तो वही भाव महसूसे तथा कुछ पल के लिए ही सही उस कहानी के संसार में शामिल हो तथा बेहतरी की उम्मीदों के साथ वापस आए।
मूल स्पेनी में कई ऐसे मुहावरे भी पेश आए जिन्हें हिंदी में ढालते वक़्त यह बात मालूम हुई कि यहाँ भी हूबहू उन्हीं शब्दों के साथ उन्हीं भावों को लिए हुए मुहावरे मौजूद हैं। मसलन स्पेनी में कहते हैं: estar en el septimo cielo (एस्तार एन एल सेप्तिमो सीएलओ) जिसका शब्दशः अनुवाद “सातवें आसमान पर होना” है, जो हिंदी में भी वैसे ही इस्तेमाल होता है। ऐसा ही एक और मुहावरा है con alma y vida (कोन आल्मा इ बीदा), जिसका शब्दशः मतलब “दिल और जान से है” जिससे भारत में हम एक मुहावरे के तौर पर बख़ूबी परिचित हैं। वहीं दूसरी तरफ़, कुछ कहानियों में रोज़ाना गली-मुहल्लों में खाई जाने वाली ऐसी चीज़ों का जिक्र आया है जिनका अनुवाद समाज, भूगोल, संस्कृति के कई जाने-अनजाने दरवाज़े खोल गया। जैसे कि, एक कहानी ‘वसीयत जिसको कहते हैं’ में स्पेन के हर शहर के हर रेस्त्रां और कैफेटेरिया में मिलने वाले ख़ास मीठे chocolate con churro (चोकोलाते कोन चुर्रो) का ज़िक्र आता है। यह दो अलग-अलग चीज़ों का अद्भुत मेल है, जिसमें एक खाई जाने वाली तो दूसरी पी जाने वाली है। गर्मागर्म चॉकलेट की लपसी और छोटी डंडी की तरह दिखता चुर्रो । चॉकलेट की लपसी तो फिर भी लोग समझ लेंगे, लेकिन चुर्रो को बयान करना दिलचस्प और कठिन दोनों ही था। जो लोग बिहार या उत्तर प्रदेश से होंगे, उन्होंने गाँवों-कस्बों में फोफी नाम की चीज देखी और खाई होगी। अब आप उसी फोफी को नमकीन नहीं मीठा समझिए और उसे खोखला न देखकर अंदर से भरा हुआ, ऊपर से चीनी के छोटे-छोटे टुकड़ों से सजा हुआ, हल्के -गहरे भूरे रंग का देखिए, तब आप चुर्रो को देखने-समझने के काफ़ी क़रीब होंगे। ऐसी सब तफ़सीलें लगभग हर कहानी के फुटनोट में हैं।
इन तफ़सीलों को समझने, इनकी तह में जाने का अनुभव भी काफी दिलचस्प रहा। लगभग हर कहानी में 2-3 तो अक्सर थोड़े लम्बे हो गए फुटनोट्स ही हैं। इनमें हर एक को लिखते समय की गई इतिहास, भूगोल, संस्कृति, खान-पान, रीति-रिवाज़ आदि की लंबी-लंबी विचार यात्राएँ हमेशा ख़ास रहेंगी, उन पर अलग से एक पूरी किताब लिखी जा सकती है!
जिन लोगों ने भी गालेआनो को पढ़ा है, वो बख़ूबी जानते होंगे कि उनके यहाँ छोटे-छोटे वाक्यों, मुहावरों आदि का इस्तेमाल एक अनूठा संसार रचता है। उन्हें पढ़ने वाले इस रचे जा रहे संसार में बेखटके ऐसे दाख़िल होते हैं, जैसे वह गालेआनो के साथ मिलकर यह सब कुछ देख और बयान कर रहे हैं। छू जाने वाली, सहलाने वाली, कभी नींद से झिंझोड़ कर जगाती, कभी प्यारी-सी थपकी देकर अनदेखे संसार में उतारने वाली, कभी पास बैठकर बाँह पकड़कर अन्याय के ख़िलाफ़ खड़ा होने को झकझोरती, गालेआनो की भाषा अपनी अतरंगी कूची से कितने ही रूहानी, सीधा असर करने वाले रंग बिखेरती है। अनुवाद करते समय इन सब अनुभूतियों, रंगों, अहसासों को उसी तरह कम शब्दों तथा छोटे-छोटे वाक्यों में ज़ाहिर करना लगातार एक चुनौती के साथ-साथ दिलचस्प और सिखाने वाला अनुभव रहा। मुझे हमेशा याद रहेगा कि कैसे अक्सर ही किसी कहानी में आए एक ख़ास शब्द को हिंदी में ढालते वक़्त पूरा-पूरा दिन सोचते हुए निकल जाता था।
कई बार तो दो-दो दिन। तब इरादा कभी भी कोई एक शब्द, जो ढीले-ढाले तरीके से भी मुफ़ीद हो, चस्पाँ कर आगे बढ़ जाने का कभी नहीं रहा। और जब वह ख़ास शब्द मिलता, जो अंदर से तस्दीक़ कराता कि हाँ मैं ही वह शब्द हूँ जिसकी तुम ताक में हो, तब उस संतुष्टि और आनंद की तुलना किसी और अनुभूति से नहीं हो सकती। उस ख़ास शब्द तक पहुँचने का सफ़र इस अनुवाद का सबसे अहम और खूबसूरत हिस्सा था। यह सफ़र हर बार भाषा, समाज, संस्कृति, राजनीति, भूगोल और जीवन के तमाम दूसरे ताने-बाने की इतनी गहराइयों में ले जाता था कि यह अहसास अपने-आप हो जाया करता कि मैं जिसे ‘अपनी’ भाषा, ‘अपनी’ संस्कृति कहता रहा हूँ, उसे कितना जानना अभी बाक़ी है। अनुवाद, दरअसल, अगर ‘दूसरी’ से ज़्यादा ख़ुद ‘अपनी’ संस्कृति को जानना नहीं है तो और क्या है? इससे भी आगे बढ़कर यह कहा जाना चाहिए कि यह सिर्फ़ और सिर्फ़ अनुवाद के ज़रिये ही हो सकता है कि हम यह समझें कि वास्तव में सारी संस्कृतियाँ और सारी भाषाएँ एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उनका एक-दूसरे में आना-जाना इस धरती पर इंसानी सफ़र का सबसे बड़ा सच है। फिर हम यह भी देख पाएंगे कि ‘अपनी’ और ‘दूसरी’ या विदेशी (जिसे ‘विरोधी’ या ‘दुश्मन’ बताने में देर नहीं लगती) के तमाम झगड़े कितने अर्थहीन ही नहीं हास्यास्पद भी हैं। गालेआनो अपनी लेखनी और देश-दुनिया में बुलंद की गई अपनी आवाज़ से ताउम्र इस सफ़र को जीते रहे, इसका एक शानदार और रौशन हिस्सा रहे। वह ऐसी दुनिया बनाने के ख़्वाहिश-मंद रहे, जहाँ यह सफ़र लगातार चलता रहे। फिर उनके लिखे का अनुवाद करते समय वही ख़्वाहिश आपके अंदर आकर ले, आपको कुछ करने को कहे तो फिर यह कहा जा सकता है कि गालेआनो के लिखने से शुरू हुई वह कोशिश, वह अभिलाषा एक खूबसूरत मोड़ पर पहुँच रही है। ख़त्म तो ख़ैर वह कभी नहीं होगी।
(यह अनुवादकीय डॉ. पी. कुमार मंगलम द्वारा अनूदित पुस्तक ‘औरतें’ से साभार लिया गया है।)

डॉ. पी. कुमार मंगलम
स्नातक, स्नातकोत्तर (स्पेनी भाषा), एम. फ़िल. एवं पी.एच.डी. (लातिन अमरीकी साहित्य), जे.एन.यू., नई दिल्ली
स्नातकोत्तर कार्यक्रम Crossways in Cultural Narratives (यूरोपीय यूनियन के स्कालरशिप प्रोग्राम के साथ): इंग्लैंड, स्पेन तथा फ्रांस में अध्ययन, 2014-2016
मेक्सिको में पोस्ट-डॉक प्रवास (2019)
जे.एन.यू. तथा दून विश्वविद्यालय में बतौर शोधार्थी एवं अस्थायी शिक्षण
2019 से कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा में स्पेनी भाषा में पूर्णकालिक अध्यापन
‘समयांतर’, ‘बया’, ‘सामयिक वार्ता ‘आदि कई पत्रिकाओं में अनुवाद और लेखों का प्रकाशन। 2015 में किताब की शक़्ल में एदुआर्दो गालेआनो के लेखों का अनुवाद प्रकाशित।
स्पेनी-भाषा समाजों के इतिहास, संस्कृति तथा साहित्य के अध्ययन में गहरी रुचि। स्पेन और लातीनी अमरीका की कुछ बेहद दिलचस्प परिघटनाओं पर भारत के नज़रिए से हिंदी में लेखन की योजना। pkmangalam@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है.
P. Kumar Mangalam is currently serving as Assistant Professor in Spanish at the Central University of Karnataka, Kalaburagi, India. He has obtained his PhD from JNU, New Delhi. He was also awarded a Postdoctoral fellowship of the prestigious Mexican agency GAPA in the year 2019. His paper entitled “Where Defending Mother-Earth and Quests for a Just World are the Same and One: Some Instances from Latin America” has been accepted for the edited volume “Critical Zones: Environmental Humanities in South Asia” to be published by Routledge India.
The post अनुवादक की बात appeared first on Translators of India.
]]>The post विने एवं दार्बेलने की अनुवाद प्रविधियाँ appeared first on Translators of India.
]]>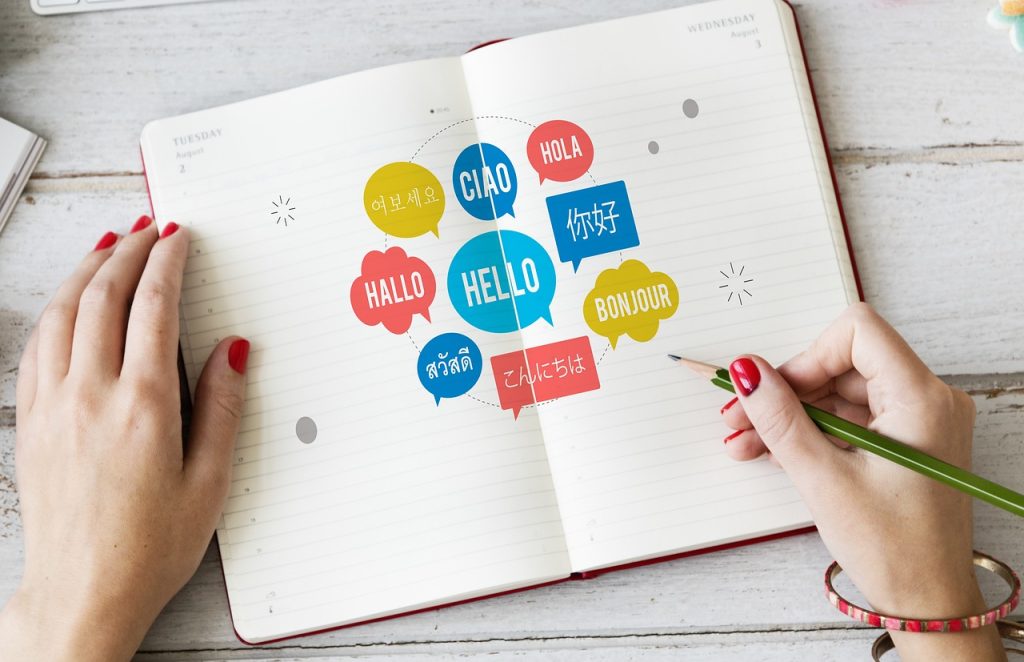
ज़ौं पॉल विने एवं ज़ौं पॉल दार्बेलने ने 1958 में प्रकाशित अपनी फ़्रेंच पुस्तक ‘Stylistique comparée du français et de l’anglais: méthode de traduction’ (स्तिलिस्तिक कौम्पारे द्यु फ़्रांसै ए द लौंग्ले : मेतोद द त्राद्युक्सियों) में अनुवाद प्रविधियों का वर्णन किया है। इस पुस्तक में अनुवाद को केंद्र में रखकर अंग्रेज़ी और फ़्रेंच की भाषिक संरचनाओं की तुलना की गई है। फ़्रांस में इसे तुलनात्मक शैलीविज्ञान की प्रतिनिधि पुस्तकों में से एक माना जाता है। विने एवं दार्बेलने ने इस पुस्तक में अनुवाद की सात प्रविधियों का उल्लेख किया है। यह पुस्तक चार दशक बाद 1995 में अंग्रेज़ी में ‘Comparative Stylistics of French and English : A methodology for translation’ (फ़्रेंच और अंग्रेज़ी का शैलीगत तुलनात्मक अध्ययन : अनुवाद प्रविधि) शीर्षक से अनूदित की गई। इतना समय बीत जाने के बावजूद इस पुस्तक का अंग्रेज़ी में अनूदित किया जाना इसकी प्रासंगिकता का प्रमाण है। अनुवाद प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी इस पुस्तक को उपयोगी माना जाता है।
हर भाषा की अपनी विशिष्ट भाषिक संरचनाएँ होती हैं। इन संरचनाओं की भिन्नता कई बार अनुवाद की चुनौती बनकर सामने आती है। भाषिक संरचनाओं की विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर न केवल भाषिक ग़लतियों से बचा जा सकता है, बल्कि अनुवाद को अधिक सहज और प्रभावी भी बनाया जा सकता है। विने एवं दार्बेलने ने अनुवाद की जिन सात प्रविधियों का उल्लेख किया है, उनका अध्ययन करके अनुवाद प्रशिक्षु अपनी स्रोत और लक्ष्य भाषाओं की भाषिक संरचनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनते हैं। इस सात प्रविधियों में से पहली तीन प्रविधियाँ प्रत्यक्ष अनुवाद से संबंधित हैं और बाकी चार प्रविधियाँ अप्रत्यक्ष अनुवाद से। जो प्रविधियाँ भाषिक संरचनाओं तक सीमित रहती हैं, उन्हें प्रत्यक्ष अनुवाद के अंतर्गत रखा गया है। वहीं, जिन प्रविधियों में भाषिक संरचनाओं से परे जाकर परिवर्तन किए जाते हैं, उन्हें अप्रत्यक्ष अनुवाद में शामिल किया गया है। ये सात प्रविधियाँ सरलता से जटिलता के क्रम में प्रस्तुत की गई। पहली प्रविधि सबसे सरल है और अंतिम सबसे जटिल। इन प्रविधियों का विवरण नीचे प्रस्तुत है :
1. आदान (Borrowing)
लक्ष्य भाषा में उपयुक्त विकल्प मौजूद नहीं होने की स्थिति में स्रोत भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चूँकि ये शब्द बिना किसी परिवर्तन के ग्रहण किए जाते हैं, इन्हें ‘ऋण शब्द’ कहा जाता है। यदि लक्ष्य भाषा की लिपि अलग हो, तो अनुवाद में इन शब्दों के लिप्यंतरित रूपों का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, विज्ञापन आदि क्षेत्रों में ऋण शब्दों का अधिक प्रयोग होता है।
कुछ हिंदी अख़बारों की संपादकीय नीति के कारण कई बार उपयुक्त शब्दों के उपलब्ध होने के बावजूद ऋण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, ‘विज्ञापन’ को ‘एडवर्टाइज़मेंट’ लिखना। जो देश आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, उनकी भाषाओं में विकसित भाषाओं के शब्दों के अनावश्यक प्रयोग की प्रवृत्ति देखी जाती है। यह स्थिति केवल हिंदी, मराठी जैसी भारतीय भाषाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जर्मन और फ़्रेंच में भी अंग्रेज़ी शब्दों की भरमार होने लगी है।
यदि विदेशी भाषा से शब्द ग्रहण करते समय सावधानी नहीं बरती जाए, तो इससे अनुवाद के ग़लत होने की आशंका बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, जब ‘Bodymist’ नाम की डियोडरेंट कंपनी के उत्पाद को जर्मनी के बाज़ार में उपलब्ध कराने के लिए इस नाम का ऋण शब्द के रूप में प्रयोग किया गया, तो ‘mist’ शब्द के कारण समस्या पैदा हो गई। जर्मन में ‘mist’ का अर्थ ‘खाद’ है, इसलिए प्रस्तुत संदर्भ मे जर्मन के बाज़ार में इसका प्रयोग अटपटा साबित हुआ।
2. काल्क (Calque)
विने एवं दार्बेलने ने इस प्रविधि को ‘एक विशिष्ट प्रकार का आदान’ कहा है। ‘काल्क’ (प्रतिलिपि) शब्द की व्युत्पत्ति फ़्रेंच की calquer क्रिया से हुई है, जिसका अर्थ ‘डिज़ाइन, मानचित्र आदि की नकल उतारना’ है। इसमें स्रोत भाषा की अभिव्यक्ति ग्रहण करके उसके घटकों का शाब्दिक अनुवाद किया जाता है। जैसे, अंग्रेज़ी के ‘cold war’ को हिंदी में ‘शीत युद्ध’ लिखा जाता है। यहाँ हिंदी समतुल्य में अंग्रेज़ी के शब्दों को यथावत नहीं लेकर ‘cold’ और ‘war’ के शाब्दिक अनुवादों के माध्यम से ‘शीत युद्ध’ समतुल्य प्रस्तुत किया गया है। काल्क के ज़रिए लक्ष्य भाषा में नई अवधारणाएँ शामिल होती हैं। जैसे, बैंकिंग में ‘चालू खाता’ (current account) और ‘बचत खाता’ (savings account) तथा राजनीति में ‘प्रधानमंत्री’ (prime minister) और ‘मुख्यमंत्री’ (chief minister) जैसे समतुल्य काल्क के उदाहरण हैं। समय के साथ ये समतुल्य इतने प्रचलित हो गए हैं कि इन्हें हिंदी में समतुल्य के बजाय मूल हिंदी शब्द माना जाने लगा है।
3. शब्दानुवाद (Literal Translation)
यह प्रविधि समान भाषिक संरचनाओं या संस्कृतियों वाली भाषाओं में अधिक प्रयुक्त होती है। इसमें बस वही परिवर्तन किए जाते हैं जो लक्ष्य भाषा के व्याकरण के लिए अनिवार्य होते हैं। उदाहरण के लिए, He hit Mohan को हिंदी में “उसने मोहन को मारा” लिखा जाता है। यहाँ हिंदी व्याकरण का पालन करते हुए ‘को’ जोड़ा गया है। ऐसे व्याकरणिक परिवर्तन शाब्दिक अनुवाद के दायरे में शामिल रहते हैं।
4. प्रतिस्थापन (Transposition)
इसमें अर्थ में परिवर्तन किए बिना स्रोत भाषा की व्याकरणिक कोटि को लक्ष्य भाषा की भिन्न व्याकरणिक कोटि से प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसे, “It is raining” को हिंदी में “बारिश हो रही है” लिखा जाता है। यहाँ अंग्रेज़ी की क्रिया (raining) के लिए हिंदी में ‘बारिश’ संज्ञा का प्रयोग किया गया है। “His presence suffices” वाक्य को हिंदी में “उसकी मौजूदगी काफ़ी है” लिखा जा सकता है। इस हिंदी वाक्य में अंग्रेज़ी की ‘suffices’ क्रिया’ को हिंदी में ‘काफ़ी’ विशेषण में परिवर्तित किया गया है।
5. मॉडुलन (Modulation)
जब स्रोत भाषा के कथ्य के रूप में परिवर्तन किया जाता है, उसे मॉडुलन कहते हैं। दूसरे शब्दों मे, इसमें मूल कथ्य को एक नये दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया जाता है। जैसे, “I hurt my toe” का हिंदी अनुवाद “मेरे अँगूठे में चोट लग गई” है। इस वाक्य में कर्तृवाच्य को अकर्मक रूप में बदला गया है। इसी प्रकार, “The meeting was chaired by Manmohan Sharma” को हिंदी में “मनमोहन सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की” लिखकर अंग्रेज़ी के कर्मवाच्य को हिंदी के कर्तृवाच्य में बदला गया है। इस परिवर्तन से लक्ष्य भाषा में संदेश अधिक सहज बनता है।
6. समतुल्यता (Equivalence)
इसमें स्रोत भाषा में वर्णित स्थिति को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने के लिए भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लोकोक्तियों, मुहावरों आदि के अनुवाद में इस प्रविधि का सर्वाधिक प्रयोग होता है। शब्दकोशों में इनके जिन समतुल्यों को शामिल किया जाता है, वे समतुल्यता के उदाहरण होते हैं। जैसे, “rain cats and dogs” को हिंदी में “मूसलाधार बारिश होना” कहते हैं। “Barking dogs seldom bite” के लिए “जो गरजते हैं, वे बरसते नहीं” का प्रयोग भी समतुल्यता का उदाहरण है।
7. अनुकूलन (Adaptation)
अनुवाद की यह प्रविधि तभी अपनाई जाती है जब स्रोत भाषा में वर्णित स्थिति लक्ष्य भाषा की संस्कृति में मौजूद नहीं होती है। विने एवं दार्बेलने इसके लिए अंग्रेज़ी के एक वाक्य का उदाहरण देते हैं : “He kissed his daugther on the mouth.” यदि हम इस उदाहरण को हिंदी के संदर्भ में देखें, तो ‘kissed’ के लिए ‘चूमा’ के बजाय ‘गले लगाया’ का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार, इसका अनुवाद “उसने अपनी बेटी का मुँह चूमा” के बजाय “उसने अपनी बेटी को गले लगाया” होगा। स्रोत भाषा की संस्कृति में पुत्री के मुख पर चुंबन लेने को असहज या अस्वीकार्य नहीं माना जाता है। चूँकि हिंदी में यह स्थिति सहज नहीं मानी जाती है, अनुवादक को एक नई स्थिति का सृजन करना पड़ता है। विने एवं दार्बेलने ने अनुकूलन को ‘एक विशिष्ट प्रकार की समतुल्यता’ कहा है। इस प्रविधि का प्रयोग तभी किया जाता है जब उपर्युक्त सभी प्रविधियों से अर्थ व्यक्त नहीं हो पा रहा हो।
लेखक : सुयश सुप्रभ

नई दिल्ली में रहने वाले सुयश सुप्रभ को मार्केटिंग, बिज़नेस, गेम, टेक्नॉलजी आदि क्षेत्रों में अनुवाद और कॉपी लेखन का 18 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अनुवाद अध्ययन में एमए किया है। वे अनुवाद एजेंसियों और ग़ैर-सरकारी संस्थाओं के लिए अनुवाद करने के साथ तहलका और करियर्स360 जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के लिए काम कर चुके हैं। साथ ही, उन्होंने भाषा और अनुवाद से जुड़े कई लेख लिखे हैं। उनसे suyash.suprabh@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।
Suyash Suprabh is based in New Delhi and has more than 18 years of experience in translation and copywriting in many fields, including marketing, business, games, and technology. He has a postgraduate degree in translation studies. Besides having worked for translation agencies and non-government organizations, he has also worked with renowned Hindi magazines, including Tehelka and Careeres360, and has written many articles on languages and translation. He can be reached at suyash.suprabh@gmail.com.
The post विने एवं दार्बेलने की अनुवाद प्रविधियाँ appeared first on Translators of India.
]]>The post Gendered Languages in Game Localization appeared first on Translators of India.
]]>
What makes gendered languages hard to handle in game localization?
1. Lack of context
If you’re translating games, you already know that the lack of context is very common and can cause many problems. One of these problems is a lack of knowledge about the gender of things mentioned, like when a character says “look at that!” Translating may appear easy in such situations. However, the word ‘that’ could have diverse meanings, depending on the gender it represents. In Arabic, for example, there are at least 3 options to convey the word “that”, depending on what it refers to and its grammatical number.
2. Space
When your target language has more than one pronoun to refer to the addressee depending on their gender, it could be a nightmare because some games address all genders, and if you’re translating from English, “you” is just a three-character word that applies to all genders of all numbers. This could result in exceeding the character limit.
3. Placeholders
It’s very common to deal with placeholders in game localization. They could cause a problem when your target language requires adding prefixes depending on the gender of the word replaced by the placeholder. So, you need to know that placeholder and its number if it’s needed to convey an accurate meaning of the sentence.
4. Multiple characters in the game
Problems arise when there is a game that has many characters and there is no specific script for which characters will be in a particular situation. Sometimes you can start a mission in the game and some characters die during the mission. The text should be neutral to suit whatever happens in the mission because you will never know which characters survive or their gender and number.
How can such a problem be handled carefully?
The only possible solution is to use a gender-neutral style as much as you can. If your target language depends on using direct speeches and pronouns, try to tweak the sentence to convey the meaning. For some languages, resorting to nouns instead of adjectives is a good option.
By Eman Abdo

Eman Abdo is an English to Arabic translator specializing in localization and transcreation, mainly in marketing and game localization. She is also the author of Egypt Localization Guide and the force behind the localization of so many apps and games in Arabic and a gamer at core aspiring to change the way Arabic is represented globally. You can reach her at emanabdo.eman12@gmail.com.
The post Gendered Languages in Game Localization appeared first on Translators of India.
]]>