The post विने एवं दार्बेलने की अनुवाद प्रविधियाँ appeared first on Translators of India.
]]>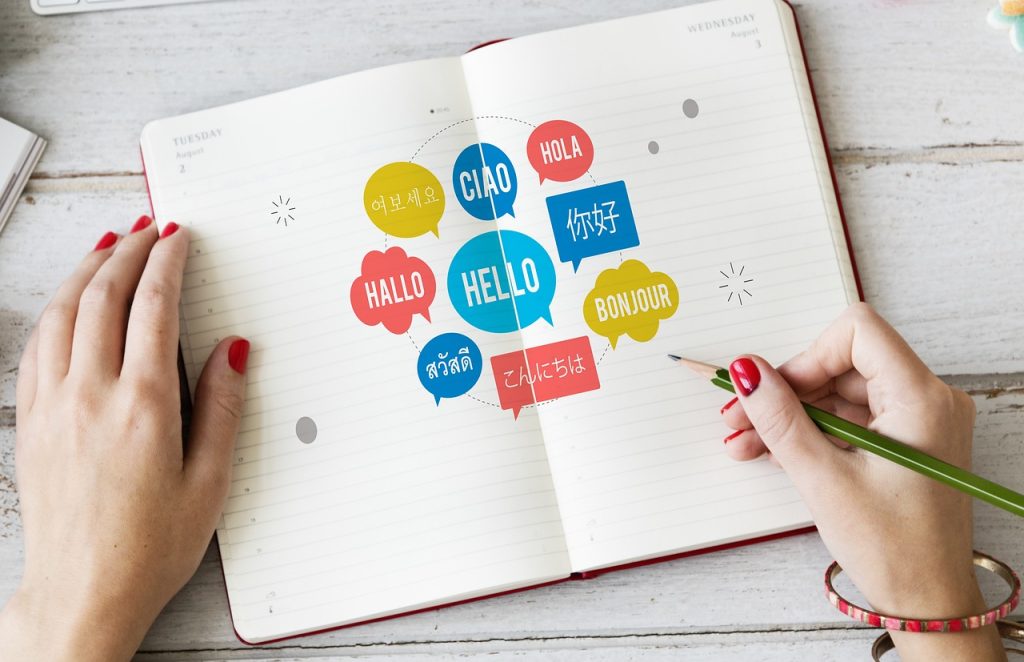
ज़ौं पॉल विने एवं ज़ौं पॉल दार्बेलने ने 1958 में प्रकाशित अपनी फ़्रेंच पुस्तक ‘Stylistique comparée du français et de l’anglais: méthode de traduction’ (स्तिलिस्तिक कौम्पारे द्यु फ़्रांसै ए द लौंग्ले : मेतोद द त्राद्युक्सियों) में अनुवाद प्रविधियों का वर्णन किया है। इस पुस्तक में अनुवाद को केंद्र में रखकर अंग्रेज़ी और फ़्रेंच की भाषिक संरचनाओं की तुलना की गई है। फ़्रांस में इसे तुलनात्मक शैलीविज्ञान की प्रतिनिधि पुस्तकों में से एक माना जाता है। विने एवं दार्बेलने ने इस पुस्तक में अनुवाद की सात प्रविधियों का उल्लेख किया है। यह पुस्तक चार दशक बाद 1995 में अंग्रेज़ी में ‘Comparative Stylistics of French and English : A methodology for translation’ (फ़्रेंच और अंग्रेज़ी का शैलीगत तुलनात्मक अध्ययन : अनुवाद प्रविधि) शीर्षक से अनूदित की गई। इतना समय बीत जाने के बावजूद इस पुस्तक का अंग्रेज़ी में अनूदित किया जाना इसकी प्रासंगिकता का प्रमाण है। अनुवाद प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी इस पुस्तक को उपयोगी माना जाता है।
हर भाषा की अपनी विशिष्ट भाषिक संरचनाएँ होती हैं। इन संरचनाओं की भिन्नता कई बार अनुवाद की चुनौती बनकर सामने आती है। भाषिक संरचनाओं की विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर न केवल भाषिक ग़लतियों से बचा जा सकता है, बल्कि अनुवाद को अधिक सहज और प्रभावी भी बनाया जा सकता है। विने एवं दार्बेलने ने अनुवाद की जिन सात प्रविधियों का उल्लेख किया है, उनका अध्ययन करके अनुवाद प्रशिक्षु अपनी स्रोत और लक्ष्य भाषाओं की भाषिक संरचनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनते हैं। इस सात प्रविधियों में से पहली तीन प्रविधियाँ प्रत्यक्ष अनुवाद से संबंधित हैं और बाकी चार प्रविधियाँ अप्रत्यक्ष अनुवाद से। जो प्रविधियाँ भाषिक संरचनाओं तक सीमित रहती हैं, उन्हें प्रत्यक्ष अनुवाद के अंतर्गत रखा गया है। वहीं, जिन प्रविधियों में भाषिक संरचनाओं से परे जाकर परिवर्तन किए जाते हैं, उन्हें अप्रत्यक्ष अनुवाद में शामिल किया गया है। ये सात प्रविधियाँ सरलता से जटिलता के क्रम में प्रस्तुत की गई। पहली प्रविधि सबसे सरल है और अंतिम सबसे जटिल। इन प्रविधियों का विवरण नीचे प्रस्तुत है :
1. आदान (Borrowing)
लक्ष्य भाषा में उपयुक्त विकल्प मौजूद नहीं होने की स्थिति में स्रोत भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चूँकि ये शब्द बिना किसी परिवर्तन के ग्रहण किए जाते हैं, इन्हें ‘ऋण शब्द’ कहा जाता है। यदि लक्ष्य भाषा की लिपि अलग हो, तो अनुवाद में इन शब्दों के लिप्यंतरित रूपों का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, विज्ञापन आदि क्षेत्रों में ऋण शब्दों का अधिक प्रयोग होता है।
कुछ हिंदी अख़बारों की संपादकीय नीति के कारण कई बार उपयुक्त शब्दों के उपलब्ध होने के बावजूद ऋण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, ‘विज्ञापन’ को ‘एडवर्टाइज़मेंट’ लिखना। जो देश आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, उनकी भाषाओं में विकसित भाषाओं के शब्दों के अनावश्यक प्रयोग की प्रवृत्ति देखी जाती है। यह स्थिति केवल हिंदी, मराठी जैसी भारतीय भाषाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जर्मन और फ़्रेंच में भी अंग्रेज़ी शब्दों की भरमार होने लगी है।
यदि विदेशी भाषा से शब्द ग्रहण करते समय सावधानी नहीं बरती जाए, तो इससे अनुवाद के ग़लत होने की आशंका बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, जब ‘Bodymist’ नाम की डियोडरेंट कंपनी के उत्पाद को जर्मनी के बाज़ार में उपलब्ध कराने के लिए इस नाम का ऋण शब्द के रूप में प्रयोग किया गया, तो ‘mist’ शब्द के कारण समस्या पैदा हो गई। जर्मन में ‘mist’ का अर्थ ‘खाद’ है, इसलिए प्रस्तुत संदर्भ मे जर्मन के बाज़ार में इसका प्रयोग अटपटा साबित हुआ।
2. काल्क (Calque)
विने एवं दार्बेलने ने इस प्रविधि को ‘एक विशिष्ट प्रकार का आदान’ कहा है। ‘काल्क’ (प्रतिलिपि) शब्द की व्युत्पत्ति फ़्रेंच की calquer क्रिया से हुई है, जिसका अर्थ ‘डिज़ाइन, मानचित्र आदि की नकल उतारना’ है। इसमें स्रोत भाषा की अभिव्यक्ति ग्रहण करके उसके घटकों का शाब्दिक अनुवाद किया जाता है। जैसे, अंग्रेज़ी के ‘cold war’ को हिंदी में ‘शीत युद्ध’ लिखा जाता है। यहाँ हिंदी समतुल्य में अंग्रेज़ी के शब्दों को यथावत नहीं लेकर ‘cold’ और ‘war’ के शाब्दिक अनुवादों के माध्यम से ‘शीत युद्ध’ समतुल्य प्रस्तुत किया गया है। काल्क के ज़रिए लक्ष्य भाषा में नई अवधारणाएँ शामिल होती हैं। जैसे, बैंकिंग में ‘चालू खाता’ (current account) और ‘बचत खाता’ (savings account) तथा राजनीति में ‘प्रधानमंत्री’ (prime minister) और ‘मुख्यमंत्री’ (chief minister) जैसे समतुल्य काल्क के उदाहरण हैं। समय के साथ ये समतुल्य इतने प्रचलित हो गए हैं कि इन्हें हिंदी में समतुल्य के बजाय मूल हिंदी शब्द माना जाने लगा है।
3. शब्दानुवाद (Literal Translation)
यह प्रविधि समान भाषिक संरचनाओं या संस्कृतियों वाली भाषाओं में अधिक प्रयुक्त होती है। इसमें बस वही परिवर्तन किए जाते हैं जो लक्ष्य भाषा के व्याकरण के लिए अनिवार्य होते हैं। उदाहरण के लिए, He hit Mohan को हिंदी में “उसने मोहन को मारा” लिखा जाता है। यहाँ हिंदी व्याकरण का पालन करते हुए ‘को’ जोड़ा गया है। ऐसे व्याकरणिक परिवर्तन शाब्दिक अनुवाद के दायरे में शामिल रहते हैं।
4. प्रतिस्थापन (Transposition)
इसमें अर्थ में परिवर्तन किए बिना स्रोत भाषा की व्याकरणिक कोटि को लक्ष्य भाषा की भिन्न व्याकरणिक कोटि से प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसे, “It is raining” को हिंदी में “बारिश हो रही है” लिखा जाता है। यहाँ अंग्रेज़ी की क्रिया (raining) के लिए हिंदी में ‘बारिश’ संज्ञा का प्रयोग किया गया है। “His presence suffices” वाक्य को हिंदी में “उसकी मौजूदगी काफ़ी है” लिखा जा सकता है। इस हिंदी वाक्य में अंग्रेज़ी की ‘suffices’ क्रिया’ को हिंदी में ‘काफ़ी’ विशेषण में परिवर्तित किया गया है।
5. मॉडुलन (Modulation)
जब स्रोत भाषा के कथ्य के रूप में परिवर्तन किया जाता है, उसे मॉडुलन कहते हैं। दूसरे शब्दों मे, इसमें मूल कथ्य को एक नये दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया जाता है। जैसे, “I hurt my toe” का हिंदी अनुवाद “मेरे अँगूठे में चोट लग गई” है। इस वाक्य में कर्तृवाच्य को अकर्मक रूप में बदला गया है। इसी प्रकार, “The meeting was chaired by Manmohan Sharma” को हिंदी में “मनमोहन सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की” लिखकर अंग्रेज़ी के कर्मवाच्य को हिंदी के कर्तृवाच्य में बदला गया है। इस परिवर्तन से लक्ष्य भाषा में संदेश अधिक सहज बनता है।
6. समतुल्यता (Equivalence)
इसमें स्रोत भाषा में वर्णित स्थिति को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने के लिए भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लोकोक्तियों, मुहावरों आदि के अनुवाद में इस प्रविधि का सर्वाधिक प्रयोग होता है। शब्दकोशों में इनके जिन समतुल्यों को शामिल किया जाता है, वे समतुल्यता के उदाहरण होते हैं। जैसे, “rain cats and dogs” को हिंदी में “मूसलाधार बारिश होना” कहते हैं। “Barking dogs seldom bite” के लिए “जो गरजते हैं, वे बरसते नहीं” का प्रयोग भी समतुल्यता का उदाहरण है।
7. अनुकूलन (Adaptation)
अनुवाद की यह प्रविधि तभी अपनाई जाती है जब स्रोत भाषा में वर्णित स्थिति लक्ष्य भाषा की संस्कृति में मौजूद नहीं होती है। विने एवं दार्बेलने इसके लिए अंग्रेज़ी के एक वाक्य का उदाहरण देते हैं : “He kissed his daugther on the mouth.” यदि हम इस उदाहरण को हिंदी के संदर्भ में देखें, तो ‘kissed’ के लिए ‘चूमा’ के बजाय ‘गले लगाया’ का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार, इसका अनुवाद “उसने अपनी बेटी का मुँह चूमा” के बजाय “उसने अपनी बेटी को गले लगाया” होगा। स्रोत भाषा की संस्कृति में पुत्री के मुख पर चुंबन लेने को असहज या अस्वीकार्य नहीं माना जाता है। चूँकि हिंदी में यह स्थिति सहज नहीं मानी जाती है, अनुवादक को एक नई स्थिति का सृजन करना पड़ता है। विने एवं दार्बेलने ने अनुकूलन को ‘एक विशिष्ट प्रकार की समतुल्यता’ कहा है। इस प्रविधि का प्रयोग तभी किया जाता है जब उपर्युक्त सभी प्रविधियों से अर्थ व्यक्त नहीं हो पा रहा हो।
लेखक : सुयश सुप्रभ

नई दिल्ली में रहने वाले सुयश सुप्रभ को मार्केटिंग, बिज़नेस, गेम, टेक्नॉलजी आदि क्षेत्रों में अनुवाद और कॉपी लेखन का 18 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अनुवाद अध्ययन में एमए किया है। वे अनुवाद एजेंसियों और ग़ैर-सरकारी संस्थाओं के लिए अनुवाद करने के साथ तहलका और करियर्स360 जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के लिए काम कर चुके हैं। साथ ही, उन्होंने भाषा और अनुवाद से जुड़े कई लेख लिखे हैं। उनसे suyash.suprabh@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।
Suyash Suprabh is based in New Delhi and has more than 18 years of experience in translation and copywriting in many fields, including marketing, business, games, and technology. He has a postgraduate degree in translation studies. Besides having worked for translation agencies and non-government organizations, he has also worked with renowned Hindi magazines, including Tehelka and Careeres360, and has written many articles on languages and translation. He can be reached at suyash.suprabh@gmail.com.
The post विने एवं दार्बेलने की अनुवाद प्रविधियाँ appeared first on Translators of India.
]]>The post व्यवहार से सिद्धांत और सिद्धांत से व्यवहार की ओर appeared first on Translators of India.
]]>
अनुवाद के क्षेत्र में लगभग एक दशक तक सक्रिय रहने के बाद इसके सैद्धांतिक पक्ष को ठीक से समझने में मेरी दिलचस्पी जगी। सबसे पहले तो यह सवाल दिमाग़ में आया कि अनुवाद करते समय हम भाषा, वर्तनी आदि से जुड़े जो विकल्प चुनते हैं उनका कोई सुव्यवस्थित अध्ययन हुआ है या नहीं। मुझे इस सवाल का जवाब अनुवाद अध्ययन में एमए करते समय नाइडा, न्यूमार्क, वर्मीयर जैसे अनुवाद सिद्धांतकारों के अकादमिक लेखन में मिला। जैसे-जैसे अनुवाद के सिद्धांतों में मेरी रुचि बढ़ती गई, मुझे अनुवाद के विस्तृत दायरे के बारे में और बहुत कुछ जानने को मिला। भारत में अनुवाद के इतिहास को ठीक से समझने में मुझे देवशंकर नवीन की पुस्तक ‘अनुवाद अध्ययन का परिदृश्य‘ से बहुत मदद मिली।
कई बार हम किसी धारणा को सिर्फ़ इसलिए सही मान लेते हैं कि अधिकतर लोग उसका समर्थन करते हैं। केवल सहज-सरल अनुवाद को अच्छा अनुवाद मानने की सोच भी ऐसी धारणाओं में से एक है। अकादमिक विषय के सिद्धांत की एक अच्छी बात यह होती है कि उसमें किसी बात को उसका समर्थन करने वालों की संख्या के आधार पर ही सही नहीं मान लिया जाता है। अनुवाद चिंतक लॉरेन्स वेनुती ने अनुवाद के सहज-सरल होने को उसका एकमात्र गुण मानने की सोच पर सवाल खड़ा किया है। अनुवाद में पाठ के विदेशीकरण और घरेलूकरण से जुड़े वेनुती के लेखन से हमें पता चलता है कि पाठक की सहूलियत का मामला उतना सरल नहीं है जितना हम उसे समझते आए हैं। सच तो यह है कि अनुवाद में सहजता लाने के सचेत प्रयास के कारण कई बार पाठक को अनुवाद में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जो उसके अनुभव-संसार का दायरा बढ़ाए। वेनुती ने अमेरिकी प्रकाशन जगत में सरल अंग्रेज़ी अनुवाद पर ज़ोर दिए जाने को अमेरिका की वर्चस्वकारी संस्कृति से जोड़कर देखा है। अनुवाद में स्रोत पाठ की संस्कृति की विशिष्टताओं को जगह न देना सांस्कृतिक श्रेष्ठता के बोध से जुड़ा है जिसमें अन्य संस्कृतियों के बारे में जानने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती है। वेनुती के लेखन में इस प्रवृत्ति की आलोचना दिखती है।
अनुवाद की दुनिया में क़दम रखने के बाद अनुभवी अनुवादकों से मुझे यह मालूम हो गया था कि अनुवाद भाव का होता है न कि शब्द का। लेकिन एक भाषा में कही गई बात को किसी दूसरी भाषा में व्यक्त करना हमेशा संभव नहीं होता है। चाहे साड़ी या धोती जैसे पहनावे से जुड़े शब्दों का अनुवाद करना हो या श्राद्ध, मुंडन जैसी धार्मिक-सांस्कृतिक अवधारणाओं को विदेशी पाठकों के लिए बोधगम्य बनाना हो, अनुवादक की चुनौतियों का कोई अंत नहीं होता है। जब आप ऐसे शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उनकी व्याख्या करते हैं, तो अनुवाद में मूल पाठ जैसी सहजता नहीं रह जाती। यह एक आम धारणा है कि केवल शब्दकोश की मदद से कोई भी व्यक्ति अनुवाद कर सकता है, जबकि सच यह है कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की सामाजिक-सांस्कृतिक जटिलताओं को ठीक से नहीं जानने वाले व्यक्ति से अच्छे अनुवाद की उम्मीद नहीं की जा सकती है। दो भाषाओं के पाठ असल में सममूल्य होते ही नहीं है। उनमें सममूल्यता की जगह समतुल्यता का संबंध होता है। यही वजह है कि नाइडा ने अनुवाद में निकटतम और सहजतम समतुल्यता की बात कही है न कि एक भाषा के कथ्य के सममूल्य अर्थ को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की।
नाइडा ने अपनी पुस्तक ‘टूवर्ड ए साइंस ऑफ़ ट्रांसलेटिंग‘ में बाइबिल के उन संदर्भों का उल्लेख किया है जो समतुल्यता से जुड़ी जटिलताओं को सामने लाते हैं। उदाहरण के लिए, बाइबिल में इस बात का उल्लेख है कि लंबे बाल रखना पुरुषों को शोभा नहीं देता है। लेकिन इक्वाडोर की जिवारो जनजाति के लोगों को यह बात अटपटी लगेगी क्योंकि वे लंबे बाल रखते हैं। इस जनजाति की औरतें छोटे बाल रखती हैं। दक्षिण अफ़्रीका के कुछ हिस्सों के लोग अपने मुखिया का स्वागत करने के लिए उसके रास्ते में पड़े पत्तों और शाखाओं को साफ़ कर देते हैं। बाइबिल में यह लिखा गया है कि जब ईसा मसीह येरूशलम जा रहे थे तब श्रद्धालु उनके रास्ते पर पत्ते और शाखाएँ फेंककर उनका स्वागत कर रहे थे। जहाँ लोग रास्ते में पड़े पत्ते और शाखाएँ साफ़ करने को स्वागत से जोड़कर देखते हैं, उनके लिए इस प्रसंग को समझना मुश्किल है। इस तरह, हम देखते हैं कि समतुल्यता को केवल शब्द के स्तर पर नहीं समझा जा सकता है, बल्कि इसे विभिन्न संस्कृतियों की मान्यताओं, अवधारणाओं आदि के बड़े दायरे में देखना होगा।
कई अनुवादकों का मानना है कि अनुवाद अध्ययन से अनुवादक को किसी तरह की मदद नहीं मिलती है। वे कुछ अच्छे अनुवादकों के नाम गिनाते हुए कहते हैं कि उन्होंने अनुवाद सिद्धांतों की जानकारी के बिना इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। उनकी इस बात से यहाँ तक मेरी सहमति है कि अनुवादक अपने कौशल के लिए सिद्धांत पर निर्भर नहीं होते हैं। लेकिन जब बात अनुवाद अध्ययन को सिरे से ख़ारिज करने तक पहुँच जाती है तो मैं असहमति जताना ज़रूरी समझता हूँ। अकादमिक दुनिया में अनुवाद अध्ययन की स्थिति बेहतर होने से अनुवादक से जुड़े मसलों के प्रति बेहतर समझ पैदा करने में मदद मिलेगी। अधिकतर लोगों को यह पता ही नहीं है कि किसी भाषा की सामाजिक-सांस्कृतिक विशिष्टताओं को दूसरी भाषा में अच्छे ढंग से व्यक्त करने के लिए अनुवादक को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर अनुवाद की जटिलताओं और सभ्यता के विकास में इसके योगदान की विस्तृत जानकारी स्कूल के स्तर पर ही दे दी जाए, तो पढ़-लिखे लोगों की अनुवाद के प्रति अतार्किक सोच को बदलना संभव हो जाएगा।
आज अनुवाद अध्ययन में कॉर्पस भाषाविज्ञान, स्कोपस सिद्धांत, शब्दावली प्रबंधन आदि की पढ़ाई पर ध्यान देकर अनुवादक की व्यावसायिक और व्यावहारिक ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही, औपनिवेशिकता, जेंडर आदि से जुड़े विमर्श के माध्यम से अनुवाद के वैचारिक दायरे का विस्तार किया जा रहा है। ज़रूरत बस अनुवाद के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्षों के बीच संवाद में तेज़ी लाने की है। ऐसा तभी होगा जब पेशेवर अनुवादकों और अकादमिक दुनिया के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए सांस्थानिक स्तर पर प्रयास किए जाएँगे।

नई दिल्ली में रहने वाले सुयश सुप्रभ को मार्केटिंग, बिज़नेस, गेम, टेक्नॉलजी आदि क्षेत्रों में अनुवाद और कॉपी लेखन का 17 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अनुवाद अध्ययन में एमए किया है। वे अनुवाद एजेंसियों और ग़ैर-सरकारी संस्थाओं के लिए अनुवाद करने के साथ तहलका और करियर्स360 जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के लिए काम कर चुके हैं। साथ ही, उन्होंने भाषा और अनुवाद से जुड़े कई लेख लिखे हैं। उनसे suyash.suprabh@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।
Suyash Suprabh is based in New Delhi and has more than 18 years of experience in translation and copywriting in many fields, including marketing, business, games, and technology. He has a postgraduate degree in translation studies. Besides having worked for translation agencies and non-government organizations, he has also worked with renowned Hindi magazines, including Tehelka and Careeres360, and has written many articles on languages and translation. He can be reached at suyash.suprabh@gmail.com.
The post व्यवहार से सिद्धांत और सिद्धांत से व्यवहार की ओर appeared first on Translators of India.
]]>